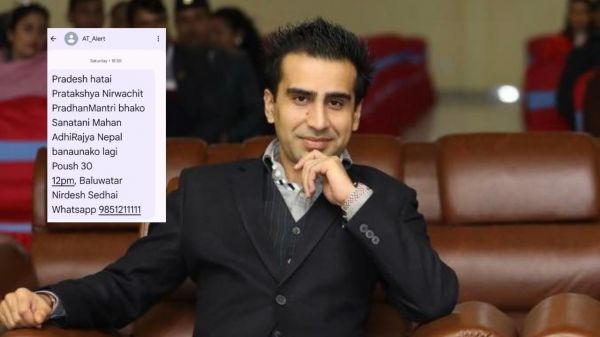मुग़ल-ए-आज़म हिंदुस्तानी सिनेमा इतिहास की एक ऐसी यादगार फिल्म है जिसे बनाने का सपना हर फिल्मकार देखता है लेकिन साकार कोई बिरला ही कर पाता है। पिछले 64 बरसों में हजारों फिल्में बनी हैं, कुछ ही याद रह गईं और बाक़ी वक्त की धूल में दब चुकी हैं। लेकिन मुग़ल-ए-आज़म आज इतने समय के बाद भी दर्शकों के दिलोदिमाग में क्यों ताजा है? प्रख्यात फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही ने 1980 में अपने एक लेख में मुग़ल-ए-आज़म की अभूतपूर्व सफलता के बारे में बताते हुए कहा था कि इसका मुख्य कारण परफेक्ट कास्टिंग... उनके मुताबिक के. आसिफ ने इस फिल्म में हर किरदार के लिए एक-एक एक्टर ऐसा चुना था जो अंगूठी में नगीने की तरह जड़ा हुआ मालूम होता है। फिल्म में संगतराश के किरदार के लिए कुमार का चुनाव कमाल अमरोही की इस बात को बड़ी पुख्तगी से स्वीकार करता है।
संगतराश पूरी फिल्म का एकमात्र ऐसा किरदार है जो बादशाह के खिलाफ़ है। प्रख्यात पत्रकार राजकुमार केसवानी ने अपनी पुस्तक दस्तान-ए- मुग़ल-ए-आज़म में इस पात्र के बारे में लिखते हुए कहा है कि इस एक किरदार के ज़रिए आसिफ़ ने 16 वीं सदी की कहानी में बड़ी महीन कारीगरी और नफ़ासत से एक ऐसा चेहरा जोड़ दिया है जिसे इक्कीसवीं सदी में फ़िल्म देखने वाला भी ब-आसानी अपने दौर के साथ जोड़कर देख सकता है। इस संगतराश के एक-एक लफ़्ज़ में शहंशाही निज़ाम के लिए नफ़रत और हक़परस्ती की बेख़ौफ़ बात मौजूद है। संगतराश जब-जब मुंह खोलता है, तब-तब सिनेमा हाल में बैठे दर्शक को बेसाख़्ता उस आवाज़ में ख़ुद अपनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। संगतराश का यह बेख़ौफ़ अंदाज़ उसके पहले दृश्य में ही नज़र आ जाता है। उसके पास एक मुज्जसमे की फरमाइश लेकर आई बहार उसके तंज़ का शिकार बनती है-
"संगतराश! संगतराश !... महलों की बहार वीराने में ! साहिबे आलम के लिए पत्थर का एक मुज्जसमा लेने आई हूं।
"मेरे बनाए हुए मुज्जसमे शहज़ादों और बादशाहों को पसंद नहीं आएंगे..."
क्यों?"
"क्योंकि यह सच बोलते हैं।
एक दूसरा संवाद है- " वो तीर ही क्या संगतराश, जो दिल के पार न हो। वो बुत ही क्या जिसके आगे मग़रूर सिर खुद न झुक जाएं...'
संगतराश- 'तो फिर मैं एक ऐसा बुत बनाऊंगा, जिसके क़दमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर रख दे।"
संगतराश का सामना शहंशाह अकबर से जब-जब होता है उस वक़्त भी उसकी वही बेख़ौफ़ अदा बनी रहती है। के. आसिफ़ जिस वक़्त शहज़ादा सलीम की सज़ा-ए-मौत के वक़्त अवाम के विरोध की आवाज़ बुलंद करने वाला मंज़र सोचते हैं तो उस इंक़लाब की आवाज़ की रहनुमाई की बागडोर भी वे संगतराश के हाथ में दे देते हैं... ज़िंदाबाद.. ज़िंदाबाद.. ऐ मुहब्बत ज़िंदाबाद... फिल्म में संगतराश एक कलाकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का चेहरा हैं। वह शाही खानदान के किरदारों की तरह हसीन चेहरा नहीं बल्कि उनके मुकाबले बिखरे बालों और बिजली की सी कड़क भरी आवाज़ में बेखौफ सीधी और सच्ची बात करता है। यह वही शानदार अभिनेता है जो श्री 420 में राज कपूर को एक परम सत्य से परिचय कराता है या वह जिन पर फिल्म मेहंदी में हेमंत कुमार का गया मशहूर गीत,"बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है" फिल्माया गया है।
कुमार का जन्म 1903 में लखनऊ में हुआ। इनका पूरा नाम था सैयद हसन अली जाहिदी था। आगे चलकर मीर हसन अली कहलाए। शुरुआती फिल्मों में अली मीर के नाम से काम करते रहे लेकिन फिल्मी करियर में एक मोड़ आया जब वे पूरन भगत (1933) के दौरान कुमार हो गए। इस नाम के साथ उन्होंने अंत तक अनेक फिल्मों में काम किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। 1936 में कुमार की मुलाकात उस समय की मशहूर अभिनेत्री प्रमिला से फिल्म महामाया के सेट पर हुई जो आजाद हिंदुस्तान की पहली मिस इंडिया बनीं। दोनों ने शादी कर ली। अपनी खनकदार आवाज़ और डायलॉग बोलने के विशिष्ट अंदाज़ से उन्होंने कई किरदारों को यादगार बनाया। अपने 45 साल के फिल्मी कैरियर में उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1932 से 1948 तक विभिन्न प्रकार के रोल नायक के रूप में निभाए और इसके बाद 1948 से 1966 तक अपनी बढ़ती उम्र के कारण चरित्र रोल किए। कमाल अमरोही की महल में महल के केयरटेकर माली, नेक परवीन में हाजी साहब, तराना में मधुबाला के सूरदास पिता वाली भूमिकाओ में उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। 1961 में फिल्म शमा, रजिया सुल्तान, झुमरू और 1962 में अपने पुराने दोस्त महबूब खान की आखिरी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी वह दिखे। 40 के दशक में उन्होंने सिल्वर फिल्म नाम से अपना होम प्रोडक्शन भी शुरू किया था और कई फिल्मों का निर्माण भी किया था। वे 1963 में पाकिस्तान चले गए और फिल्मों में काम करते रहे। 1982 में वे हमारे बीच नहीं रहे। उनके बेटे सैयद हैदर अली हैं, जिन्हें हमलोग नुक्कड़ में राजा का किरदार निभाते देख चुके हैं। फ़िल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में उन्होंने शाहरुख के पिता की भूमिका निभाई थी। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर के लेखक भी वही हैं।
चलते-चलते
मीर हसन अली के कुमार बनने का किस्सा कुछ यूं है कि 1930 के दशक के महान फ़िल्मकार देवकी बोस न्यू थियेटर्स, कलकत्ता के लिए फ़िल्म 'पूरन भगत' (1933) बनाने की योजना बना रहे थे। मीर हसन अली भी एक्टर बनने की तमन्ना लिए लखनऊ से रंगून तक चक्कर लगाकर कलकत्ता लौट आए थे। देवकी बोस ने उन्हें सीधे 'पूरन भगत' की भूमिका दी। जिस वक़्त यह फ़िल्म रिलीज़ के नज़दीक पहुंची उस वक़्त तक साम्प्रदायिक दंगों की आग देश के कई शहरों में भड़क चुकी थी। ऐसे में मीर हसन अली को पूरन भगत बनाकर पेश करना काफ़ी जोख़िम का काम था। बहुत सोच विचार के बाद देवकी बोस ने मीर हसन अली से कहा कि मैं तुम्हें अपने नाम का एक हिस्सा बतौर तोहफ़ा देता हूं। मैं अब से अपने नाम में कुमार नहीं लगाऊंगा।अब से कुमार तुम हो और मैं सिर्फ़ देवकी बोस। उन दिनों फिल्मों में कुमार सब सफलता का पर्याय माना जाता था जैसे अशोक कुमार, दिलीप कुमार तो चल ही चल रहे थे आगे चलकर राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार से होकर यह परंपरा कुमार गौरव तक चली जाती है।
-अजय कुमार शर्मा