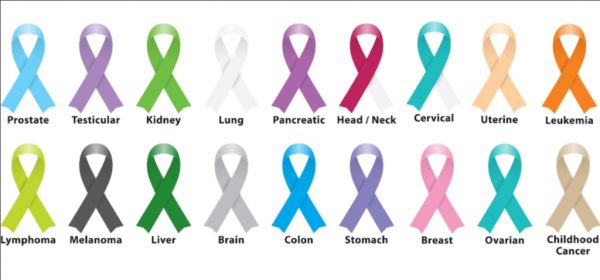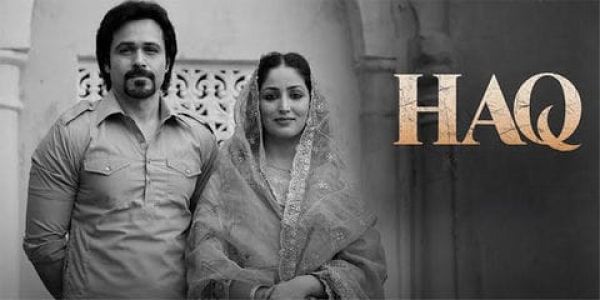हर वर्ष 9 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, जो 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम ने देशभर में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का समान अवसर मिले और कोई व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक या अन्य बाधाओं के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार तथा कानून के समक्ष समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बावजूद, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक असमानता या प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियाँ अनेक लोगों को न्यायिक प्रणाली तक पहुँचने से रोकती हैं। इन्हीं कारणों से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क, सुलभ और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
इस अधिनियम के तहत देशभर में त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) का संचालन संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। इन संस्थाओं को केंद्रीय और राज्य सरकारों से विभिन्न कानूनी सहायता कोषों के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच विधिक सेवा प्राधिकरणों की निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं से 44.22 लाख लोगों को लाभ मिला है।
अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की गई है, जो विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी माध्यम हैं। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिससे यह पहल विश्व के सबसे बड़े वैकल्पिक विवाद निपटान अभियानों में शामिल हो गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) योजना के अंतर्गत आपराधिक मामलों में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी बचाव उपलब्ध कराया जाता है। 30 सितंबर 2025 तक देश के 668 जिलों में यह योजना कार्यरत है। अब तक 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वर्ष 2023-26 के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
आधुनिक तकनीक न्याय तक पहुँच को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिशा योजना, जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया गया है, इसके अंतर्गत अब तक 2.10 करोड़ से अधिक लोगों को मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क कानूनी सेवाएँ, प्रतिनिधित्व और जागरूकता प्रदान की जा चुकी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका कुल बजट 250 करोड़ रुपये है।
कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने भाग लिया। न्याय विभाग की कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP) योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की 22 भाषाओं और बोलियों में सामग्री विकसित की गई। दूरदर्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन अभियानों ने एक करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुँच बनाई।
महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई। 30 जून 2025 तक 865 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) और 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) कार्यरत हैं, जिनमें से 392 अदालतें पॉक्सो (POCSO) मामलों के लिए समर्पित हैं। स्थापना के बाद से इन अदालतों ने 3.34 लाख मामलों का निपटारा किया है। यह योजना निर्भया फंड सहित 1,952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक विस्तारित की गई है।
ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की सुलभ पहुँच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मार्च 2025 तक देश में 488 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं, जो स्थानीय विवादों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत नारी अदालतों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करना है। असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में इन अदालतों का संचालन किया जा रहा है, जबकि 16 अन्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका पायलट परीक्षण चल रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों के निपटारे के लिए 211 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और एनएएलएसए न्यायाधीशों, विधिक अधिकारियों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वर्ष 2023-24 से मई 2024 तक पूरे देश में 2,315 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रभावी, संवेदनशील और समय पर प्रदान की जा सके।
भारत की न्याय प्रणाली का मूल उद्देश्य सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। विधिक सेवा प्राधिकरणों, लोक अदालतों, फास्ट ट्रैक न्यायालयों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को न्याय तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रणाली न केवल विवादों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, न्याय से वंचित न रहे।





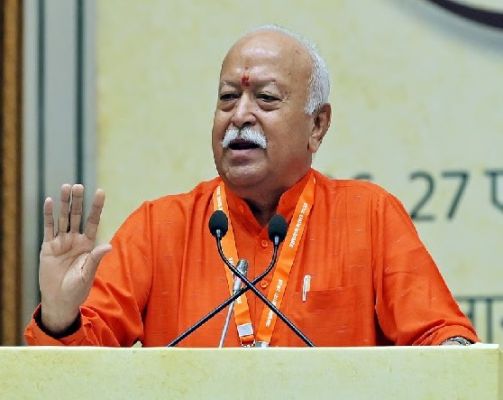






.jpg)




.jpg)


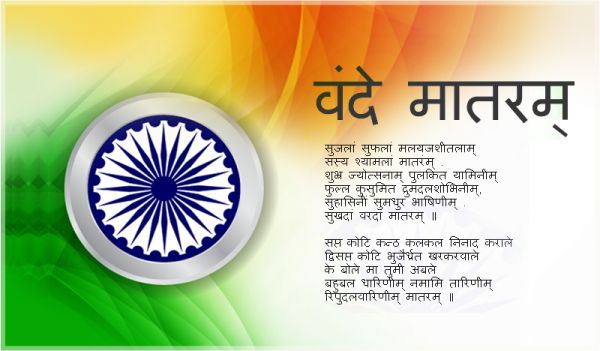
.jpg)