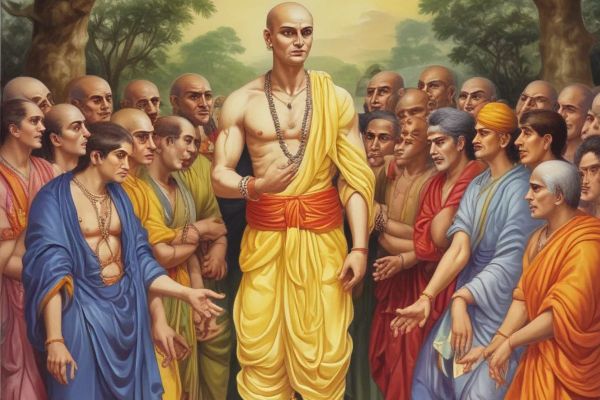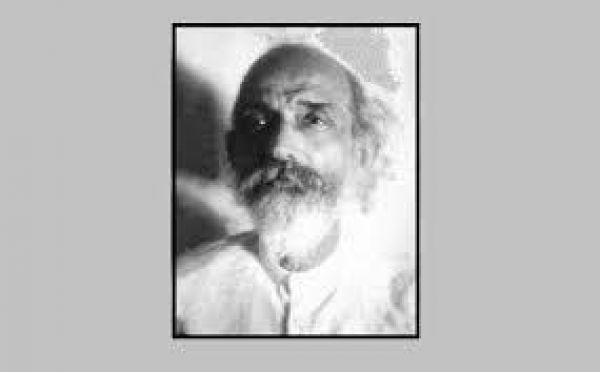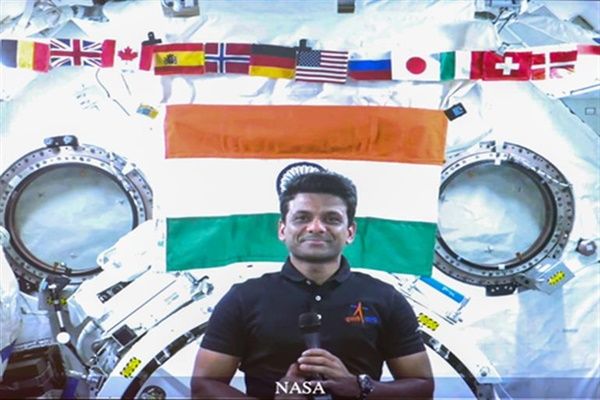वाराणसी, बनारस का प्राचीन शक्तिशाली शहर, इतिहास, कला, पुरातत्व, भूगोल, पौराणिक कथाओं और संस्कृति के अन्य वर्गों से प्रसिद्धि पाता है। वाराणसी देवत्व, सभ्यता और आधुनिक संस्कृति की जन्मभूमि से जुड़ा है। आज, वाराणसी प्राचीन भारतीयों की कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवनशैली के संग्रहालय के रूप में खड़ा है।
इतिहास-
वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका उपयोग अभी भी किया जाता है। इस शहर का नाम पहले काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवताओं ने मनुष्यों के बीच रहने के लिए इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान शिव खासी में रहते थे। इतिहासकारों के अनुसार वाराणसी में सभ्यता की शुरुआत आर्यों द्वारा गंगा घाटी सभ्यता के दौरान हुई थी। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अंत तक , वाराणसी देश के संपन्न और समृद्ध क्षेत्रों में से एक था।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में , भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी से सिर्फ 10 किमी दूर , नए धर्म, बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हुए दिया था। देश भर से कई लोग विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए काशी पहुंचे। एक चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 635 ई. में काशी का दौरा किया था।
यह भूमि 12वीं शताब्दी तक फली-फूली , जब आक्रमणकारियों ने प्राचीन काशी के अधिकांश भाग को नष्ट कर दिया। कई मुस्लिम शासकों ने तीन शताब्दियों तक वाराणसी को नष्ट कर दिया व 17 वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा इसे फिर से नष्ट कर दिया गया। 18 वीं सदी में वाराणसी को एक अलग राज्य घोषित किया गया, जिसकी राजधानी रामनगर थी। 20 वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इसे एक अलग राज्य घोषित कर दिया । आजादी के बाद वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सीमा में जोड़ दिया गया।
बोली-
95% से अधिक स्थानीय आबादी हिंदी बोलती है और लगभग 3% आबादी उर्दू को अपनी पहली भाषा बताती है। वाराणसी में भोजपुरी भी बोली जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत बनारस की सबसे प्राचीन भाषा थी। हालाँकि, वाराणसी में आज अंग्रेजी काफी आम है।
साहित्य-
वाराणसी कभी आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र था। इसे सर्वविद्या की राजधानी कहा जाता था। वाराणसी ने विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्वानों, बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों को विकसित किया। वाराणसी में अतीत में कई विश्वविद्यालय बनाये गये।
तुलसीदास कुल्लूका, कबीर दास, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य शुक्ल, तेग अली, बलदेव उपाध्याय, वागीश शास्त्री, विद्या निवास मिश्र और अन्य जैसे कई लेखक वाराणसी में फले-फूले। यह शहर आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और पंचकर्म उपचार में भी फला-फूला। कई अस्पताल बनाए गए और प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सा पुस्तक सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत वाराणसी में रहते थे और प्रशिक्षण लेते थे।
तथ्य-
बनारस शहर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है।
यह शहर योग, चिकित्सा, समग्र उपचार विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और अन्य के अध्ययन का केंद्र था।
वाराणसी देश की आध्यात्मिक राजधानी है।
वाराणसी सोने के ब्रोकेड, बनारसी रेशम, चांदी के सामान और अन्य वस्तुओं का प्रमुख व्यापार केंद्र भी है
शहर में हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं को समर्पित 3,000 से अधिक मंदिर हैं।
एशिया का सबसे बड़ा एवं प्राचीन विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आज एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है।
बरसात के मौसम में, अश्वमेघघाट में एक पुजारी द्वारा मेंढकों के एक जोड़े की शादी कराई जाती है। नवविवाहित जोड़े को नदी में छोड़ दिया गया है।
यह एक लोकप्रिय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस वाराणसी में लेता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके कारण, हर साल सैकड़ों लोग मरने तक रहने के लिए वाराणसी आते हैं। कुछ तो अपनी जान देने के लिए नदी में भी कूद जाते हैं।
इस शहर में 88 घाट हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक नदी तटों वाला शहर बनाता है।
वाराणसी के बनारस और काशी के अलावा कई अन्य नाम भी हैं। लोगों के बीच लोकप्रिय शीर्ष नाम सुदर्शन, ब्रह्मा वर्धा, महास्मासन, राम्या और अन्य हैं।
धर्मों-
वाराणसी भारत के तीन प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान है; हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये आध्यात्मिक मान्यताएँ और अनुष्ठान पवित्र नदी गंगा के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान शिव ने धरती पर फलने-फूलने के लिए भेजा था। वाराणसी में 3,300 मंदिरों के अलावा, 3 चर्च, 9 बौद्ध मंदिर, 3 गुरुद्वारे, 1,388 मस्जिदें और दरगाहें और 3 जैन मंदिर भी हैं।
कला-
वाराणसी में एक अनूठी कला संस्कृति है। अतीत में, यह परंपराओं और संस्कृति का केंद्र था। प्रत्येक आधुनिक सांस्कृतिक प्रदर्शन इस भूमि की प्राचीन कला और संस्कृति से उत्पन्न हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार, बनारस या काशी कई कलाकृतियों और प्रदर्शन कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। भूमि पर पनपने वाली शीर्ष कला कृतियाँ धातु कृतियाँ, बनारस रेशम बुनाई, तांबे के बर्तन और अन्य थीं।
नृत्य और संगीत-
वाराणसी प्राचीन काल से ही संगीत का प्रतीक रहा है। बनारस में गायन और वाद्य संगीत खूब फला-फूला। आज भी यह शहर समृद्ध लोक संगीत कृतियों से भरा पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के नृत्य और संगीत रूपों को भगवान शिव द्वारा विकसित किया गया था। संगीत परम्परा का प्रसार विश्वामित्र के पुत्र रेनू ने किया। संगीत कौशल के लिए प्रसिद्ध प्राचीन संत मीरा, कबीर, सूरदास, तुलसीदास और रविदास हैं। संगीत का आधुनिक रूप नव-वैष्णव आंदोलन के दौरान विकसित हुआ।
16 वीं शताब्दी के दौरान , होरी, धमार, चतुरंगा, असरवारी और अन्य जैसे संगीत के नए रूप विकसित हुए। हाल के दिनों में, चैती, बनारसी ठुमरी, कजरी, होरी और अन्य जैसे आधुनिक संगीत रूपों का विकास हुआ। वाराणसी की उल्लेखनीय संगीत हस्तियाँ समता प्रसाद, किशन महाराज, समर साहा और अन्य हैं।
शहर के अंदर एक वाराणसी संगीत विद्यालय है, जो बच्चों को कजरी, चैती और अन्य संगीत के पारंपरिक और लोक संस्करणों में प्रशिक्षित करता है। इस विद्यालय में वाद्य और स्वर दोनों प्रकार का संगीत सिखाया जाता है। वाराणसी के शीर्ष संगीत वाद्ययंत्र सितार और तबोला हैं। यदि आप वाराणसी से वाद्ययंत्र खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो याद रखें कि वाद्ययंत्र आम के पेड़ की लकड़ी और सागौन की लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। आम के पेड़ की लकड़ी वाली लकड़ी कीमत में घटिया और सस्ती होती है। विजयसार, एक हर्बल पेड़ की लकड़ी से बने उपकरण बहुत महंगे हैं और एक विरासत के रूप में माने जाते हैं।
वाराणसी के नृत्य रूप-
1. कथक
कथकी बनारस और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह नृत्य कहानी कहने और पौराणिक वर्णन का एक रूप है। कथक के बनारस घराने संस्करण की उत्पत्ति वाराणसी में हुई।
2. रासलीला
यह एक विशिष्ट पौराणिक कथाओं पर आधारित नृत्य-सह-संगीत नाटक है, जो भगवान कृष्ण के जीवन और प्रेम को समझाता है। यह लोक नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित त्योहारों के दौरान बहुत आम है।
3.रामलीला
यह रासलीला के समान है, लेकिन यह भगवान राम की किंवदंतियों पर केंद्रित है। नृत्य का यह रूप बनारस के लोक नृत्यों के सबसे पुराने रूपों में से एक है। यह लोक नृत्य आमतौर पर दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है। तबला और हारमोनियम इस प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र हैं।