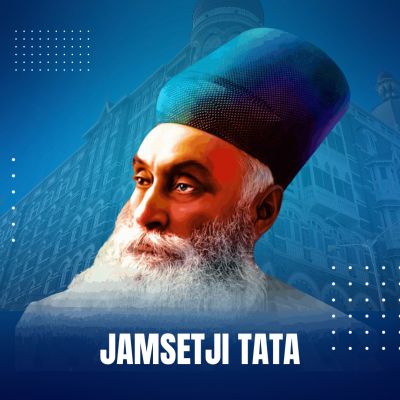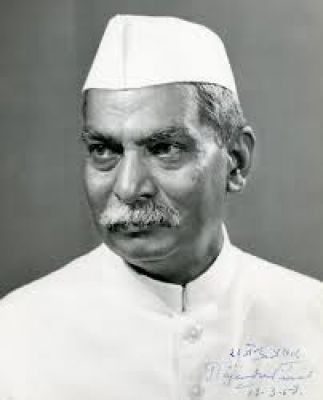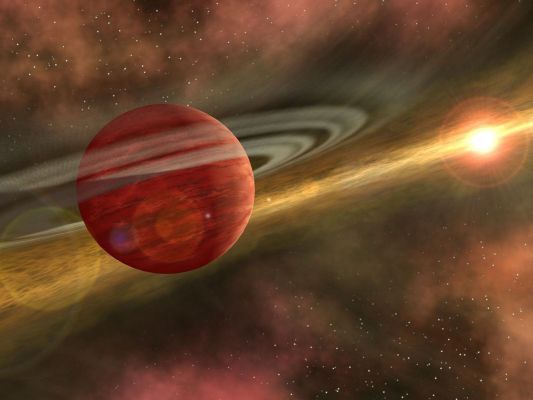स्वतंत्रता- यह शब्द सुन कर अक्सर मन में सबसे पहले बंधन से मुक्ति का भाव आता है। इस स्थिति में किसी तरह के बंधन नहीं रहते और प्राणी को स्वाधीनता का अहसास होता है। परंतु स्वतंत्रता निष्क्रिय शून्यता की स्थिति नहीं है और स्वतंत्रता स्वच्छंदता भी नहीं है। वह दिशाहीन नहीं हो सकती। बिना किसी लक्ष्य के निरुद्देश्य स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं रखती। इस बारे में सोचते हुए ये सवाल उठते हैं कि स्वतंत्रता किससे चाहिए? और यह भी कि स्वतंत्रता किसलिए चाहिए? सच कहें तो स्वतंत्रता या स्वतंत्र (बने) रहना एक क्रिया है, एक जिम्मेदार क्रिया क्योंकि इसमें किसी और पर निर्भरता नहीं रहती। स्वतंत्र होकर संकल्प और आचरण के केंद्र हम स्वयं हो जाते हैं। स्वतंत्रता बनी रहे और जिस उद्देश्य के लिए है, वह पूरा होता रहे ऐसा अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए प्रतिबद्धता और दिशाबोध के साथ जरूरी सक्रियता भी होनी चाहिए। थोड़ी गहराई में जाएं तो यही लगेगा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है अपने कार्य का दायित्व खुद अपने लेना, दूसरे के जिम्मे न सौंपना और जिस देश-काल में मौजूद हैं, उसके प्रति अपने दायित्वों को स्वीकार करना। उसी के विवेक के अनुसार बिना किसी के दबाव के स्वतंत्र निर्णय लेना और उसके अनुसार कार्य करना। ऐसा न हुआ तो स्वतंत्रता उच्छ्रिंखलता का रूप लेने लगेगी । स्वतंत्रता की संस्कृति का आवाहन है कि हम अपने कार्यों का सुचारु निर्वहन करें और उत्कृष्टता के साथ। तभी सृष्टि में संगति बनेगी, रहे तभी रचनात्मकता आएगी, और तभी विकास और उन्नति का लक्ष्य भी सधेगा।
भारत को सन् 47 में आजादी मिलने के बाद देश ने तीन चौथाई सदी का एक लम्बा सफर पूरा कर अब अमृतकाल में प्रवेश किया है। इस बीच भारत की संप्रभुता को कई बार चुनौतियाँ मिलीं और उन क्षणों में स्वतंत्रता के अनुभव को हम जानने पहचानने की कोशिश करते रहे। इससे लगता है कि एक राजनैतिक इकाई के रूप में अन्य देशों द्वारा स्वीकृति और स्वयं अपनी पहचान को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना एक लगातार चौकसी रखने वाली प्रक्रिया है। उसका स्थायित्व बहुत हद तक हमारे अपने दम ख़म और प्रयास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता सदैव आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के सापेक्ष्य ही संभव होती है और उसके लिए निरंतर प्रयास की भी अपेक्षा होती है। यह बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों में और दूरदराज की तमाम जगहों पर चल रही छोटी बड़ी उथल-पुथल के संदर्भ में आसानी से देखी जा सकती है।
स्वतंत्रता पाने के लिए भारतीय समाज ने बड़ी कीमत अदा की थी। अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई में देश के कोने-कोने से हर भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और कई विचारधाराओँ के लोग शामिल हुए थे । देश के सामने उनकी छोटी अस्मिताएँ आड़े नहीं आ रही थीं और सबने बिना किसी भेद भाव के त्याग और बलिदान किया था । भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि से आने के बावजूद देश भक्तों के बीच आपस में भरोसा था । स्वतंत्रता पाने के साझे के लक्ष्य के स्वीकार के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ ऊपर जाकर भारत माता के इन वीर सपूतों ने वीरता की अमर गाथा लिखी। वे तमाम कष्ट झेल कर भी देश के लिए एकाग्र चित्त से काम करते रहे । उनके बलिदानों का सुख बाद के लोग और हम सभी भोग रहे हैं । स्मरणीय है कि उन सबने अंग्रेजों की वंदिनी बनी भारत माता के उद्धार के रूप देशप्रेम की परिकल्पना थी। वन्दे मातरम में मां-बेटे के उस रिश्ते की ध्वनि गूंजती है जिसके बीज हज़ारों साल पहले वेद में ऋषि की वाणी माता भूमि: पुत्रोहं पृथिव्या: में निहित भावना में व्यक्त है। ]इसमें माँ पहले आती है, वह पूर्व पक्ष है, और उसकी संतान बाद में, वह उत्तर पक्ष है । पुत्र तो जन्म से ही मातृ ऋण से बंधा होता है। यह उस राष्ट्र राज्य (नेशन स्टेट) के मसौदे से उलट है जो कुछ लोग या समुदाय मिल कर अपने उद्देश्य के लिए बनाते हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्र या देश बाद में आता है और व्यक्ति पहले। इस सोच में राष्ट्र या देश व्यक्ति या समुदाय के लिए एक संसाधन या उपाय बन जाता है उसका कोई जैविक रिश्ता संकल्पित नहीं होता । उसकी सत्ता उसकी उपयोगिता पर टिकी होती है । देश उन लोगों का होता है, उस पर उनका अधिकार होता है। वे देश के हों, यह उनकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। आखिर देश उनका अपना निर्णय है और देश को ‘बिलोंग’ करना न करना उनका ‘च्वायस’ है। उन पर देश का कोई ऋण नहीं बनता।
पिछले पचहत्तर सालों में हमारी सोच-समझ का नजरिया बदला है। औपनिवेशिक प्रभाव के चलते देश की स्वतंत्रता को लेकर अपने दायित्व के बारे में कुछ भ्रम फैले हैं। हम अधिकार की भाषा ज्यादा जानते हैं। संविधान में नागरिकों को दी गयी स्वतंत्रता को याद रखते हैं पर कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। देश हमें क्या दे यह तो याद रहता है पर हम देश को क्या दें, यह भूलता जा रहा है।
वर्तमान काल भारतीय समाज के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है और पथ-प्रदर्शन के पारम्परिक स्रोत सूख रहे हैं । मीडिया की बैसाखी पर व्यक्तिवाद और भौतिक समृद्धि का आकर्षण खूब फल-फूल रहा है। विचार और कर्म के प्रदूषण का ख़तरा भी बढ रहा है । नैतिकता और स्वाभाविक कर्तव्य को छोड़ लोग स्वार्थ, लोभ और मुफ़्तख़ोरी में प्रवृत्त हो रहे हैं । यह परिस्थिति निजी जीवन और समाज की प्रगतिकामी गतिविधियों को बाधित कर रही है। इन सबके चलते नकारात्मकता बढ़ रही है। हम स्वतंत्रता का सतही अर्थ लगा कर अपने लिए छूट पाने के अवसर बनाने लगे। लोग अपने हित के लिए रक्षा कवच के रूप में स्वतंत्रता का उपयोग करने लगे। इन सभी प्रवृत्तियों के पीछे उस भौतिकवादी सोच की भी बड़ी भूमिका है जो भ्रामक और अदूरदर्शी है और जो हमारे अस्तित्व के बड़े सच को झुठलाने वाली है । यहाँ पर यह याद रखना ज़रूरी है कि भारतीय चिंतन भौतिक अस्तित्व का विरोध नहीं करता पर उसे ही सर्वस्व नहीं मानता। मानव जीवन का प्रयोजन विवेक के साथ एक ऐसी समावेशी दृष्टि को अपनाना है जिसे एक अर्थ में ‘आध्यात्मिक’ कहा जा सकता है। आध्यात्मिकता से गुणवत्तापूर्ण भौतिक जीवन का सबल आधार होती है क्योंकि उसे अपना सद्भाव और सौहार्द के साथ हम जी सकेंगे । इस प्रसंग में देश के श्रेष्ठतम प्रतीक के रूप स्वीकृत भारत के झंडे को स्मरण करना प्रासंगिक होगा जो देश की प्रतिबद्धता को रूपायित करता है। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाती है। बीच की धवल श्वेत पट्टी में सुंदर धर्म-चक्र बना है। यह शांति और सत्य की अभिव्यक्ति है। नीचे की हरे रंग की पट्टी उर्वरता, वृद्धि और पवित्रता को व्यक्त करती है। गौर करने की बात है कि शांति और सत्य मध्य में है और उसके केंद्र में धर्म चक्र है। इसी पर शेष टिका हुआ है। बल की प्रतीति कराने वाली शक्ति हो या साहस या फिर समृद्धि, उत्पादकता और पवित्रता हो सबके लिए धर्म ही प्राथमिक महत्व का है। भारतीय समाज का स्वभाव और उसकी जीवन-दृष्टि मूलतः धर्म से अनुप्राणित है । उसमें समष्टि चैतन्य के अभिनंदन का भाव निहित है । इस विश्व दृष्टि में मनुष्य और प्रकृति ओतप्रोत हैं । मनुष्य होने का अर्थ ही है आत्म-विस्तार।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का स्पंदन एक दूसरे से जुड़ कर ही संभव होता है क्योंकि हम जिस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं उसमें कुछ भी अकेला, निरपेक्ष और पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ऐसे में हर घटना अपने आसपास जो कुछ भी है उसे प्रभावित करती चलती है। अपने अहं का अतिक्रमण कर और अन्य से जुड़ कर ही अध्यात्म हो या लोक-कल्याण, भक्ति हो या मनोरंजन की राह खुलती है। सब एक-दूसरे से जुड़ कर अर्थवान होते हैं। हमारे विचार, शब्द और काम मिलजुलकर जिन रिश्तों का संगीत रचते हैं उसको लगातार संजोने और संवारने की जरूरत होती है।
संसदीय लोकतंत्र की राह पर चलते हुए देश ने कई पड़ाव पार किए हैं। अब तक अनेक विचारधाराओं के दलों को सरकार बनाने का अवसर मिला है और आभिजात्य वर्ग का वर्चस्व टूटता दिख रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। इनके बावजूद धन-बल और बाहु-बल की भूमिका बढ़ती गयी है। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ती राजनैतिक पैठ नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में जनहित को हाशिए पर धकेल देता है।
आशा की किरण भारत की नई पीढ़ी है। युवतर हो रहे भारत के युवक युवतियों में कई तरह के विचार हिलोर लेते रहते हैं। वे अक्सर उत्साह और प्रेरणा से सराबोर रहते हैं। ज़रूरी है कि उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जहां वे जीवन मूल्यों को ग्रहण कर सकें। वहाँ उत्साहवर्धक अनुभव और विमर्श का अवसर पैदा कर भारत का भविष्य संवारा जा सकता है।
गिरीश्वर मिश्र