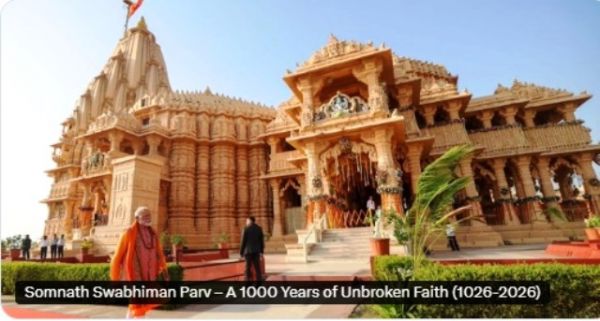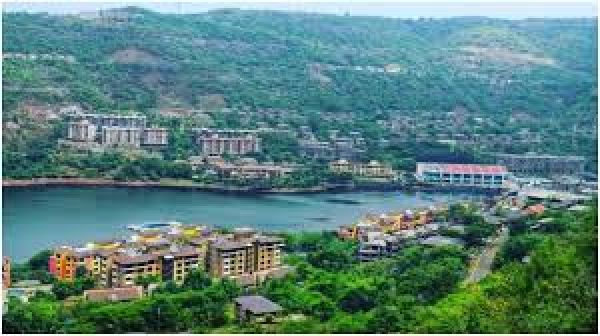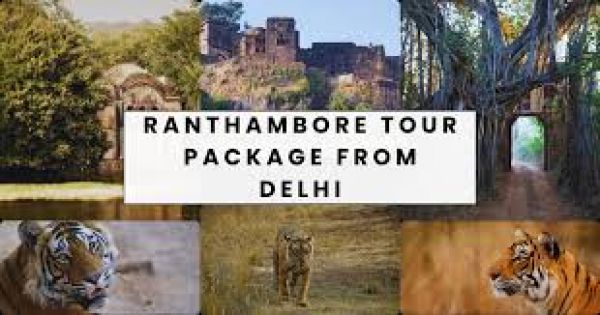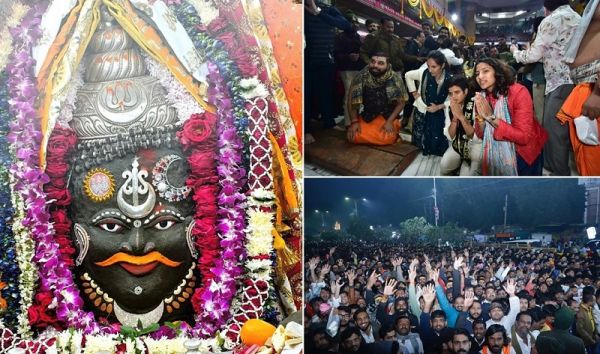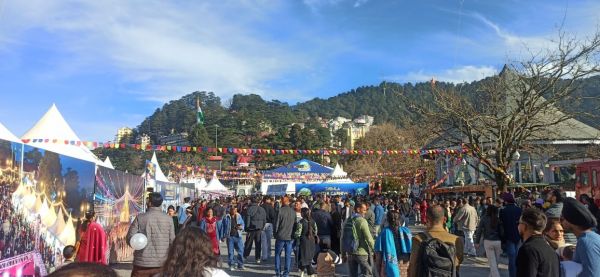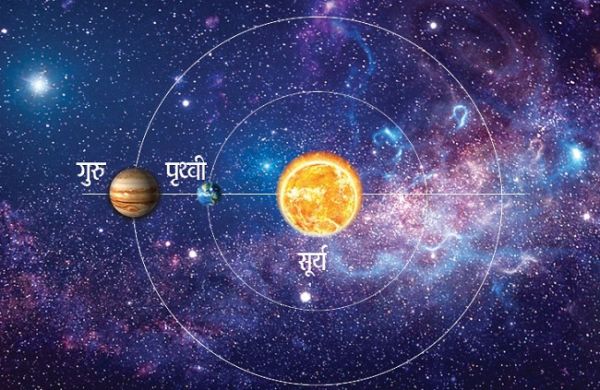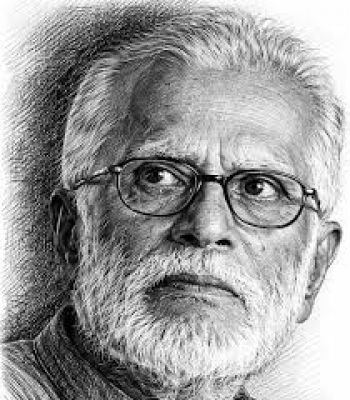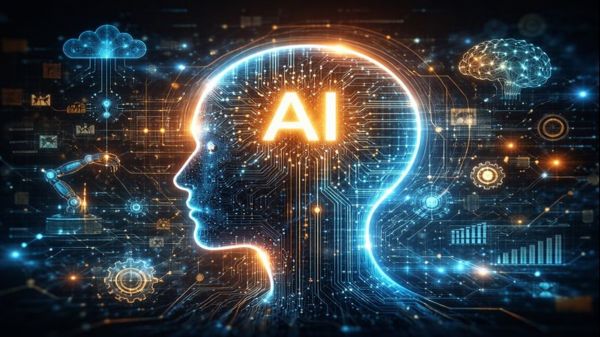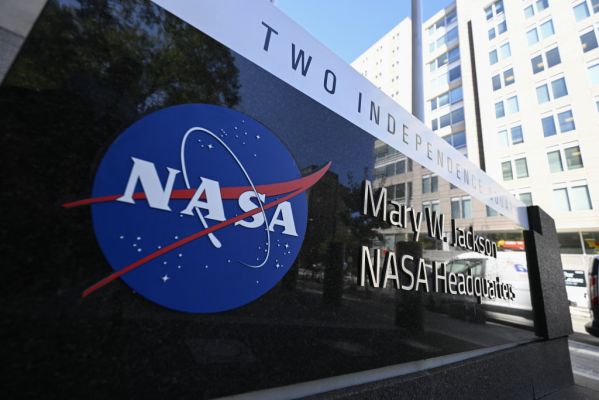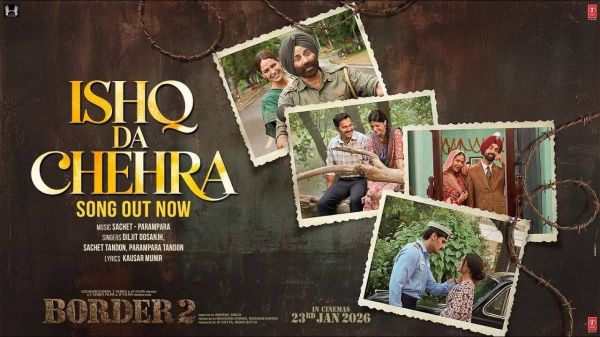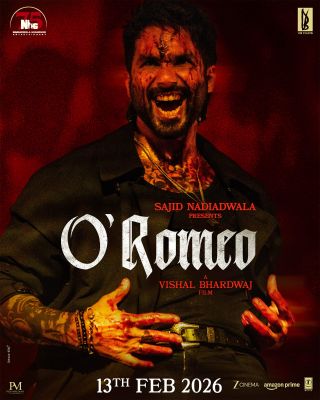भारत में ऐसी कई आदिवासी जनजातियां रहती है, जिनके बारे में बहुत ही कम जानकारियां हमारे पास उपलब्ध है, इन्हीं जनजातियों में से एक है, मुंडा जनजाति, तो आज के हमारे इस लेख में हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं।
‘मुंडा’ संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा ओके प्राचीन हिंदू पड़ोसी उन्हें ‘मुंडा’नाम से पुकारते थे। इस समुदाय के लोगों को ‘कोल’ भी कहा गया। मुंडा अपने को ‘होरो को’ (मनुष्य) कहते हैं। वह अपने को कोल कहलाना पसंद नहीं करते,यद्यपि मुंडा के जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उनकी भाषा में इसका अर्थ होता है, ‘विशिष्ट व्यक्ति’ । विशेष अर्थ में इस शब्द का मतलब था –गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड के रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, जिलों में बसे हुए हैं। मुंडा ओं का सबसे सघन जमाव रांची जिले में है।
मुंडा जनजाति का संबंध आष्ट्रेलायड प्रजाति समूह से है। इनकी त्वचा का रंग काला, नाक मोटी, चौड़ी व जड़ से दबी हुई, हॉट मोटे, सिर लंबा एवं कद छोटा होता है।
गोन गीत : अपने मूल स्वभाव से गेना-गीत, जदुर-गीतों के ही पूरक हैं, जो नृत्य की सुविधा के लिए बनाये गये हैं। बहुधा दो जदुर-गीतों के बाद गेना गाया जाता है, जो जदुर-नृत्य की ताल को थोड़ी देर के लिए बदल देता है।
जदुर के कठिन आरोह-अवरोह के बाद गेना के सरल नृत्य में थोड़ा आराम मिलता है और वातावरण की एकरुपता में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, जो रात-रात भर चलने वाली लघुतर बनाने के लिये गेना-गीतों की पंक्तियाँ भी छोटी-छोटी रखी गई हैं।
करमा : करमागीत भाव, लय और लोकप्रियता की दृष्टि से जदुर-गीतों से भी आगे बढ़े हुए हैं। सरहुल की समाप्ति से ही करमा-गीतों का प्रारम्भ होता है। मुण्डा जनजाति के लोग सरहुल की अन्तिम सन्ध्या आने के पहले ही, उसी दिन के धुँधले प्रभात में दो-चार करमागीत गाकर करमा के महान् मौसम का स्वागत करते हैं। और फिर, इन गीतों का क्रम नित्य बदलते रहने वाले वातावरण में अपना रुप बदलता हुआ आश्विन के अन्त तक चलता है। भादव की शुक्ल एकादशी को करमापर्व मनाया जाता है और उस पर्व से भी सम्बद्ध बहुत से गीत हैं; किन्तु दरअसल, करमागीत पर्व की सीमाओं में बँधे हुए नहीं हैं। अपने प्रकृत रुप में वे एकान्त संगीत हैं, जो गरमा में वन वृक्षों की शीतल छाया में, अषाढ़ की काली घटाओं में, बरसात की एकान्त खेतों में और भादव की सूनी राहों में समान रुप से गाये जाते हैं। वास्तव में, बरसात के दृश्य इन पहाड़ी भागों में बड़े मोहक हो जाते हैं। धरती पर छाई हुई हरियाली, बादलों के गंगाजल से धुले हुए जंगल, घास और झुरमुटों की चादर ओढ़े पहार, खेतों में कुलकालाता हुआ पानी, रात की नि:स्तब्धता, झींगुरों की झनकार, पक्षियों की चहचहाहट, धरती से आकाश तक के सारे दृश्य और क्षण क्षण परिवर्तित प्रकृति के रुप बड़े प्रभावशाली होते हैं, जी मुण्डाओं के मस्त स्वभाव को छेड़े बिना नहीं रह सकते।
एकान्त के क्षणों में उन्ही क्षणों के लिए बने होने के कारण करमागीतों का प्रभाव बड़ा गहरा होता है। और उनके कम्पित स्वर तथा लय की लहरों का बड़ा मधुर विकास हुआ है। सूनेपन की टेर उनके स्वरों को ऊंचा उठाती है और दर्द उनमें कम्पन पैदा करता है। जंगल के किसी एकान्त से खुलकर गाये हुए करमागीत प्रकृति के चरणों में पुरुष की चिरन्तन प्रकार के समान जान पड़ते हैं। मानो प्रणयातुर धरती, आकाश को अपने मिलन का विह्मवल सञ्देश सुनी रही हो। करमा गीतों का अर्थ वही है जो दूर क्षितिज के ऊपर उठती हुई काली घटाओं में बगुलों की पंक्ति का अर्थ है; जो ठण्डी हवा के साथ खुली खिड़की से आकर बदन को सिहरा देने वाली भाप की फुहारों का अर्थ है, जो आषाढ़ के पहले पानी पाकर धरती से उठने वाली सोंधी-सोंधी गन्ध का अर्थ है और जो सूनी रात के बेचैन कानों में दूर से आने वाली बाँसुरी की करुण पुकार का अर्थ है।
करमा पर्व मुण्डा जाति के लोगों का बहुत पुराना पर्व नहीं है। ऐसा लकता है कि इस पर्व को उन्होंने दूसरों से सीखा है। किन्तु, उसमें अपना रंग मिलाकर उसे और भी रसमय बना लिया है। अस्तु; पर्व के लिये भी बहुत से गीत बने हैं। करमा के अलग नृत्य हैं और बाजों के अलग लय-ताल हैं।
करमा गीतों में कृष्णकाव्य और रामायण की भी बहुत सी कथाएँ गाई जाती हैं। मुण्डा जाति का कृष्णकाव्य प्रीतपला के नाम से और रामकता रामायाण के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे गीतों में पूर्णता है और भावों की अभिव्यंजना अधिक मार्मिक और कलापूर्ण। ये शिक्षित गीतकारों द्वारा रचे गए हैं। इन्हें "बुदू बाबू' नामक एक पाँच परगना (खूँटी अनुमण्डल का पूर्वी भाग पाँच परगना कहलाता है) निवासी कवि एवं गीतकार ने बनाया है। इनमें चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनों का प्रभाव और बँगला गीतों की रसमयता है।
अधिकांश करमा गीतों की पंक्तियाँ लम्बी होती हैं, जो गाते समय खींचकर और भी बढ़ा ली जाती हैं। उनके स्वरों का आरोह, जो इन्हें अन्य गीतों में प्रमुखता प्रदान करती हैं।