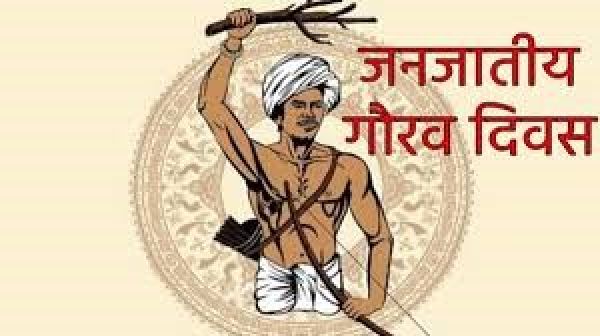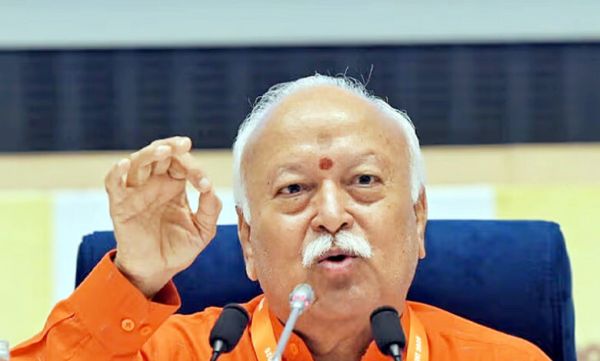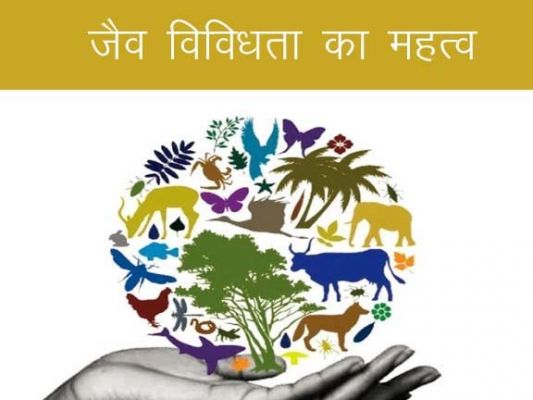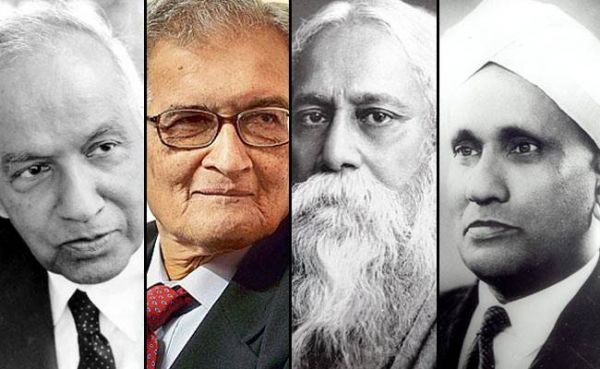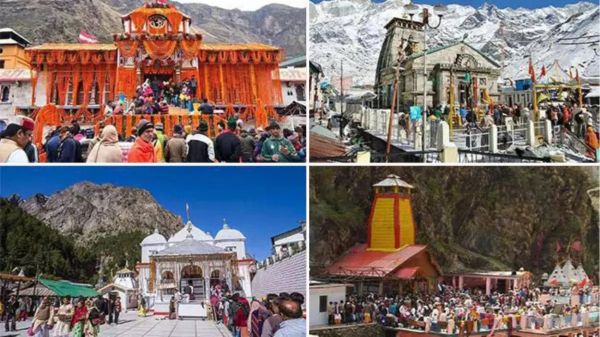दिल्ली में हाल ही में उजागर हुए फिदायीन मॉड्यूल ने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कट्टरपंथ का जाल हमारी सामाजिक संरचना में कितनी गहराई तक पैठ चुका है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इस मॉड्यूल में शामिल दानिश और उमर जैसे युवा चिकित्सक थे-ऐसे प्रशिक्षित पेशेवर, जिनका पहला कर्तव्य मानव-जीवन की रक्षा है। लेकिन वे जिहादी विचारधारा से संचालित होकर आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहे थे। यह घटना केवल एक आतंकी षड्यंत्र नहीं बल्कि गहन सामाजिक-धार्मिक संकट का संकेत है, जिसे मुस्लिम समाज सहित पूरे देश को समझना होगा।
अक्सर यह कहा जाता है कि “आतंकी का कोई मज़हब नहीं होता।” यह वाक्य साम्प्रदायिक तनाव से बचने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन तथ्यों की दुनिया में इसकी सीमाएँ हैं। यह एक कटु सत्य है कि विश्वभर में अनेक आतंकी हमले ऐसी विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं- चाहे वह अल-कायदा हो, आईएसआईएस, तालिबान या आईएम जैसे संगठन। यह विचारधारा इस्लाम की मुख्यधारा नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि दानिश और उमर जैसे शिक्षित युवक इसी उग्रवादी नैरेटिव के प्रभाव में आए बिना फिदायीन बनने की राह पर नहीं चलते। समस्या को पहचानना समाधान का पहला और अनिवार्य कदम है।
कट्टरपंथ का सबसे खतरनाक रूप यह है कि यह केवल गरीब, अशिक्षित या वंचित समाज पर निर्भर नहीं रहता। दुनिया के अनेक आतंकवादी मॉड्यूल में बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवक शामिल पाए गए हैं। उच्च शिक्षा कई बार कट्टर विचारधारा को अधिक बौद्धिक तर्क प्रदान कर देती है, जिससे व्यक्ति अपने कदम को “धार्मिक कर्तव्य” या “उम्मत की सेवा” की संकल्पना के भीतर सही ठहराता है। दानिश और उमर इसी वैश्विक पैटर्न के उदाहरण हैं—जहाँ पढ़े-लिखे युवक भी झूठे धार्मिक रोमांच और शहादत के भ्रम में अपने जीवन को विनाश की ओर धकेल देते हैं।
कट्टरपंथ का बीजारोपण अचानक नहीं होता। यह वर्षों तक धीरे-धीरे पनपता है- पहले पहचान आधारित भावनाएँ उभारी जाती हैं, फिर “हम बनाम वे” की खतरनाक मानसिकता पैदा की जाती है। पीड़ित भाव (victimhood) को धार्मिक कर्तव्य से जोड़ कर बताया जाता है कि पूरी दुनिया इस्लाम के विरुद्ध साजिश कर रही है। इसके बाद सोशल मीडिया, विदेशी नेटवर्क और गुप्त ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से युवाओं को विश्वास दिला दिया जाता है कि हिंसा कोई अपराध नहीं बल्कि “जन्नत का रास्ता” है। कट्टरपंथ की यह साइलेंट प्रक्रिया मस्जिद, मदरसा, परिवार और मोबाइल- चारों दिशाओं से समान रूप से चलती है।
ऐसे में सवाल उठता है कि समाधान केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर ही क्यों छोड़ा जाए? जिस समाज से प्रभावित युवक निकलते हैं, उस समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से विचार करना होगा कि क्या उनकी धार्मिक शिक्षा, आधुनिक और व्यावहारिक है? क्या मस्जिदों के इमाम अपने भाषणों में कट्टरपंथ को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं? परिवार क्या अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर सतर्क है? क्या समुदाय में प्रगतिशील आवाजों को समर्थन मिलता है? यदि इन सभी सवालों का जवाब ‘नहीं’ की ओर इशारा करता है, तो आत्ममंथन आवश्यक है।
कट्टरपंथ का सबसे गहरा और दीर्घकालिक नुकसान स्वयं मुस्लिम समाज को होता है। प्रत्येक आतंकी घटना के बाद पूरा समुदाय संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे उसकी कोई गलती न हो। पढ़े-लिखे युवाओं पर नौकरी और अवसरों में अविश्वास बढ़ता है। प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आवाज दब जाती है और सामान्य मुसलमान भी सामाजिक संदेह का बोझ झेलते हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज जितनी दृढ़ता से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा होगा, उतनी ही तेजी से वह स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित रख पाएगा।
समाधान कठोर भी होना चाहिए और न्यायपूर्ण भी- मदरसा शिक्षा में आधुनिक पाठ्यक्रम जोड़ा जाए, मस्जिदों में जिम्मेदार और संयमित भाषण अनिवार्य हों, कट्टरपंथ फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और परिवार अपने बच्चों को धार्मिकता और कट्टरता के बीच अंतर समझाएँ। बहुसंख्यक समाज की भूमिका भी जिम्मेदार होनी चाहिए- उकसावे, नफरत और भीड़-मानसिकता से बचते हुए कानून, सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा बनाए रखना।
दानिश और उमर का मामला केवल अराजकता या षड्यंत्र नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कट्टरपंथ की जड़ें समाज के भीतर तक पहुँच चुकी हैं। भारत के करोड़ों शांतिप्रिय मुसलमान इस देश की उम्मीद और ताकत हैं। उनका आगे आकर कट्टरपंथ की निंदा करना, युवाओं को सचेत करना और समाज में सौहार्द का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी उठाना आवश्यक है। कट्टरपंथ किसी एक समुदाय का नहीं पूरे देश का शत्रु है और उसकी हार तभी संभव है जब समाज, समुदाय और राज्य तीनों मिलकर उसके विरुद्ध एकजुट हों।
कृष्ण मोहन शर्मा





.jpg)
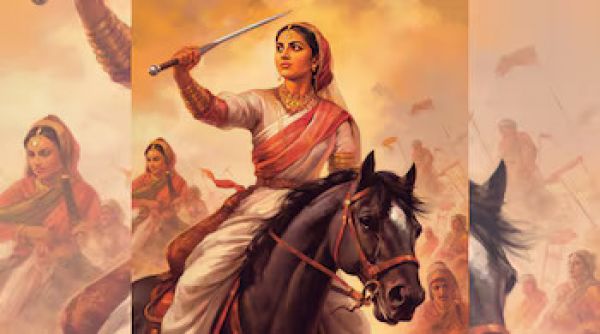


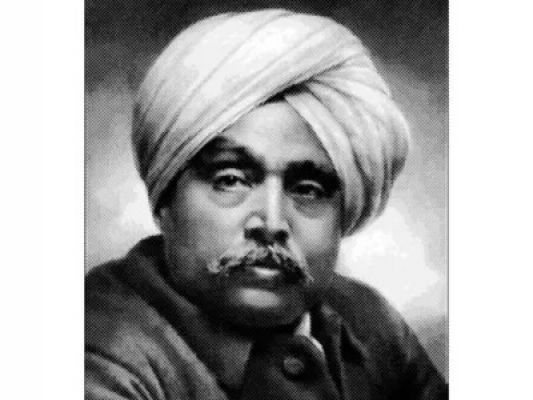

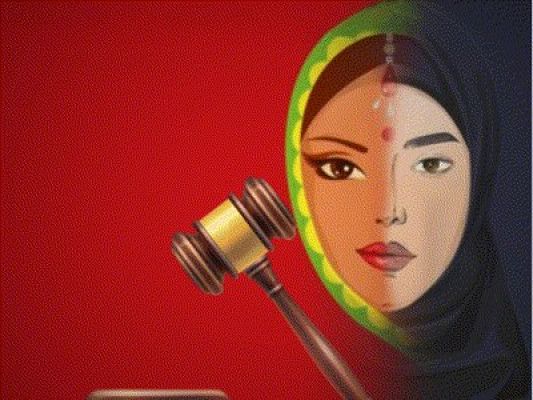
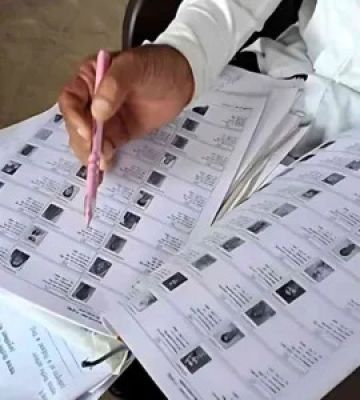


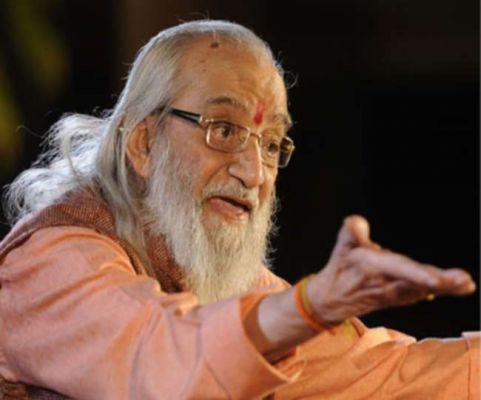
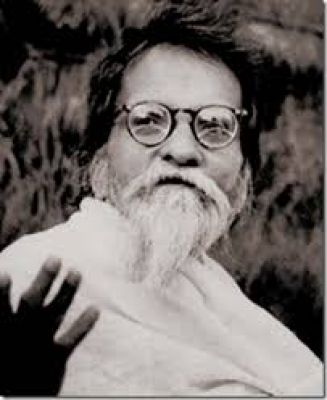
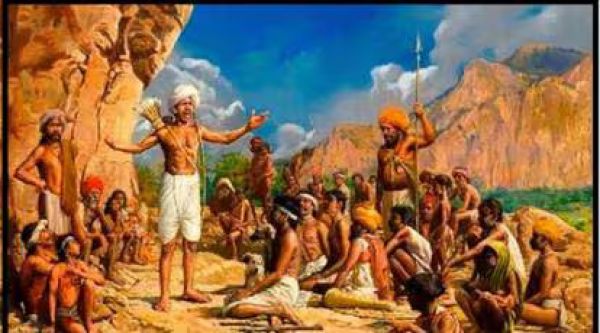
.jpg)