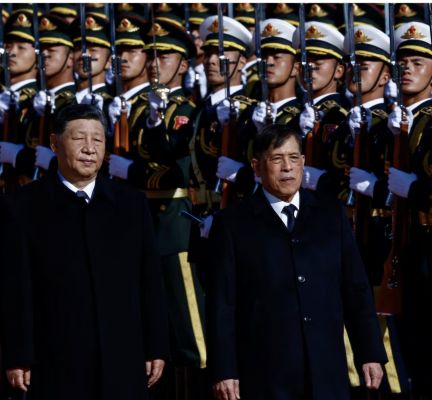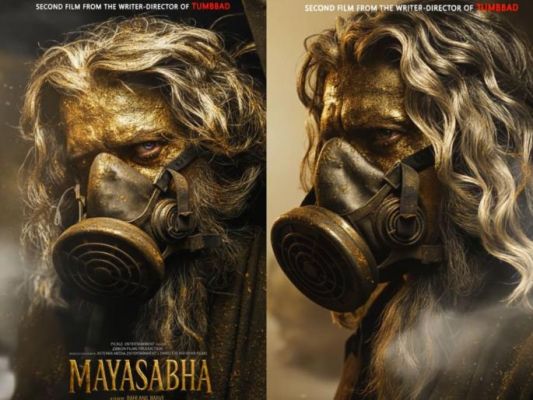कुलभूषण उपमन्यु
जैव विविधता मानव जीवन और आर्थिक संपन्नता का आधार है। प्रकृति जैव विविधता के माध्यम से ही सृष्टि की एक-दूसरे पर आधारित व्यवस्था को चलाती है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र करोड़ों एशियावासियों के लिए आजीविका और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाता है। भारतीय हिमालय वनस्पति, वन्य प्राणी, ग्लेशियर, बर्फ, पारंपरिक ज्ञान, और पर्वतीय कृषि विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। गंगा और सिंध के मैदानों को हरा-भरा बनाने वाली नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय बहुत संवेदनशील है। यह दुनिया के 34 जैव विविधता के लिए सबसे संवेदनशील स्थलों में से एक है। हिमालय के वन इसकी जैव विविधता के मुख्य आधार हैं। वनस्पति और वन्यप्राणी विविधता स्वस्थ वनों के बिना संभव ही नहीं है। बढ़ती आबादी, वन उत्पादों की बढ़ती मांग, और प्रबन्धन की कमियों के चलते वन संसाधन और वनों पर आधारित जैव विविधता घटते जा रहे हैं। जिससे हिमालय परिस्थिति तंत्र द्वारा दी जाने वाली अनेक पर्यावरणीय सेवाएं भी खतरे में पड़ती जा रही हैं।
हिमालय के वनों द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं का वार्षिक मूल्य, 1150 डॉलर प्रति हेक्टेयर आंका गया है। हिमालय में 18440 वनस्पति प्रजातियां, 1748 जड़ीबूटी प्रजातियां, 675 कंद मूल फल प्रजातियां चिह्नित की गई हैं। हिमालय द्वारा दी जाने वाली मुख्य पर्यावरणीय सेवाएं निम्न हैं- फल, चारा, ईंधन, खाद, रेशा, और दवाई, चरागाह, और अन्य गैर इमारती वन उत्पाद प्रदान सेवाएं। जलवायु नियमन, वायु की गुणवत्ता नियमन, पानी की मात्रा और गुणवत्ता का नियमन, भूमि कटाव नियंत्रण, परागण, कीट नियंत्रण सेवाएं। मिट्टी निर्माण, उपजाऊ तत्वों का पुन:चक्रीकरण, पानी का चक्रीकरण, बर्फ और ग्लेशियर द्वारा वर्ष पर्यंत जल प्रदान सेवाएं। सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण मित्र पर्यटन, सौन्दर्य सेवाएं आदि।
जैव विविधता के विनाश से उपरोक्त सभी सेवाएं प्रदान करने की हिमालय की सामर्थ्य क्षीण होती जाएगी, जिससे भारतीय महाद्वीप में जीवनयापन के लिए कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनका समाधान संभव नहीं होगा। जैव विविधता के लिए खतरों का आकलन करने के लिए हिमालय को पांच हजार फुट से ऊंचे क्षेत्र और पांच हजार फुट से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र इन दो भागों में देख सकते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य खतरा निम्न कारणों से है, ज्यादा कीमती जड़ी-बूटियों का अति दोहन, कृषि में एकल प्रजाति खेती को प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन, बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्य, दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार आदि। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरे निम्न हैं- खरपतवार, वनों में लगने वाली आग, सुधार वानिकी के चलते एकल प्रजाति चीड़ आदि रोपण, अवैज्ञानिक तकनीक से सड़क निर्माण और अन्य परियोजना निर्माण, सांस्कृतिक एकरूपता के प्रयास, स्थानीय बोलियों और पारंपरिक ज्ञान का ह्रास आदि।
इन कारणों से जैव-विविधता के ह्रास के चलते जहां एक ओर ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बर्फ रेखा पीछे हट रही है। वहीं वनों में विविधता के घटने से जल संरक्षण में भी कमी आ रही है। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव खेती पर पड़ रहा है। सिंचाई के लिए क्षेत्रीय टकराव बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर खरपतवारों के आक्रमण के कारण बेकार हो चुकी चरागाहों के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में चारे का संकट खड़ा हो गया है। पंजाब और हरियाणा से तूड़ी लाकर कमी पूरी की जा रही है। यह तूड़ी पहाड़ों तक पहुंचते 10 से 15 रुपये किलो तक हो जाती है। इतनी महंगी घास से पशुपालन आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बनता जा रहा है। वनों में विविधता के नाश से अन्य वन्य प्राणियों के लिए भी भोजन का संकट पैदा हो गया है। इसलिए मानव-वन्यप्राणी टकराव बढ़ता जा रहा है। विशेषकर बंदर, सूअर, नीलगाय द्वारा फसलों को नुकसान के चलते किसान कई इलाकों में खेती छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। बेसहारा छोड़े जा रहे पशुओं के पीछे भी चरागाहों में खरपतवार के कारण घास उत्पादन समाप्त होना एक कारण है। जड़ी-बूटियों के नष्ट होने से स्थानीय स्तर पर मनुष्यों और पशुओं के इलाज की पारंपरिक व्यवस्थाएं और ज्ञान भी समाप्त होता जा रहा है। बौद्धिक संपदा कानूनों की जानकारी और जागरुकता के अभाव में बहुत सा पारंपरिक ज्ञान अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं द्वारा पेटेंट कानूनों का दुरुपयोग करके चुराया जा रहा है।
समय की जरूरत है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। 2002 में संसद ने जैव विविधता कानून पास करके इस दिशा में शुरुआती प्रयास किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि जमीनी संरक्षण कार्य तो ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना संभव है। इसलिए ग्राम पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबन्धन समिति को सशक्त, कार्यक्षम और जागरूक बनाना पड़ेगा। एक्ट में इन पंचायत स्तरीय जैव विविधता समितियों को वन्य और कृषि जैव विविधता संरक्षण का कार्य सौंपा गया है, किन्तु 2004 में बनाए नियमों द्वारा उसकी संरक्षण की भूमिका को कमजोर कर दिया गया है और केवल जैव विविधता रजिस्टर बनाने तक ही उसे सीमित कर दिया गया है। रजिस्टर का इतना तो लाभ हो सकता है कि कोई व्यापारिक संस्था यदि पारंपरिक ज्ञान की चोरी करके उसका पेटेंट लेने की कोशिश करे तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत रोका जा सकता है, किन्तु संरक्षण के काम को गति देने के लिए तो जमीनी स्तर पर पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को कार्यक्षम बनाना पड़ेगा।
कृषि क्षेत्र की जैव विविधता पर रासायनिक खेती प्रक्रियाओं का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। संकर बीजों और जीन संशोधित बीजों के कारण पारंपरिक न्यूक्लियस बीजों का विनाश हुआ है। जीन संशोधित बीजों से क्षैतिज संदूषण का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अभी कपास के लिए ही जीन संशोधित बीजों की अनुमति है। धान के लिए प्रायोगिक अनुमति पर कार्य हो रहा है। किन्तु इसके खतरों का अभी कोई अनुभव नहीं है। इससे किसानों की बीज आत्मनिर्भरता बीज कंपनियों की गुलाम हो जाएगी। कीटनाशकों ने तितलियों मधु-मक्खियों आदि किसान के मित्र कीटों को भी हानि पहुंचाई है। फसलों में घास मारने वाली दवाइयों ने एकल फसल खेती को प्रोत्साहित किया है, जबकि पहले पर्वतीय क्षेत्रों में कई फसलों को एक साथ बोने की परंपरा थी।
गेहूं के साथ चना, सरसों आदि लगते थे। मक्की के साथ श्री धान्य (मिलेट्स),उड़द आदि लगते थे। उत्तराखंड में बारानाजा की परंपरा थी, जिसमें बारह प्रकार के अन्न एक साथ उगाए जाते थे। नस्ल सुधार कार्यक्रमों ने पशु विविधता को भी नष्ट किया है। देसी पहाड़ी, साहिवाल, हरयाणवी आदि देसी नस्लों की अपनी खूबियां थीं। खास कर उनका दूध ए-2 किस्म का होता है जो पाचक और ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। जैव विविधता की रक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी वनस्पतियों और जीवों की उपयोगिता और गुणों की अभी तक विज्ञान को भी जानकारी नहीं है, जो जैव पदार्थ हमने खो दिया उसके गुणों से मानव समाज सदा के लिए वंचित हो जाएगा। परिस्थिति तन्त्र इतना पेचीदा और संवेदनशील होता है कि एक पदार्थ के लुप्त होने से उस पर निर्भर और कई जैव पदार्थ भी लुप्त हो जाते हैं। अत: विश्व समाज में विकास को टिकाऊ बनाने के लिए हमें जैव विविधता को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना होगा।
(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् हैं।)




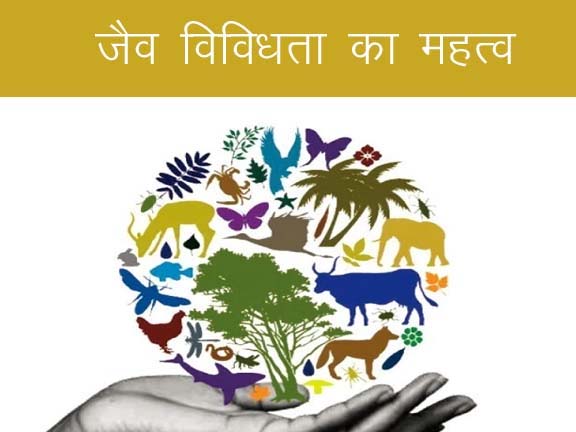
.jpg)
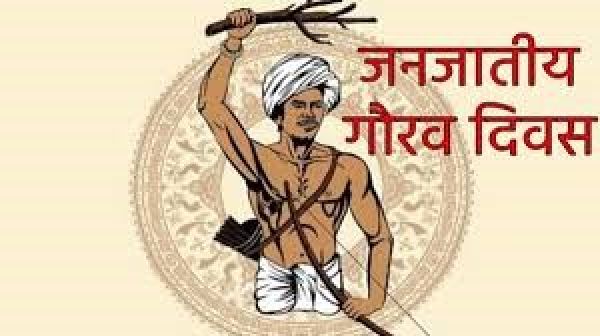
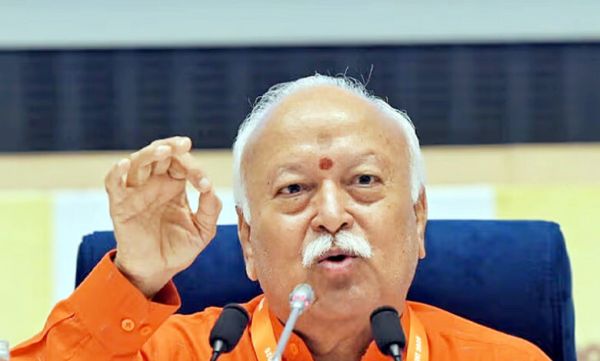

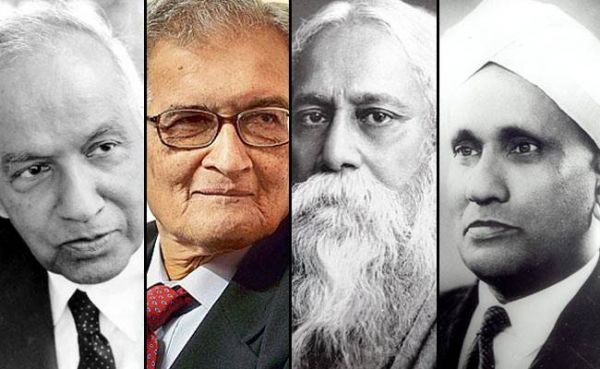
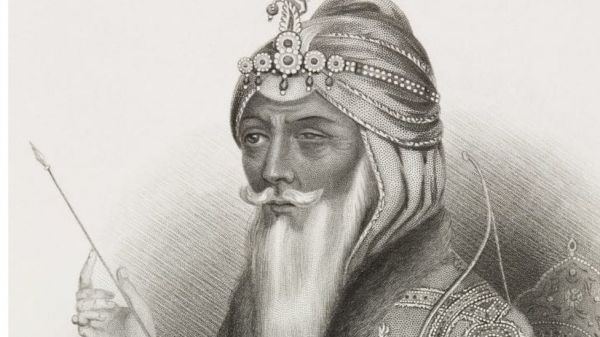




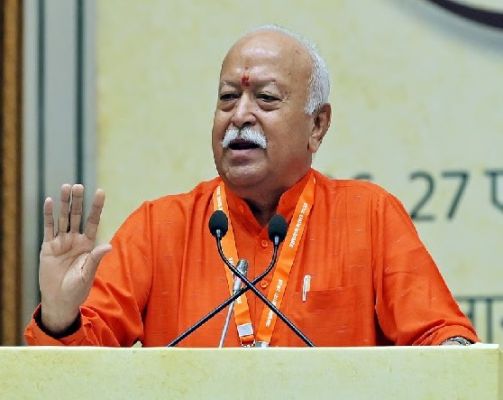







.jpg)