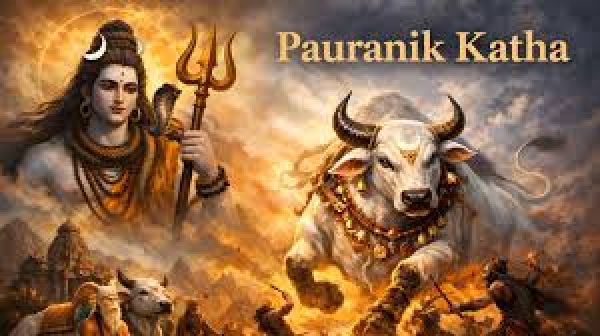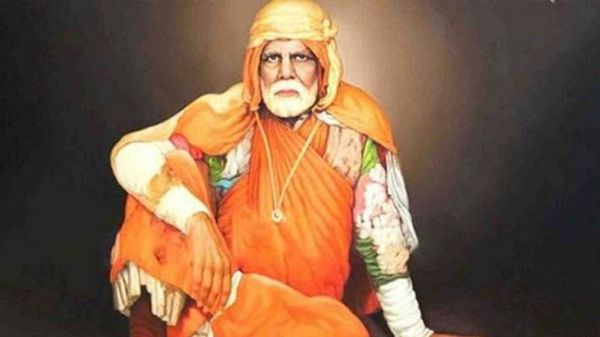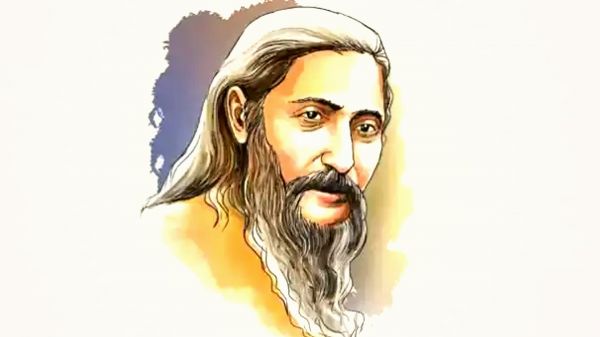भगवान राम की कथा पर आधारित रामलीला नाटक के मंचन की परंपरा भारत में युगों से चली आयी है। लोक नाट्य के रूप में प्रचलित इस रामलीला का देश के विविध प्रान्तों में अलग अलग तरीक़ों से मंचन किया जाता है। उत्तराखण्ड ख़ासकर कुमायूं अंचल में रामलीला मुख्यत: गीत-नाट्य शैली में प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः पूर्व में यहां की रामलीला विशुद्ध मौखिक परंपरा पर आधारित थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक मानस में रचती-बसती रही। शास्त्रीय संगीत के तमाम पक्षों का ज्ञान न होते हुए भी लोग सुनकर ही इन पर आधारित गीतों को सहजता से याद कर लेते थे। पूर्व में तब आज के समान सुविधाएं न के बराबर थीं स्थानीय बुजुर्ग लोगों के अनुसार उस समय की रामलीला मशाल, लालटेन व पैट्रोमैक्स की रोशनी में मंचित की जाती थी। कुमायूं में रामलीला नाटक के मंचन की शुरुआत अठारहवीं सदी के मध्यकाल के बाद हो चुकी थी। बताया जाता है कि कुमायूं में पहली रामलीला 1860 में अल्मोड़ा नगर के बद्रेश्वर मन्दिर में हुई। जिसका श्रेय तत्कालीन डिप्टी कलैक्टर स्व. देवीदत्त जोशी को जाता है। बाद में नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में क्रमशः 1880, 1890 व 1902 में रामलीला नाटक का मंचन प्रारम्भ हुआ। अल्मोड़ा नगर में 1940-41 में विख्यात नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर ने छाया चित्रों के माध्यम से रामलीला में नवीनता लाने का प्रयास किया। हालांकि पंडित उदय शंकर द्वारा प्रस्तुत रामलीला यहां की परंपरागत रामलीला से कई मायनों में भिन्न थी लेकिन उनके छायाभिनय, उत्कृष्ट संगीत व नृत्य की छाप यहां की रामलीला पर अवश्य पड़ी।
विशेषता
कुमायूं की रामलीला में बोले जाने वाले संवादों, धुन, लय, ताल व सुरों में पारसी थियेटर की छाप दिखायी देती है, साथ ही साथ ब्रज के लोक गीतों और नौटंकी की झलक भी। संवादों में आकर्षण व प्रभावोत्पादकता लाने के लिये कहीं-कहीं पर नेपाली भाषा व उर्दू की ग़ज़ल का सम्मिश्रण भी हुआ है। कुमायूं की रामलीला में संवादों में स्थानीय बोलचाल के सरल शब्दों का भी प्रयोग होता है। रावण कुल के दृश्यों में होने वाले नृत्य व गीतों में अधिकांशतः कुमायूंनी शैली का प्रयोग किया जाता है। रामलीला के गेय संवादो में प्रयुक्त गीत दादर, कहरुवा, चांचर व रूपक तालों में निबद्ध रहते हैं। हारमोनियम की सुरीली धुन और तबले की गमकती गूंज में पात्रों का गायन कर्णप्रिय लगता है। संवादों में रामचरितमानस के दोहों व चौपाईयों के अलावा कई जगहों पर गद्य रूप में संवादों का प्रयोग होता है। यहां की रामलीला में गायन को अभिनय की अपेक्षा अधिक तरजीह दी जाती है। रामलीला में वाचक अभिनय अधिक होता है, जिसमें पात्र एक ही स्थान पर खडे़ होकर हाव-भाव प्रदर्शित कर गायन करते हैं। नाटक मंचन के दौरान नेपथ्य से गायन भी होता है। विविध दृश्यों में आकाशवाणी की उद्घोषणा भी की जाती है। रामलीला प्रारम्भ होने के पूर्व सामूहिक स्वर में रामवन्दना “श्री रामचन्द्र कृपालु भजमन“ का गायन किया जाता है। नाटक मंचन में दृश्य परिवर्तन के दौरान जो समय ख़ाली रहता है उसमें विदूशक (जोकर) अपने हास्य गीतों व अभिनय से रामलीला के दर्शकों का मनोरंजन भी करता है। कुमायूं की रामलीला की एक अन्य ख़ास विशेषता यह भी है कि इसमें अभिनय करने वाले सभी पात्र पुरुष होते हैं। आधुनिक बदलाव में अब कुछ जगह की रामलीलाओं में कोरस गायन, नृत्य के अलावा कुछ महिला पात्रों में लड़कियों को भी शामिल किया जाने लगा है।