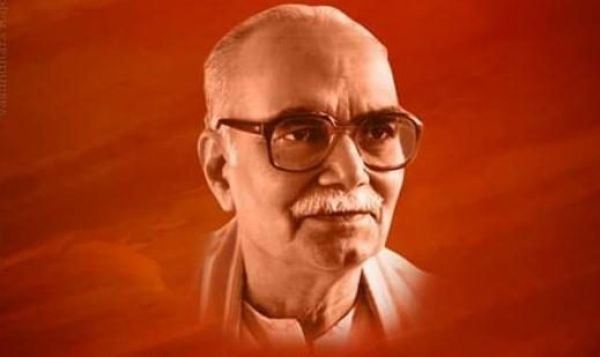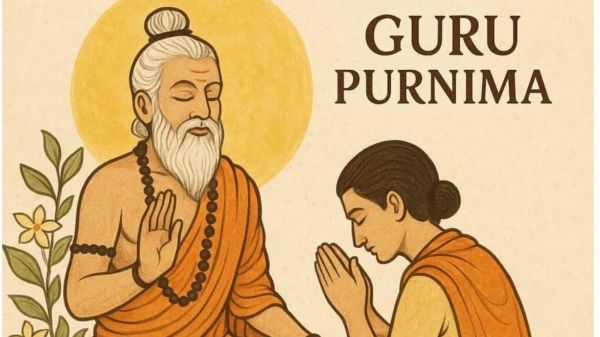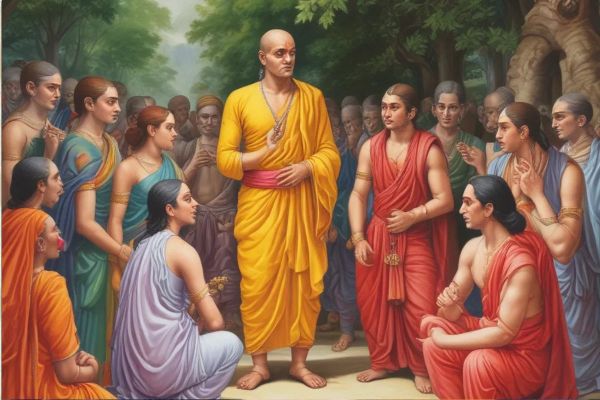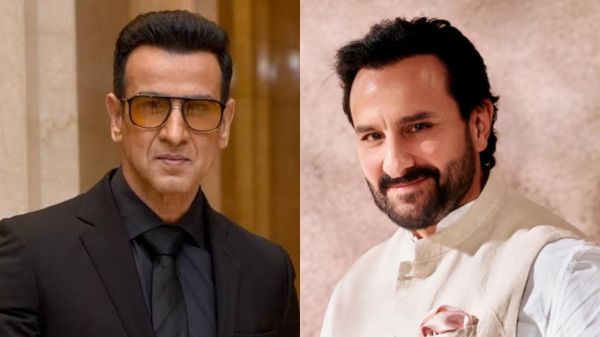नाबार्ड की इस साल मार्च में जारी रिपोर्ट से जहां संतोष होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रवाह का दायरा बढ़ा है, वहीं यह चिंता की बात है कि जरूरत के समय गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने वाले ग्रामीणों में करीब साढ़े सात फीसदी लोगों को 50 फीसदी से भी अधिक ब्याज दर से कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इससे साफ है कि एक बार गैर संस्थागत स्रोत से कर्जदार बने तो फिर कर्ज के मकड़जाल से निकलना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है।
नाबार्ड की रिपोर्ट को आधार मानकर चलें तो पिछले साल सितंबर में जुटाये गए आंकड़ों के अनुसार 17.6 फीसदी लोग अपनी तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर हैं। हालांकि इसमें करीब साढ़े तीन फीसदी का सुधार है। पहले 21.1 प्रतिशत ग्रामीण अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर थे। हमारी ग्रामीण संस्कृति की इस खूबी की सराहना करनी पड़ेगी कि आज भी 31.7 प्रतिशत रिश्तेदार या परिचित ऐसे हैं जो दुःख-दर्द में भागीदार बनते हैं और ऐसे समय में उपलब्ध कराये गये धन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। रिश्तेदारों या परिचितों से इस तरह की धन की आवश्यकता कुछ समय के लिए ही होती है और समय पर लौटा दिया जाता है। यह तथ्य भी नाबार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट से ही उभर कर आया है।
चाहे ग्रामीण हों या शहरी ऐसी आवश्यकताएं आ ही जाती हैं, जिनके लिए तत्काल धन की जरूरत होती है। अन्य कोई सहारा नहीं देखकर व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिश्तेदार, परिचित, साहूकार, दोस्त, कमीशन एजेंट या रुपये उधार देने वाले लोगों के सामने हाथ पसारते हैं। अब इनमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाने में किसी तरह का गुरेज नहीं करते और मजबूरी का फायदा उठाते हुए 50 से 60 प्रतिशत तक ब्याज लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। रिपोर्ट के अनुसार ऋण लेने वाले करीब 40 फीसदी ग्रामीणों को 15 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ता है। 0.9 प्रतिशत को 60 प्रतिशत या 6.6 फीसदी को 50 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर ऋण को चुकाना पड़ता है। साफ है कि आजादी के 75 साल बाद भी सूदखोरों का बोलबाला बना हुआ है। संस्थागत ऋणों में भी यदि हम पर्सनल लोन की बात करें तो वह भी करीब 15 से 20 प्रतिशत पर बैठता है और यदि किसी कारण से कोई किस्त बकाया रह गई तो पेनल्टी दर पेनल्टी का सिलसिला काफी गंभीर व कर्ज के मकड़जाल में फंसाने वाला हो जाता है।
एक बात और, शहरों और ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों या संस्थाओं द्वारा दैनिक आधार पर पैसा कलेक्शन करने और दैनिक आधार पर ऋण देने का कार्य किया जाता है। इस तरह के लोगों या संस्थाओं द्वारा भले दैनिक आधार पर दस रुपये के ग्यारह रुपये शाम को देना आसान लगता हो पर इस किस्त का चूकना और मासिक आधार पर गणना की जाये तो यह बहुत मंहगा होने के साथ जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से कम नहीं है। रोजमर्रा का काम करने वाले वेण्डर्स इस तरह की श्रेणी में आते हैं। कहने को चाहे 40 प्रतिशत ही हो पर इनके द्वारा 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की ब्याजदर से ब्याज राशि वसूलना किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता।
देश में संस्थागत ऋण उपलब्धता बढ़ी है पर ताजा रिपोर्ट के अनुसार 17.6 प्रतिशत ग्रामीणों का साहूकारों या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना उचित नहीं माना जा सकता। यदि ब्याज दर 20, 30, 40 या 50 प्रतिशत होगी तो प्रेमचंद के गोदान या इसी तरह की साहूकारी व्यवस्था व आज की व्यवस्था में क्या अंतर रह जाएगा। इतना जरूर है कि रिश्तों की डोर आज भी मजबूत है और इसकी पुष्टि नाबार्ड की रिपोर्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में 31.7 प्रतिशत कर्जदार रिश्तेदारों और परिचितों पर निर्भर हैं। ये लोग रिश्तों का लिहाज करते हुए जरूरत के समय एक-दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं और बदले में किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। आने वाले समय में भी हमें रिश्तों की इस डोर को मजबूत बनाये रखना होगा और सरकार को आगे आकर एक सीमा से अधिक ब्याज वसूलने वालों पर सख्ती दिखानी होगी।
लेखक - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)