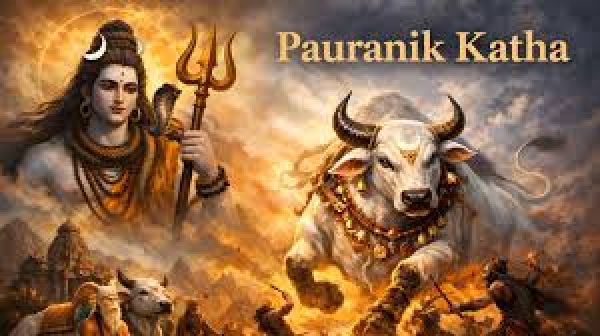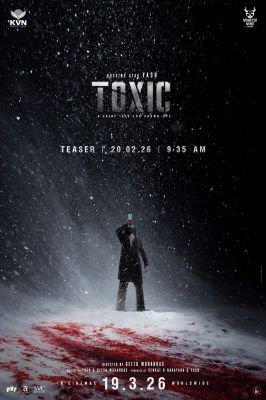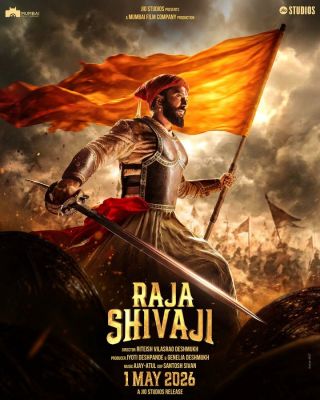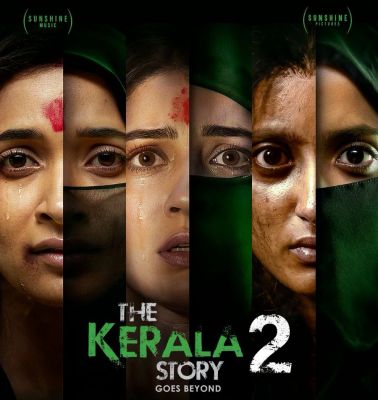भारत के आदिवासी कलाओं में बस्तर की आदिवासी परंपरागत कला कौशल प्रशिद्ध है। जनजातीय कलाओं में प्रमुख बस्तर कला है जो भारत के बस्तर-क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा प्रचलित है और अपने अद्वितीय कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बस्तर के आदिवाशी समुदाय अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे है, परन्तु प्रचार के आभाव में यह केवल उनके कुटीरों से साप्ताहिक हाट बाज़ारों तक ही सीमित है। उनकी यह कला बिना किसी उत्कृष्ट मशीनों के उपयोग के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले उपक्रमों से ही बनाये जाते हैं। बस्तर के कला कौशल को मुख्य रूप से काष्ठ कला, बाँस कला, मृदा कला, धातु कला में विभाजित किया जा सकता है। काष्ठ कला में मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचरों में बस्तर की संस्कृति, त्योहारों, जीव जंतुओं, देवी देवताओं की कलाकृति बनाना, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, साज सज्जा की कलाकृतियाँ बनायी जाती है। बांस कला में बांस की शीखों से कुर्सियां, बैठक, टेबल, टोकरियाँ, चटाई, और घरेलु साज सज्जा की सामग्रिया बनायीं जाती है। मृदा कला में , देवी देवताओं की मूर्तियाँ, सजावटी बर्तन, फूलदान, गमले, और घरेलु साज-सज्जा की सामग्रियां बनायी जाती है। धातु कला में ताम्बे और टिन मिश्रित धातु के ढलाई किये हुए कलाकृतियाँ बनायीं जाती है, जिसमे मुख्य रूप से देवी देवताओं की मूर्तियाँ, पूजा पात्र, जनजातीय संस्कृति की मूर्तियाँ, और घरेलु साज-सज्जा की सामग्रियां बनायीं जाती है।
बस्तर जिला वनों से ढका हुआ है। यह भारत में उपस्थित जनजातिय समुदाय का बड़ा हिस्सा यहाँ निवासरत है | बस्तर शिल्प की दीवार दुनिया भर में कला उत्साही और विशेषज्ञ का ध्यान आकर्षित करते हैं। बस्तर कलाकृतियों आमतौर पर जनजातीय समुदाय की ग्रामीण जीवनशैली को दर्शाती है|
आदिवासी निश्चित रूप से भारत के पहली धातु स्मिथ थे और वे अभी भी प्राचीन अभ्यास के साथ जारी हैं। ये जनजातीय कलाकार धातु की पुरानी प्रक्रियाओं के माध्यम से, जीवन, प्रकृति और देवताओं के अनूठे दृश्य को लोहे में उकेरते हैं । उनकी प्रक्रिया सरल है – इसमें मूल रूप से धातु को फोर्जिंग और हथौड़ा द्वारा रूप देना है।
बस्तर अंचल के हस्तशिल्प, चाहे वे आदिवासी हस्तशिल्प हों या लोक हस्तशिल्प, दुनिया-भर के कलाप्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि , इनमे इस आदिवासी बहुल अंचल की आदिम संस्कृति की सोंधी महक बसी रही है। यह शिल्प-परंपरा और उसकी तकनीक बहुत पुरानी है।
देवी त्यौहार , तीज त्यौहार, चैतराई, आमाखानी, अकती, बीज खुटनी, हरियाली, इतवारी, नयाखाई आदि बस्तर के आदिवासियों के मुख्य त्यौहार हैं। आदिवासी समुदाय एकजुट होकर बूढ़ादेव, ठाकुर दाई, रानीमाता, शीतला, रावदेवता, भैंसासुर, मावली, अंगारमोती, डोंगर, बगरूम आदि देवी देवताओं को पान फूल, नारियल, चावल, शराब, मुर्गा, बकरा, भेड़, गाय, भैंस, आदि देकर अपने-अपने गांव-परिवार की खुशहाली के लिए मन्नत मांगते है।
अबूझमाड़ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल के नारायणपुर जिले में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र तथा कुछ आंध्र प्रदेश मे पड़ता है। भारत मे विलुप्त होते बाघों के लिये यह क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह भारत के ६ प्रमुख बाघ आश्रय स्थलों क्रमश: इन्द्रावती, नल्लामल्ला, कान्हा, नागझीरा, ताडोबा और उदन्ती सीतानदी राष्ट्रीय उद्यान से जंगलो के द्वारा संपर्क मे है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अबूझ मतलब जिसको बूझना संभव ना हो और माड़ यानि गहरी घाटियां और पहाड़। यह एक अत्यंत दुर्गम इलाका है।
स्थिति
गुगल मैप के अनुसार लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में कोई सड़क नही है। यहां करीब 200 ऐसे गांव है जिनकी जगह बदलती रहती है क्योंकि यहां रहने वाले माड़िया आदिवासी जगह बदल बदल कर बेरवा पद्धती से खेती करते हैं।
परिस्थितियाँ
अबूझमाड़ और इसके निवासी आज तक अपने आदिकालीन स्वरूप में है। चूंकि यहां रहने वाले माड़िया आदिवासी बाहरी लोगों से संपर्क रखना पसंद नही करते, इस कारण अभी तक यहां पायी जाने वाली पेड़ पौधों और वन्य प्राणियो की संख्या और प्रकार के बारे में सही जानकारी नही है और यहां के बाघों की गणना भी नही हुई है। इसकी सीमा पर रहने वाले व्यापारी आज भी आदिवासियों से तेल और नमक का वनोंपज के साथ विनिमय करते है। आदिवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहा बाघ, वनभैंसा, गौर, सांभर चौसिंगा इत्यादि जीव प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां चीतलों की संख्या कम है।
सबसे बडी बात यह है कि यहां कभी वनों की कटाई नही हुई है और मध्य भारत में यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम हमारे मूल जंगलो मे पाई जाने वाली वनस्पतियों और वन्य प्राणियों जो जंगलों की कटाई कर उनका कोयला बना कर वहां सागौन नीलगिरी साल इत्यादि का रोपण करने के कारण विलुप्त हो चुके है का अध्ययन करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। और यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण भारत की अनेक नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है।