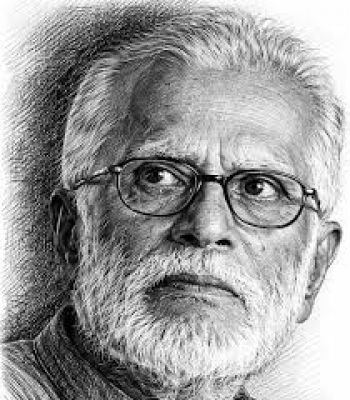23 मई बुद्ध पूर्णिमा विशेष - अत्ता हि अत्तनो नाथो !
Date : 22-May-2024
विचारक और अनुभवसिद्ध गौतम बुद्ध मानवता के इतिहास में कई दृष्टियों से आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। धर्म की स्थापना, ध्यान और मन के प्रशिक्षण तथा संघ की स्थापना जैसे कार्यों द्वारा वे एक महामानव के रूप में ढाई हजार वर्षों से वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके विचार प्रखर थे और सोचने का नजरिया साहसपूर्ण, जो उनके लगभग पांच दशकों के सक्रिय और कठोर भिक्षु-जीवन के दौरान विकसित हुआ था। उनकी सोच इस बात से शुरू होती है कि जीवन में हर कोई असंतुष्ट और बेचैन है। उन्हें जन्म और मृत्यु का बंधन एक बेड़ी जैसा लगा था। इसलिए इस बात में आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि दुःख से मुक्ति या निर्वाण (पूर्ण स्वातंत्र्य) उनके चिंतन और प्रयोग का परम लक्ष्य बन गया ।
ईस्वी पूर्व पांचवीं सदी में जब बुद्ध का आगमन हुआ था तब भारत में ब्राह्मणवाद और कर्मकांड का बोलबाला था। पर उसी दौर में आर्थिक बदलाव शुरू हो चुके थे। कृषि की सम्पन्नता से नगर विकसित हो रहे थे और सुदूर व्यापार भी हो रहा था। इस तरह के बाह्य सम्पर्क से भारत से बाहर की संस्कृतियों की जानकारी मिलनी शुरू हुई। यह भी पता चला कि जातिहीन मानव समाज भी होते हैं और दूसरी भाषाओं का उपयोग करते हैं। सामाजिक गतिशीलता के इस दौर में एक ऐसे धर्म की जरूरत महसूस हुई जो ब्राह्मण पुरोहितों, स्थानीय रीति-रिवाजों और प्राचीन मान्यताओं पर न टिका हो। उसी दौर में ब्राह्मणवाद का खंडन जैन मत भी कर रहा था। दूसरी ओर उपनिषद भी अस्तित्व में आ रहे थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने, ब्रह्म से सायुज्य और पुनर्जन्म से सदा के लिए मुक्ति के विचार प्रस्तुत कर रहे थे।
शाश्वत, अपरिवर्तनशील जगत का सार-तत्व ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित किया गया। कहा गया कि प्रत्येक जीवित प्राणी में स्थायी आत्मन् का वास होता है। वह आत्मन् ही ब्रह्म है- अहं ब्रह्मास्मि, तत् त्वम असि । यह सोच तत्ववाद की पराकाष्ठा थी। बुद्ध को लगा कि जीवन में इस तरह का अनुभव करना व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की संभावना को नकारता है। अकसर है या अस्ति (बीइंग) और जो हो रहा है या भवति (बिकमिंग) को दो छोर समझा जाता है। पहला स्थिर है तो दूसरा परिवर्तनशील । सत्यं, शिवं और सुंदरं को ब्रह्मन् का स्वरूप कहा गया। बुद्ध की समझ में हमारा अनुभव-जगत सतत परिवर्तनशील था। हमारी संतुष्टि भी परिवर्तनशील होती है और मृत्यु की भी छाया भी अनवरत बनी रहती है। परिवर्तन में पीड़ा, कुंठा या असंतोष भी बना रहता है।
बुद्ध ने अस्तित्व या जीवन के तीन लक्षण बताए: अस्थायित्व, असंतुष्टि, तथा अनात्त । वस्तुएं अस्थायी होती हैं और बदलती रहती हैं यह बात उपनिषद के विचार के ठीक उल्टी थी । बुद्ध की सोच कुछ इस तरह थी - यदि आत्म है तो इसका अर्थ होगा कि अस्तित्व अपरिवर्तनशील होगा और जीवन की प्रक्रियाओं में हमारी कोई भूमिका न होगी और हम उसका अनुभव भी न कर सकेंगे क्योंकि हमें अनुभव तो क्रिया का अर्थात् क्रम और उसके परिणाम का ही होता है। इसलिए वेदांत के विपरीत बुद्ध ने अन आत्मन या अनात्त का विचार रखा। बुद्ध ने सत्, चित् और आनंद वाली ब्रह्म की अवधारणा के विपरीत अनित्य, अविद्या और दुःख की सच्चाई को पहचाना। उन्होंने वेद, कर्मकांड और जाति-संस्था इन सबका खंडन किया। फिर ‘आर्य’ यानी सज्जन के संघ की बात की। ब्राह्मणवाद का तीव्र खंडन किया परंतु सांख्य दर्शन से जगत के प्रलय के कल्प-क्रम का विचार, योग से ध्यान के सिद्धांत, और न्याय-वैशेषिक से बहुलता का विचार और तर्क-पद्धति को ग्रहण किया।
दर असल जो बुद्ध के अनात्त के विचार को इस तरह देखते हैं कि बुद्ध व्यक्ति की निरंतरता और उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी से मुक्त करते हैं वह भ्रामक और ग़लत अर्थ निकालना है । बुद्ध कहते हैं कि हमारी निरंतरता हमारे कर्मों में बसती है और यह निश्चय ही व्यक्ति की निरंतरता का एक प्रबल विचार है। यह निरंतरता कई जन्मों तक खिंच सकती है जो निर्वाण मिलने पर ही रुकेगी। अस्तित्व (बीइंग) को लेकर भी बुद्ध ने विलक्षण स्थापना की। उपनिषद के मत में अस्ति ही सत्य या यथार्थ है। भवति (बिकमिंग) में अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों मिले होते हैं और जो बदलता है वह, जो नहीं बदलता उससे कमतर सत्य नहीं होता है। बुद्ध का विचार था कि अस्ति या बीइंग को एक श्रेणी मानने पर नैतिक और बौद्धिक सोच में मुश्किल खड़ी होती है। इस विचार को आत्मन के अस्तित्व के खंडन से जोड़ा गया। बुद्ध ने वस्तुतः हर तरह की अनिवार्यता (एसेंशियलिज्म) को नकारा।
बुद्ध का जोर कर्म पर था। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया । क्रिया सही या गलत हो सकती है। कर्म करना और भविष्य में (समानान्तर अच्छे बुरे) परिणाम इसे अभी या आगे के जन्म में अनुभव करने होंगे ही यह बात हिंदू, बौद्ध और जैन सभी स्वीकार करते हैं। आख़िर बीज बोएंगे फसल तो होगी ही ! कर्म का नैतिक मूल्य होता है। कर्ता के लिए अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा परिणाम होगा ही होगा। स्मरणीय है कि बुद्ध के पहले कर्म की अवधारणा कर्मकांड से जुड़ी हुई थी । जैन विचारकों ने उसके नैतिक पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया विशेष रूप से हिंसा को ध्यान में रख कर। बौद्ध मत ने नैतिकता के पक्ष को पुष्ट किया। वे कर्म को मंतव्य या कर्म करने की इच्छा (इंटेंशन) तक ले गए। मात्र विचार या मन की दशा से भी कर्म होता है।
वैसे तो सभी प्राणी समान नैतिक दायित्व रखते हैं परंतु जन्म के समय पूर्व जन्म के सभी कर्मों के अधीन होते हैं। पर आगे ठीक़ होने का अवसर मिलता है। अच्छे मंतव्य से मन पवित्र होता है। साथ ही ध्यान से भी शुद्धि होती है । बुद्ध ने यह आर्य सत्य देखा – दुःख सबको होता है। इच्छा दुःख का कारण है। हम वह सब चाहते हैं जो असंभव है। इच्छा न करना ही दुःख दूर करने का उपाय है। बुद्ध ने इससे उबरने के लिए नैतिक उपाय बताए। उनका आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक् पर ज़ोर देता है|सम्यक् आचरण, मानसिक प्रशिक्षण। चूंकि दुःख प्रत्येक व्यक्ति का निजी होता है समाधान भी उसी से जुड़ा होगा। यहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। हम सब अपने-अपने कर्म के लिए ज़िम्मेदार हैं। बुद्ध परम व्यावहारिक हैं। वे खुद को एक ‘शल्य चिकित्सक’ कहते हैं जो इच्छा के बाण को निकालता है। जैसे समुद्र का एक ही स्वाद होता है कि वह चारों ओर नमकीन होता है वैसे ही बुद्ध के सभी उपदेशों का एक ही अर्थ है – मुक्ति या निर्वाण।
बुद्ध की दृष्टि में हमारे जीवन में जो कुछ है और जो भी अनुभव होते हैं वे सिर्फ प्रक्रिया होते हैं। वे अनुभव का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यदि भिन्न जानकारी मिले तो अनुभव को ही प्रमाण मानो। कुछ भी कारण से स्वतंत्र नहीं होता है क्योंकि कारण आवश्यक पूर्वदशाएं हैं। सभी चीजें कारण से जुड़ी हैं या कहें सब कुछ कारण से पैदा होता है। पर इस विश्व का न आरंभ है न कोई अंतिम कारण है, हां कुछ कड़ियां जरूर होती हैं। विश्व में प्रक्रियाएं होती हैं जो यादृच्छिक (रैंडम) नहीं हैं पर बहुत स्पष्टता से निर्धारित भी नहीं हैं। कर्म नैतिक कारणता या दायित्व से जुड़ा होता है। पर कर्म ही एकमात्र कारण नहीं है। कर्म एक सामान्य दशा या परिप्रेक्ष्य पैदा करता है पर और भी कारण होते हैं जैसे बीमारी। नए कर्म में चुन सकते हैं पर एक सीमा के ही भीतर। कर्म को केंद्र में लाकर बुद्ध ने आत्म की जगह प्रक्रिया को स्थापित किया जो अनुभवगम्य है। वह परिवेश से जुड़ता है। कर्म के लिए सभी जिम्मेदार लोग प्रयास से निर्वाण पा सकते हैं।
स्मरणीय है कि ब्राह्मणवाद, जैसा-उपनिषदों में विकसित हुआ था तत्व पर बल देता था और अस्तित्व की सत्यता अस्ति (बीइंग) पर निर्भर थी । मुख्य सरोकार व्यक्ति के स्तर पर आत्मा की अमरता और ब्रहमन की शाश्वतता से था जो एक सार्वभौम नियम था। ब्रहमन अनिर्वचनीय था । उसकी व्याख्या के लिए शब्द अपर्याप्त थे। उसके वर्णन के लिए नेति-नेति कहा गया । उसकी व्याख्या सच्चिदानंद के रूप में की गई । वह अद्वितीय, अनादि, विभु, अनंत और सत्य था। इसके विपरीत बौद्ध दृष्टि तथता की थी और 'भवति' या होने की प्रक्रिया (विकमिंग) पर बल देती थी । स्थायी आत्मा का स्वीकार बुद्ध को कथमपि अनुकूल न था । उनको व्यक्तिगत या सार्वभौम किसी भी तरह की शाश्वतता स्वीकृति न थी। उनकी दृष्टि में 'अस्ति' की यदि कोई बात है तो वह सिर्फ क्षणिक है । चीजें अस्तित्व में आती हैं पर क्षण भर में ही कुछ और हो जाती हैं। यहां संसार में कुछ भी स्थिर नहीं। यह जगत जीवन-तरंगों का एक असमाप्य अंतहीन क्रम है। बुद्ध ने सर्व-धर्म-अनात्मता, सर्व-संस्कार-अनित्यता और सर्वं दु:खम के तीन सिद्धांत बताए। न तत्व, न क्षण, न सुख कुछ भी तो स्थायी नहीं है ! निर्वाण भी जीवन-दशाओं का नकार ही था। शुरू से ही बुद्ध के विचार में नकार की प्रबलता बनी रही। उन्हें सृष्टि, स्रष्टा, ईश्वर, कोई प्रथम कारण या किसी तरह का अद्वैतवादी विचार कुछ भी स्वीकार्य न था- न भौतिकवाद, न सुखवाद, न अतिशय वैराग्य।
मनुष्य और सभी जीवित प्राणी आत्मसंभव हैं। इस विश्व में सभी प्राणी एक कारण से नहीं दो या तीन कारणों से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होना पहले की स्थिति की एक शृंखला में घटित होते हैं। जीवन चक्र एक वृत्त है जिसके आरंभ का कोई पता नहीं है। काल की सत्ता एक चक्र की भांति है न कि सीधी रेखा के रूप में। काल सापेक्ष होता है। मृत्यु अंत नहीं है। उसके साथ-साथ तत्काल ही एक दूसरा जीवन शुरू होता है। एक जीवित प्राणी काल सापेक्ष्य हो कर आगे क्रम में चलता रहता है और बदलता रहता है। इस कर्ममय जगत में यदि अपने को प्यार करना है तो अपने को संभाल कर रखना होगा। बुरे कर्म करना आसान है परंतु हितकर कार्यों को करना कठिन है पर सुचरित धर्म का आचरण ही श्रेयस्कर है। वस्तुतः आदमी अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन हो सकता है : अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो पसो सिया ? अर्थात व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, भला कोई दूसरा उसका स्वामी कैसे हो सकता है?
लेखक - गिरीश्वर मिश्र




.jpg)