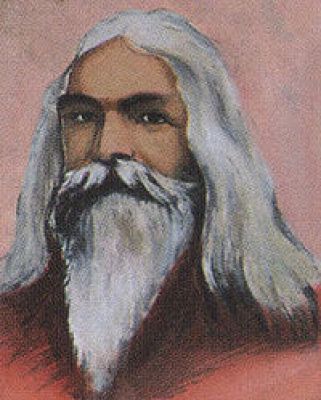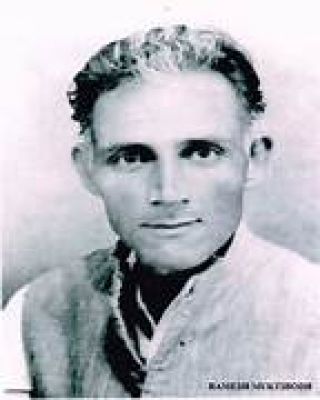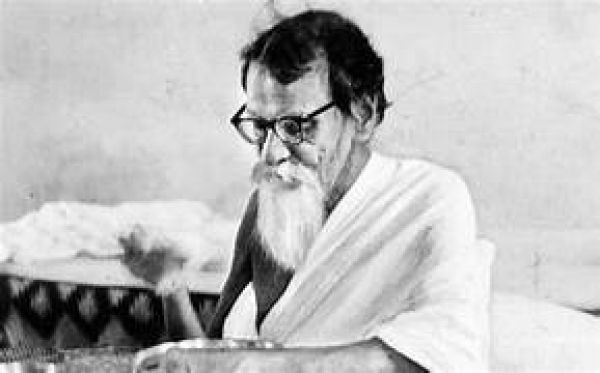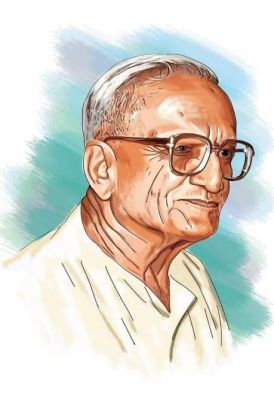मैक्रों की भारत और राहुल की फ्रांस यात्रा
जी-20 शिखर सम्मलेन में दुनिया के दिग्गज नेता सहभागी हुए। सभी ने एक स्वर में भारत के विचार प्रस्ताव और सत्कार को विलक्षण बताया। इन विदेशी मेहमानों को ऐसा उदार चिंतन पहले किसी अन्य सम्मेलन में देखने को नहीं मिला था। यह संयोग था कि इसी समय राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे। इसके पहले नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले भी राहुल गांधी ने संयोग बनाया था। मोदी की यात्रा से ठीक पहले वह अमे्रिका गए थे। उनकी प्रत्येक विदेश यात्रा में भारत की प्रतिष्ठा के अनुरूप कोई बयान नहीं होता। हर बार, हर जगह एक जैसे बयान। इस बार भी उन्होंने फ्रांस में वही दोहराया। कहा कि भारत में लोकतंत्र, संविधान पर हमला हो रहा है, आवाज को दबाया जाता है, मुसलमानों दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, केरोसिन छिड़क दिया गया है...आदि।
इतना ही नहीं राहुल ने मणिपुर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी विचार व्यक्त किए। उसका भी लब्बोलुआब वही जो वह लोकसभा में बोल चुके थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे रहे थे तो राहुल अपने समर्थकों के साथ बहिर्गमन कर गए थे, क्योंकि मोदी उनको आईना दिखा रहे थे। वस्तुतः राहुल गांधी भारत और नरेन्द्र मोदी के विरोध का अन्तर समझने में असमर्थ हैं। इसलिए विदेशों में उनके बयान भारत की छवि के प्रतिकूल हो जाते हैं। एक तरफ राहुल अपने उसी अंदाज में बयान दे रहे थे, दूसरी तरह जी-20 सम्मेलन में भारत की जय-जयकार हो रही थी। सभी विदेशी नेता मोदी के मुरीद बन गए थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब आपदा में अवसर का विचार दिया, तब आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ हो गया। भारत ने कोरोना की दो वैक्सीन सबसे पहले बना कर विकसित देशों को भी चौंका दिया। पहले विकसित देश वैक्सीन बनाते थे। दशको बाद वह भारत को नसीब होती थी। भारत का पिछला चन्द्रयान अभियान विफल हुआ था। नरेन्द्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे। उन्होंने विफलता में अवसर का विचार दिया। वैज्ञानिकों ने कमियों को दूर किया। इसके बाद चन्द्रयान अभियान सफल हुआ। इसी प्रकार नरेन्द्र मोदी ने जी-20 की अध्यक्षता को अवसर में बदल दिया। भारतीय विचार और संस्कार की दुनिया में गूंज हुई। वसुधैव कुटुम्बकम जी-20 का ध्येय वाक्य बन गया। ब्राजील को अध्यक्षता की कमान सौंपी गई।
नरेन्द्र मोदी ने घोषणा पत्र से लेकर जितने भी प्रस्ताव किए, उन सभी को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह अध्यक्षता में अवसर का बेमिसाल प्रमाण है। राहुल गांधी ने पेरिस में छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, कई उपनिषद पढ़े हैं, मैंने कई हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं, भाजपा जो करती है उसमें हिंदू धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। विपक्षी दलों का गठबंधन भारत के लोकतांत्रिक ढांचों को बचाने के लिए लड़ रहा है। विपक्ष भारत की आत्मा के लिए लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। देश मौजूदा उथल-पुथल से सकुशल बाहर आ जाएगा। निचली जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों की अभिव्यक्ति और भागीदारी को रोका जा है। प्रधानमंत्री यह फैसला कर लें कि भारत में कोई अहंकारपूर्ण आचरण या कोई हिंसा नहीं करेगा, तो यह रुक जाएगा। राहुल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक भी की।
दूसरी ओर जी-20 के सभी देश नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने के समझौते कर रहे हैं। जब राहुल गांधी फ्रांस में भारत की छवि के प्रतिकूल बयान दे रहे थे, उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और भारत की प्रगति की प्रशंसा कर रहे थे। जी-20 समिट से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मैक्रों ने बताया कि फ्रांस भारत के साथ रक्षा सहयोग को और विकसित करेगा। भारत ने विभाजित माहौल के बाद भी जी-20 केअध्यक्ष के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए वसुधैव कुटुम्बकम् लिखा। कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन ने एकता का संदेश दिया। दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्म के डिजाइन, विकास और निर्माण में साझेदारी के जरिये भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने रक्षा संबंधी औद्योगिक रूपरेखा को शीघ्र अंतिम रूप देने का भी आह्वान किया। डिजिटल, विज्ञान, तकनीकी नवाचार, शिक्षा,संस्कृति,स्वास्थ्य और पर्यावरण सहयोग बढ़ाया जाएगा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए इंडो-फ्रेंच कैंपस के मॉडल पर इन क्षेत्रों में संस्थागत संबंधों को मजबूत किया जाएगा।
नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक आर्थिक गलियारा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह गलियारा एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक विकास और डिजिटल सम्पर्क सुविधा प्रदान करने में भी मदद करेगा। नरेन्द्र मोदी और क्राउन प्रिंस ने भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। भारत, सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। जबकि सऊदी अरब, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।