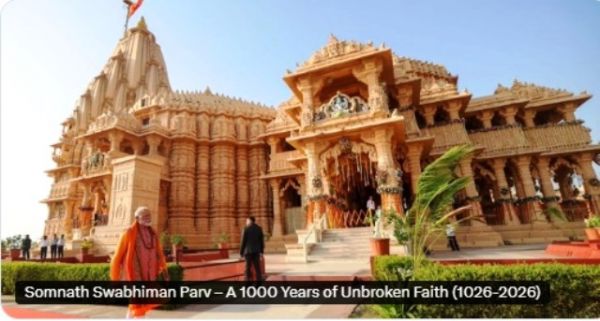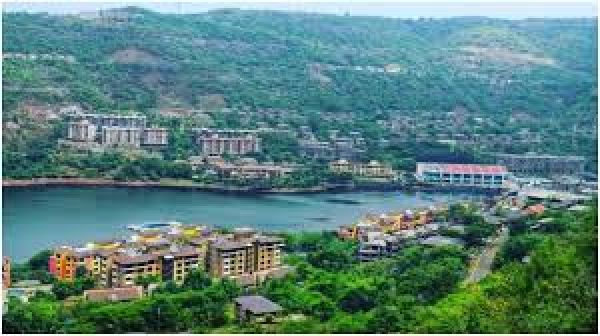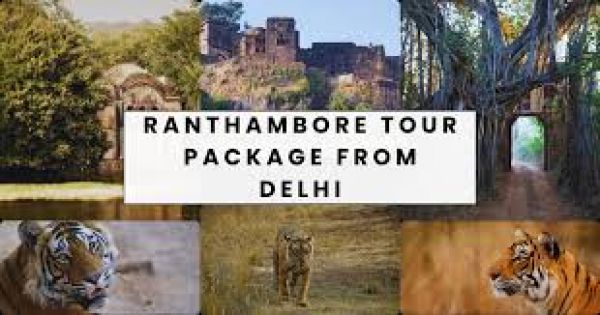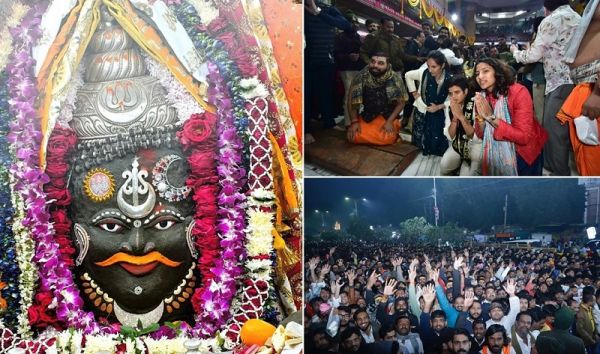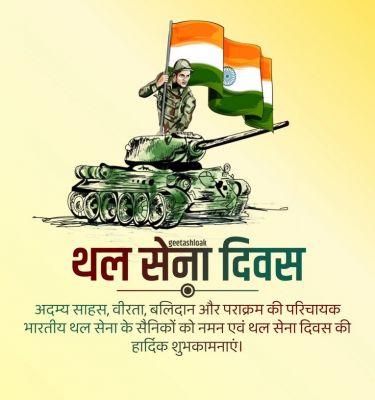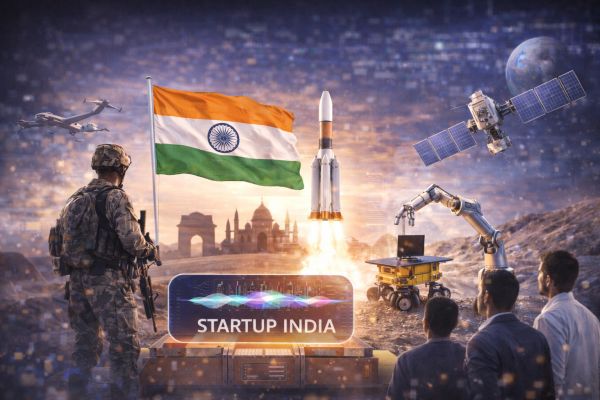Travel & Culture
RELATED POST
Leave a reply
Advertisement
-

मुख्य समाचार:: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे; साथ ही तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। भारत और जापान ने एआई संवाद शुरू किया और महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया; विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच साझेदारी में वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने की अपार क्षमता है। ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चांसलर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पत्र दायर किया; समूह से जुड़ी 140 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। क्रिकेट की बात करें तो, भारत आज दोपहर जिम्बाब्वे के बुलावेयो में पुरुषों के अंडर-19 वनडे विश्व कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा।