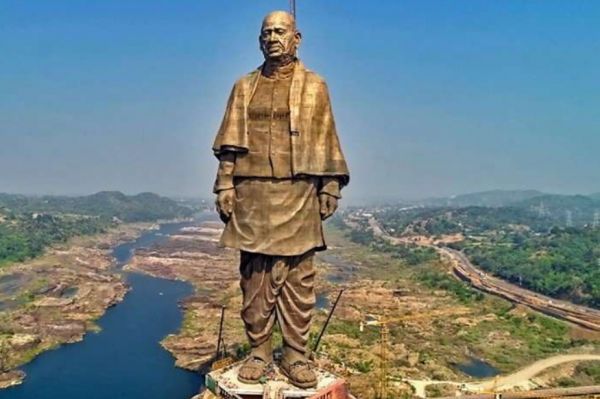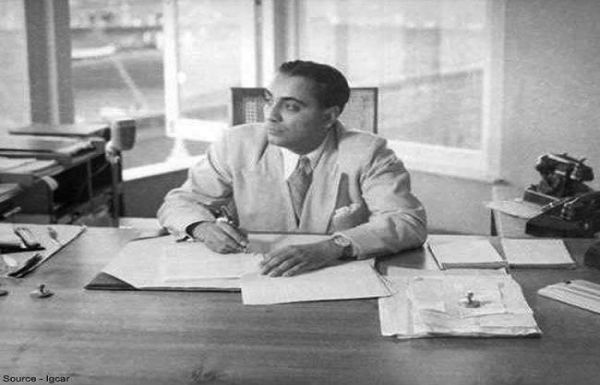हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन संतुलन को बनाए रखने के लिए बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता बहुत आवश्यक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आधारशिला है। दुनिया भर में रहने वाले लगभग आठ अरब लोग लगातार धरती की धरोहर का उपभोग कर रहे हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तब हमारा इशारा, धरती पर मौजूद तमाम जीवों और जैवप्रणालियों की जीवविज्ञानी (बायोलॉजिकल) और आनुवंशिक (जेनेटिक) विविधता से होता है। जैव विविधता के अन्तर्गत जीवित जीवधारियों पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों के अलावा फफूंद और मिट्टी में मिलने वाले सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया भी शामिल हैं। वे पूरी दुनिया की उन तमाम व्यापक इको प्रणालियों का हिस्सा हैं जो बर्फीले अंटार्कटिक, ट्रॉपिकल वर्षावनों, सहारा रेगिस्तान, मैंग्रोव वेटलैंड, मध्य यूरोप के पुराने बीच वनों और समुद्री और तटीय इलाकों की विविधता से भरा है।
ये बायोडायवर्सिटी जीने लायक चीजें मुहैया कराती हैं जैसे कि पानी, भोजन, साफ हवा और दवा, सामूहिक रूप से इन्हें इको सिस्टम सेवाएं कहा जाता है। और वे प्रजातियों की विविधता की पारस्परिकता पर भी निर्भर होती हैं। अगर कोई एक प्रजाति खत्म हो जाती है तो प्रकृति-प्रदत्त ये सेवाएं भी हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। दुनिया में कुल कितनी प्रजातियां हैं, इस पर बहुत सारे विरोधाभास हैं , लेकिन द इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी ऐंड इको सिस्टम सर्विसेज- आईपीबीईएस के अनुसार इनकी संख्या 30 लाख से 10 करोड़ के बीच है। विश्व में 14,35,662 प्रजातियों की पहचान की गई है। यद्यपि बहुत सी प्रजातियों की पहचान अभी भी होना बाकी है।
पहचानी गई मुख्य प्रजातियों में 7,51,000 प्रजातियां कीटों की, 2,48,000 पौधों की, 2,81,000 जन्तुओं की, 68,000 कवकों की, 26,000 शैवालों की, 4,800 जीवाणुओं की तथा 1,000 विषाणुओं की हैं। पारितंत्रों के क्षय के कारण लगभग 27,000 प्रजातियां प्रतिवर्ष विलुप्त हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर ऊष्ण कटिबंधीय छोटे जीव हैं। हर 10 मिनट में औसतन एक प्रजाति खत्म हो रही है। जब कोई प्रजाति इको सिस्टम से गायब हो जाती है तो प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे बिखरने लगता है।
शोधकर्ताओं के मुताबिक, हम लोग दुनिया की छठी सामूहिक विलुप्ति के बीचो-बीच पहुंच गए हैं। अगर जैव विविधता क्षरण की वर्तमान दर कायम रही तो विश्व की एक चौथाई प्रजातियों का अस्तित्व सन 2050 तक समाप्त हो जाएगा। जैव विविधता खत्म होने से एल्गी यानी शैवालों ( काई) या पेड़ों के बिना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और पौधों को परागित करने वाले परागणकर्ता (पोलिनेटर) जैसे पक्षी, मधुमक्खी और अन्य कीड़े के बिना हमारी फसलें चौपट हो जाएंगी। दो तिहाई से ज्यादा फसलें- जिनमें कई फल, सब्जियां, कॉफी और कोकोआ शामिल हैं, कीटपतंगों जैसे कुदरती पॉलिनेटरों पर निर्भर हैं। सुबह-सुबह जब अन्न का कटोरा हमारे सामने होता है तब हम ये नहीं सोचते कि कुदरत ने इन फसलों को पॉलिनेट करने में कितनी मदद की है जिसकी बदौलत वो अन्न तैयार हुआ है। रोजमर्रा के स्तर पर कुदरत जो हमारे लिए कर रही है, वो हमें दिखता ही नहीं है।
कोविड-19 जैसी महामारी के पीछे की वजह भी कहीं न कहीं से प्राकृतिक असंतुलन है। जब से हमने जैव विविधता को नष्ट करना शुरू किया तभी से हमने उस तंत्र को समाप्त करना शुरू कर दिया, जो स्वास्थ्य तंत्र के लिए मददगार होता है। आज अगर हम देखें तो इसी कोरोना वायरस की भिन्न-भिन्न किस्मों से हर साल करीब 100 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और लाखों लोगों की मौत हो जाती है। यही नहीं धरती पर इंसानों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से 75 फीसदी जूनोटिक होती है। जूनोटिक यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में आती है। साधारण शब्दों में ऐसी बीमारियां जो जानवरों में पैदा होती है और उनसे हम इंसानों के अंदर आ जाती है। दुनिया भर में फैली ये बीमारियां जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवियों से होती है। वह हल्की से बहुत घातक तक हो सकती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इंसानों में होने वाली 60 फीसद से अधिक बीमारियां जानवरों से इंसानों में पहुंचती है। दरअसल, हमने जिस तरह धरती पर से तमाम तरह के जीवों को नष्ट करके उनकी जगह खुद ले ली या उन जीवों को दे दी जिन्हें हम चाहते थे। इस वजह से धरती पर जैव की विविधता खत्म होती गई और जो जानवर इन वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे बीमारी पैदा करने वाले जीवों को संभाल सकते थे, वे धरती पर नहीं रहे। इस तरह दूसरे होस्ट के तौर पर सूक्ष्म जीवों को अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए जो जीवन चाहिए था, वह उन्हें हमसे मिलने लगा और उन्होंने हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार सन 1997 में रेबीज से पूरी दुनिया के 50 हजार लोग मर गए।
भारत में सबसे ज्यादा 30 हजार मरे। आखिर क्यों मरे रेबीज से, एक प्रश्न उठा। स्टेनफोर्ट विश्व विद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि ऐसा गिद्धों की संख्या में अचानक कमी के कारण हुआ। वहीं दूसरी तरफ चूहों और कुत्तों की संख्या में एकाएक वृद्धि हुई। अध्ययन में बताया गया कि पक्षियों के खत्म होने से मृत पशुओं की सफाई, बीजों का प्रकीर्णन और परागण भी काफी हद तक प्रभावित हुआ। अमेरिका जैसा देश अपने यहां के चमगादड़ों को संरक्षित करने में जुटा पड़ा है। अब हम सोचते हैं कि चमगादड़ तो पूरी तरह बेकार हैं। मगर वैज्ञानिक जागरूक करा रहे हैं। चमगादड़ मच्छरों का लार्वा खाता है। यह रात्रिचर परागण करने वाला प्रमुख पक्षी है। लोग कहते हैं कि उल्लू से क्या फायदा, मगर किसान जानते हैं कि वह खेती का मित्र है, जिसका मुख्य भोजन चूहा है।
विकास की दुहाई देकर जैव विविधिता का जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है उसका दूरगामी दुष्परिणाम भी विकास पर ही देखने को मिलेगा। आज आवश्यकता यह है कि विकास के लिए जैव विविधिता के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाए। विकास के नाम पर हम जंगल के जंगल साफ किये जा रहे प्रकृति की इस अकूत दौलत के आधार यानी पेड़ पर जब आरे चलते हैं तो सिर्फ पेड़ ही नहीं कटता बल्कि तमाम जीव जंतुओं के जीवन चक्र पर कुठाराघात होता है। बारिश-धूप-बारिश का चक्र टूटता है। पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की वजह से दुनिया के बहुत सारे इलाके सूखे के हालात झेल रहे हैं। शिवजी की तरह अपनी जटाओं में कार्बन डाई ऑक्साइड को उलझाए जंगल कटेंगे तो ये कार्बन कहां जाएगा? इंसानों ने जिस तरह जंगल, जमीन, जानवर, जल और दूसरे जीवन को नष्ट किया है। इसी का नतीजा है कि आज हम इस हाल में आकर खड़े हो गए हैं। हमने जो उपभोग की इंतेहा की है उसकी वजह से आज हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1.66 धरती की जरूरत है। अब यह सोचने की जरूरत है कुल मिलाकर हमारा जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सेहत सब कुछ जैव विविधता पर निर्भर है। हमें यह समझना होगा कि हम मनुष्यों का अस्तित्व प्रकृति से है न कि प्रकृति का अस्तित्व मनुष्य से है। लिहाजा जैव विविधता का संरक्षण समस्त मानव जाति का साझा उत्तरदायित्व है।
(लेखक, डॉ. सुशील द्विवेदी)







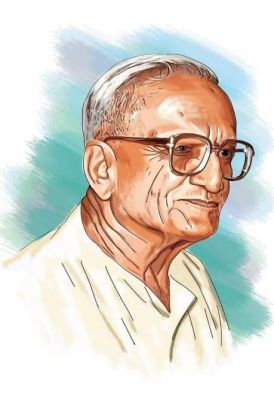





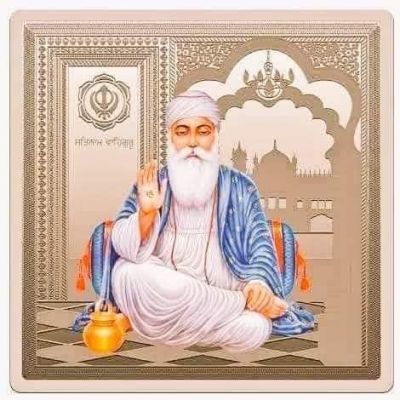
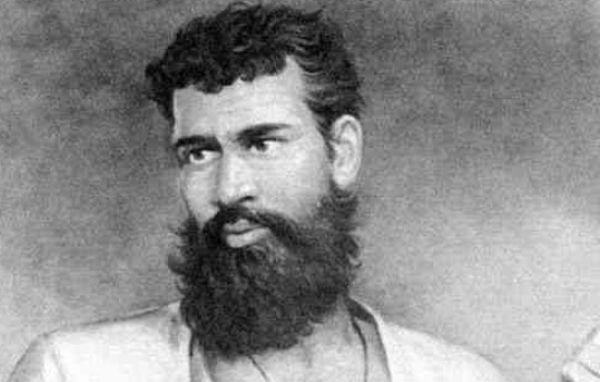
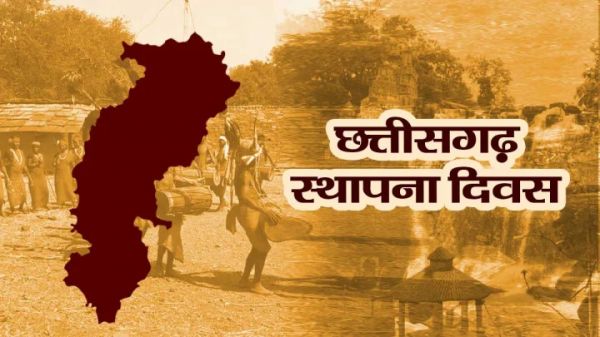





.jpg)

.jpg)