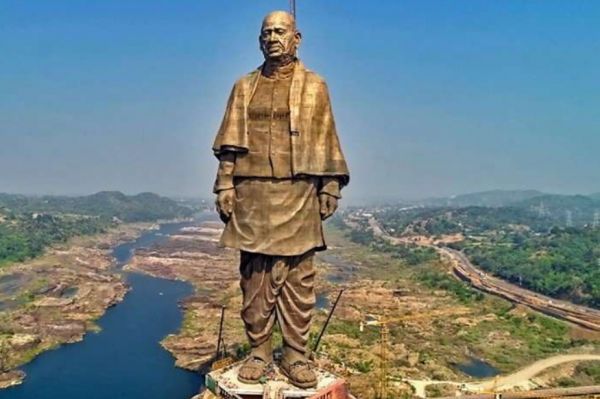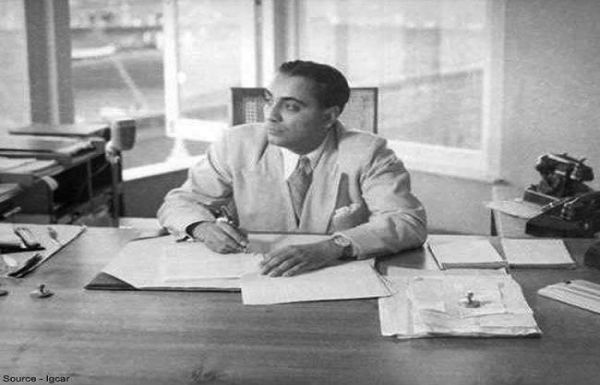पढ़ने-लिखने की उम्र में श्रम के तंदूर में झुलसता बचपन किसी के लिए भी त्रासद हो सकता है। आखिर कौन माता-पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा भी पढ़-लिखकर सुसभ्य नागरिक और देश का निर्माता बने। यह तब है जब भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियां प्रभावी हैं। भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है-14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा (धारा 24)। राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें (धारा 39-ई)। बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन और जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा (धारा 39-एफ)। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)। बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती हैं।
इस संबंध में संघीय सरकार ने कानून भी बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं-बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन धंधों और प्रक्रिया का उल्लेख कानून की अनुसूची में है। दूसरा है-फैक्टरी कानून 1948। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गई है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आया, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह हुक्म भी दिया था कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाए। इसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो। बाल श्रम ऐसा दुश्चक्र है, जो बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता। साल 2011 की जनगणना के के अनुसार, भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है। इसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। दुनिया भर में 6.4 करोड़ लड़कियां और 8.8 करोड़ लड़के बाल मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है। अगर इस अनुमान पर भरोसा किया जाए तो विश्व में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है।
हालांकि कुछ वर्षों से बाल श्रमिक दर में कुछ कमी आई है। बावजूद इसके बच्चों को कुछ कठिन कार्यों में अभी भी लगाया जा रहा है। मसलन बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक (चाइल्ड सोल्जर) और देह व्यापार। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है। देश में बाल मजदूरी और शोषण के कई कारण हैं। इनमें गरीबी, सामाजिक मानदंड, वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी, प्रवास आदि हैं। ये सब वजह सिर्फ कारण नहीं बल्कि भेदभाव से पैदा होने वाली सामाजिक असमानता का परिणाम हैं। अब तो यह साबित हो चुका है कि बाल मजदूरी शिक्षा में बहुत बड़ी रुकावट है। इससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन पर खराब प्रभाव पड़ता है।
बाल तस्करी तो बाल मजदूरी से भी बड़ा अभिशाप है। बाल मजदूरी और शोषण को एकीकृत दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रयासों से रोका जा सकता है। इसमें स्वैच्छिक संगठनों और शिक्षकों का अहम योगदान हो सकता है। यूनीसेफ, सरकार और निजी एंजेसियों के साथ मिलकर इस संबंध में जरूरी नीतियां तैयार करता है। वक्त आ गया है कि हमें बाल मजदूरी की सांस्कृतिक स्वीकृति को खारिज करने की जरूरत है। बाल अधिकारों पर वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श विभिन्न स्तर पर जारी रहता है। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में तो कई बार चर्चा हो चुकी है। देश के स्कूली बच्चों को श्रम के भंवरजाल से बाहर निकालने का संकल्प हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और एजुकेशन इंटरनेशनल ने लिया है। इस अंतरराष्ट्रीय पहल पर दुनिया भर के शिक्षाविदों ने चर्चा की है। एजुकेशन इंटरनेशनल की अध्यक्ष मिसेज सुजन हॉपगूड ने कहा, दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। इनमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा चिंताजनक है। इसे समाप्त करना महत्वपूर्ण चुनौती है। शिक्षक संगठनों और सरकार के प्रयासों के बावजूद ऐसी स्थिति गंभीर इशारा कर रही है। उल्लेखनीय है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो चुका है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। हॉपगूड ने हैरानी जताई कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भगीरथ प्रयास नहीं हो रहे।(लेखक,सुशील पाण्डेय)







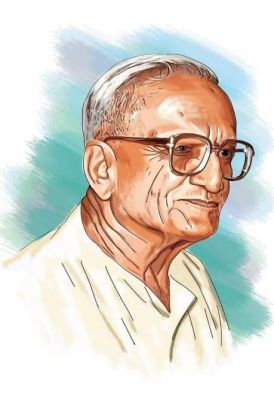





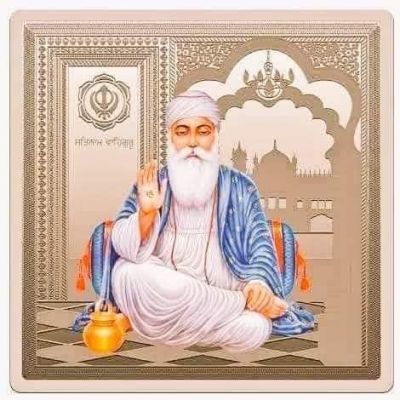
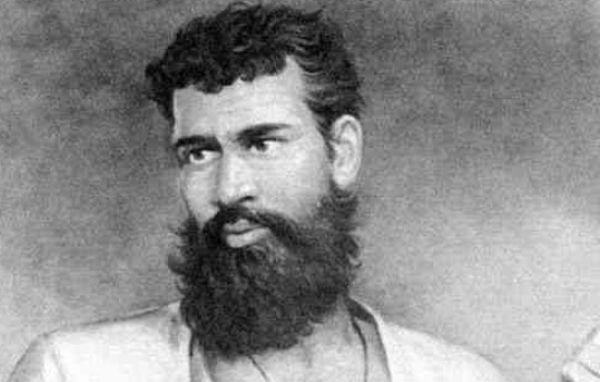
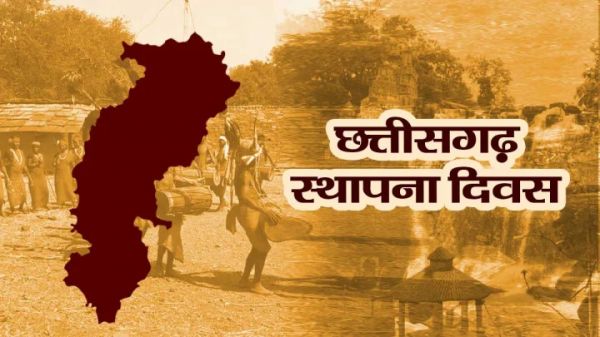





.jpg)

.jpg)