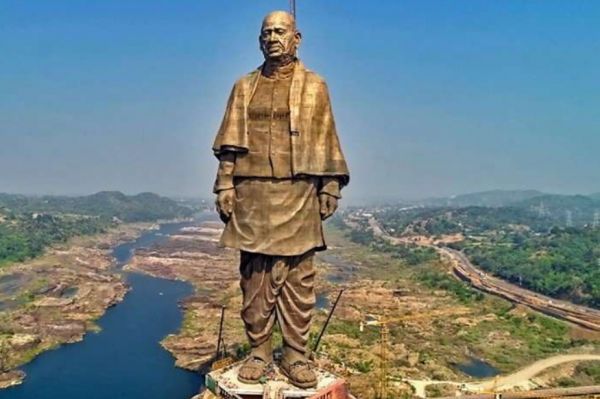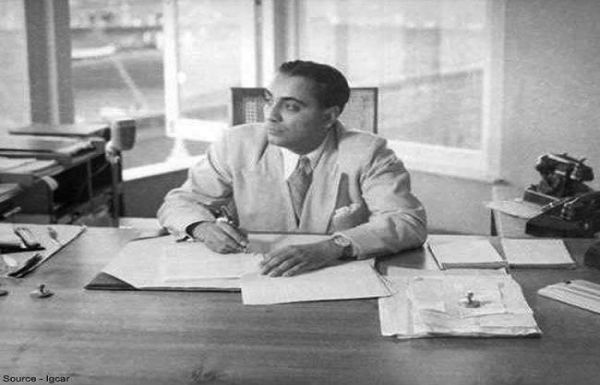मानव सभ्यता के संदर्भ में अध्यापन-कार्य न केवल दूसरे व्यवसायों की तुलना में सदैव विशेष महत्व का रहा है बल्कि अन्य सभी व्यवसायों का आधार भी है । आज सामाजिक परिवर्तन विशेषतः प्रौदयोगिकी की तीव्र उपस्थिति ने शिक्षक और शिक्षार्थी के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। साथ ही कक्षा, समाज और व्यापक विश्व के संदर्भ में शिक्षक की संस्था भी नए ढंग से जानी पहचानी जा रही है। इसके फलस्वरूप शिक्षक की औपचारिक भूमिका और व्याप्ति का क्षेत्र जरूर अतीत की तुलना में वर्तमान काल में नए नए आयाम प्राप्त कर रहा है। इन सबके बीच अभी भी अध्यापक अपने गुणों, कार्यों और व्यवहारों से छात्रों को प्रभावित कर रहा है और उसी के आधार पर भविष्य के समाज और देश के भाग्य को भी अनिवार्य रूप से रच रहा है। एक अध्यापक को समाज ने अधिकार दिया है कि वह अपने छात्र के जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करे, विद्यार्थियों को भविष्य के सपने दिखाए और उनमें निहित क्षमता को समृद्ध कर उन सपनों को साकार करने के लिए तैयार करे । ऐसा करते हुए मूल्यों और मनोवृत्तियों को भी गढ़ता है। वशिष्ठ, बुद्ध, चाणक्य, टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राधाकृष्णन आदि के स्मरण से मन में गुरु की आदर्श और तेजस्वी छवि बनती है।
शिक्षा के परिसर में अध्यापक के व्यवहार के जो नैतिक और आचारगत परिणाम होते हैं वे समाज की नैतिक परिपक्वता और विवेक को निश्चित करते हैं । इसीलिए अध्यापक को जांचने-परखने के लिए ऊंचे निकष और मानक तय किए जाते हैं जिन्हें दूसरे व्यवसाय के लोग आसानी से नहीं स्वीकारते। अध्यापकों से नैतिक गुणों की अपेक्षा होती है। उनसे आशा की जाती है कि वे अपने आचरण में उचित और अनुचित का विवेक करेंगे। योग्यता, कुशलता और गुणवत्ता उनके व्यवहारों से झलकेगी। वे प्रतिबद्धता, काम के प्रति समर्पण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पूर्वाग्रहमुक्त आचरण की मिसाल प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक की गुणवत्ता विद्यार्थी की सफलता का सबसे प्रमुख आधार होता है ऐसा सोच कर अभिभावक अपने मन में अध्यापक और गुरु के प्रति सहज सम्मान का भाव रखता रहा है । एक गुरु मानसिक और व्यावहारिक रूप से दूसरों की भलाई करने वाले और भविष्य का नज़रिया रखने वाले इंसान के रूप में प्रतिष्ठित था। वह माता-पिता से कम महत्व का न था। वह विद्यार्थी का प्रेरणास्रोत और ऐसा हितैषी था जो उसे सत्पथ पर जाने की राह दिखाता था। चरित्र-निर्माण करते हुए एक अच्छा मनुष्य और देश का अच्छा नागरिक बनाना उसका कर्तव्य था। समाज में गुरु की ऊंची साख इसलिए भी थी कि वह निर्भय हो कर बिना किसी लाग-लपेट के लोक-हित की बात कह सकता था । अब यह छवि बदल रही है और धीरे-धीरे खिसक कर हाशिए पर पहुंच रही है और थोड़े अध्यापक ही अपनी मूल छवि की रक्षा कर पा रहे हैं। ज्यादातर की दिशा बदल चुकी है या फिर बदलने की फिराक में हैं।
अध्यापक का कार्य अब पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है यानी एक ज्ञान का व्यापार करने वाला एक शुद्ध आर्थिक कार्य हो रहा है। इक्कीसवीं सदी में पहुंच कर न केवल ज्ञान की विषय वस्तु में बदलाव आया है बल्कि पठन-पाठन के तौर-; तरीक़े भी बदले हैं। साथ ही संदर्भ भी तीव्र गति से लगातार बदल रहा है। समाज, आर्थिक कारोबार, संचार, प्रशासन, मूल्य, मानक, भूमिकाएं सभी नए ढांचे में ढल रहे हैं। समय के साथ शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत हुआ है, अनेक नए विषय शुरू किए गए हैं। उसी के साथ नैतिक निर्णयों के क्षेत्र भी विस्तृत हुए हैं। व्यवसाय और शिक्षण-प्रक्रिया के नैतिक मानकों की उलझनें भी बढ़ी हैं। सैद्धांतिक रूप में मानव मूल्य और मानवीय गरिमा वे केंद्रीय सरोकार हैं जिनकी संपोषण शिक्षक-प्रशिक्षण का अहं हिस्सा होता है तथापि आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का रिश्ता अलगाव और नासमझी का शिकार हो रहा है। आज अनुदानप्राप्त शिक्षा केंद्रों में वेतन तो बढ़ा है परंतु आम तौर पर शिक्षण कार्य के साथ लगाव और रुचि में कमी आई है। तल्लीन हो कर कार्य करना और उसे गंभीरता से लेना अध्यापकों की वरीयता में नीचे खिसक रहा है। यही नहीं यदि शिक्षा संस्थाओं में उठने वाले मामलों को देखा जाए तो अपने सहकर्मियों के साथ स्वस्थ और मानवीय रिश्ता और उनके अधिकारों का आदर, सामुदायिक भावना और भागीदारी, सामाजिक मूल्यों तथा मानकों तथा न्याय की रक्षा, आचरण की पवित्रता और सदाशयता, पक्षपातविहीन रहना, समानुभूति, और निष्ठा आदि के विषय में गिरावट उनके मुख्य कारण हैं। शिक्षक की नैतिक क्षमता और नैतिक योग्यता अब दुर्लभ हो रही है। अध्यापकों का विद्यार्थियों के साथ बर्ताव को लेकर ग़लत आचरण की शंका बढ़ रही है और भरोसा कम हो रहा है। आए दिन ऐसी घटनाओं की खबरें आती रहती हैं जिनमें आदर न देना, अनावश्यक आक्रोश, गप मारना, तटस्थ बने रहना, अपेक्षित सहायता न करना, क़ायदे-क़ानून की आड़ में अकर्मण्य बने रहना, सुविधाभोगी होना, नकारात्मक रिश्ता रखना, खराब आचरण, अपर्याप्त जानकारी, अनुशासन की कमी, अनैतिक भावनाएं, अपर्याप्त तैयारी और आत्म-नियंत्रण की कमी प्रमुख होती हैं।
यह खेदजनक है कि विगत वर्षों में अनेक संस्थानों में छात्रों को प्रताड़ित करने के मामलों में वृद्धि हुई है। उनके संज्ञानात्मक और भावात्मक कल्याण को ले कर अकादमिक प्रशासन और नेतृत्व की संवेदनहीनता के सवाल बार-बार खड़े हुए हैं। उनके हितों की उपेक्षा करने और शिक्षण के प्रसंग में अनैतिक कार्यों के दायरे में डरावने अभ्यास, निर्णय लेने के गैरकानूनी तरीके, स्वीकृत नीतियों का उल्लंघन, विद्यार्थियों को उपलब्ध विकल्पों की अस्वीकृति और उपेक्षा, सार्वजनिक रूप से अवमानना और उपहास आदि के दुष्परिणाम शिक्षा के परिसरों में हिंसा, दुराचार, आत्म-हत्या, दुर्व्यवहार आदि के रूप में प्रकट हुए हैं। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्या की अनदेखी होती रही है। यू जी सी ने अब संज्ञान लिया है और इस हेतु नीति भी तैयार की है। नैतिक बोध और आचारपरक सोच को पारस्परिक विश्वास और समानुभूति के आधार पर अमली जामा देना बहुत आवश्यक हो गया है। इंटरनेट के चलते सोशल मीडिया की अनियंत्रित दखल ने स्वस्थ और सुरक्षित शैक्षिक परिवेश की राह में आज बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नैतिकता और शिक्षा प्रक्रिया (पेडागोजी) के बीच के सम्बन्ध को न्याय और ईमानदारी की भावना से दायित्व के साथ स्थापित करना आवश्यक हो गया है।
सामाजिक मूल्यों और मानकों का पालन, गुणवत्तापूर्ण सीखने-सिखाने की प्रक्रिया छात्रों की आवश्यकताओं को जान कर ईमानदार और न्यायपूर्ण समाधान आज की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। मानवीय गरिमा का आदर स्थापित हो इसके लिए प्रभावी संचार, सामूहिक दायित्व का निर्वाह और निजता की रक्षा जरूरी होगी। आज के संदर्भ में अध्यापन, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति आदि शिक्षा के विभिन्न पक्षों में प्रौदयोगिकी का समुचित उपयोग करने की प्रभावी नीति तात्कालिक आश्वश्यकता है। प्राथमिक स्तर से ले कर उच्च शिक्षा तक का शिक्षा-संदर्भ निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं की श्रेणियों में बँटा हुआ है और इनमें भी भयानक स्तर भेद हैं। इनके कायदे-कानून, अध्यापकों को मिलने वाले अवसर, कार्यभार और वेतन आदि में बड़े भेद और विसंगतियां बनी हुई हैं । केंद्रीय महत्व का होने पर भी बहुत कम संस्थाओं में अध्यापक का स्वायत्त अस्तित्व होता है अन्यथा वह राजनीति, शासन, प्रशासन पर आश्रित रहता है। आज अधिकांश शिक्षा संस्थाएं तदर्थ (एडहाक) अध्यापकों के भरोसे चल रही हैं और खोखली हो रही हैं। शिक्षा नीति–2020 के महत्वाकांक्षी स्वप्न को आकार देने के लिए अध्यापकों की स्थायी व्यवस्था जरूरी होगी। पूरी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह व्यवसायीकरण की चपेट में है उसका हिंसक परिणाम कोचिंग नगरी कोटा की कथा से उजागर होता है जहां विद्यार्थियों में आत्म हत्या की प्रवृत्ति फैल रही है या फिर अव्यवस्थित कोचिंग संस्थानों में लगी आग में विद्यार्थी झुलसते-मरते हैं। वस्तुतः शिक्षा अभी तक हमारी राष्ट्रीय विकास योजना के एजेंडा में बहुत नीचे पड़ी हुई है। शिक्षा को भगवान भरोसे छोड़ बाक़ी चीजों में निवेश हो रहा है। इस उदासीनता के दुष्परिणाम भी दिख रहे हैं पर राजनीति की समाधि नहीं टूट रही है। सा विद्या या विमुक्तये कहते हुए भी शिक्षा कारोबार होती जा रही है। बाजार और व्यवसाय के ताने बाने में शिक्षक इस कारोबार का एक अदना किरदार हो गया है। शिक्षक की गरिमा स्थापित कर के ही अमृत काल के संकल्प चरितार्थ हो सकेंगे।(लेखक, गिरीश्वर मिश्र)







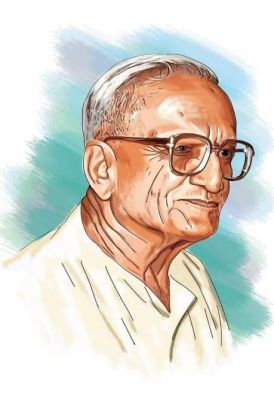





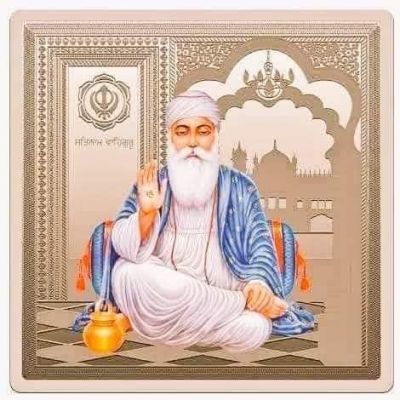
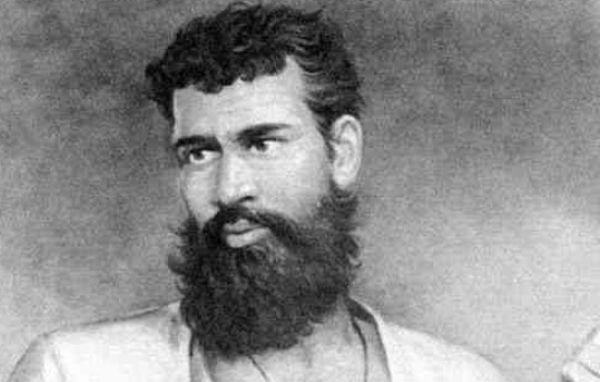
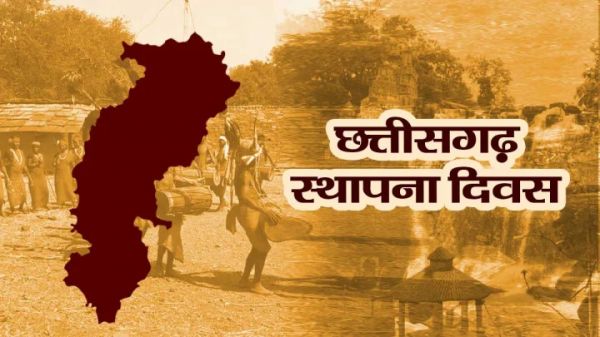





.jpg)

.jpg)