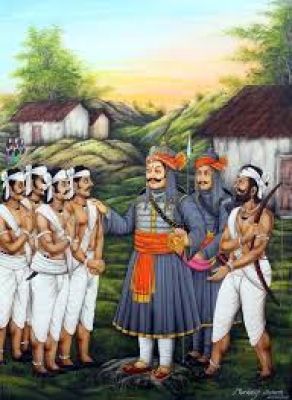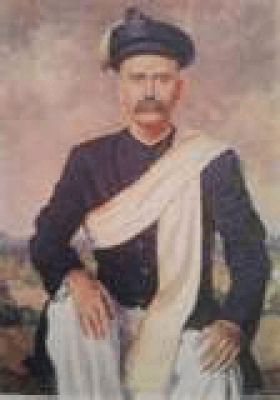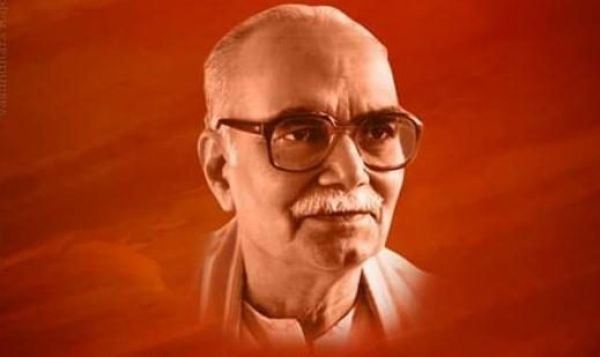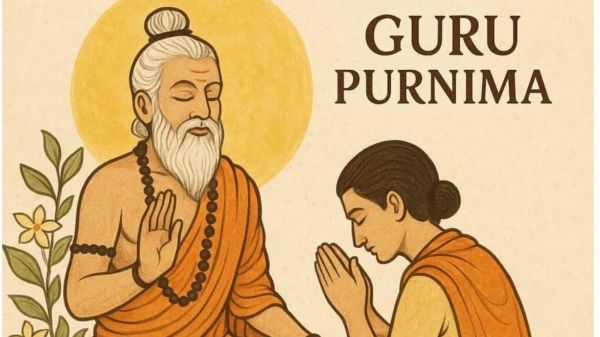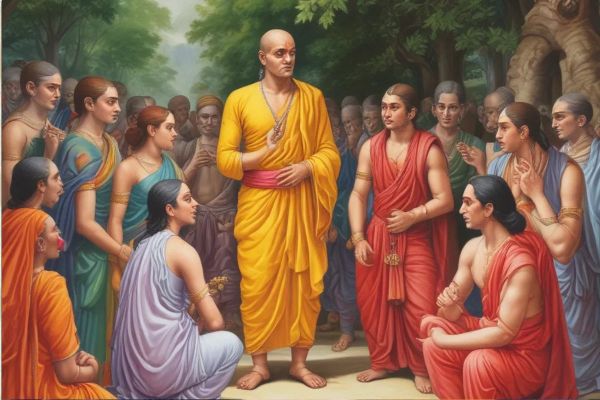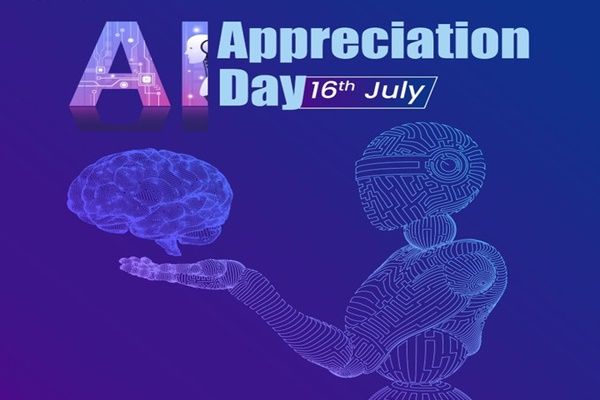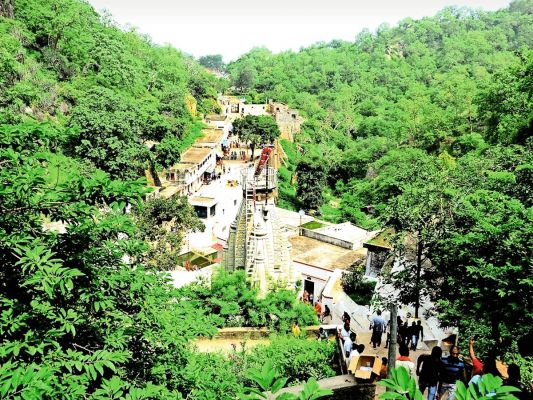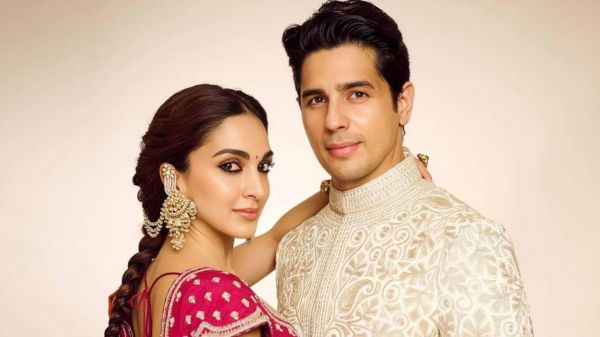लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी मनुस्मृति लेकर सदन में गए। मनुस्मृति के हवाले से तमाम छोटी बातें की। वे इतिहास बोध से नहीं जुड़ते। आखिरकार इन मनु का परिचय क्या है? ऋग्वेद वाले मनु या शतपथ ब्राह्मण वाले मनु? हम मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ है मनु के या मनु का। मानव का अर्थ भी यही है-मनोः अपत्याम मानवः। संस्कृत विद्वान डॉ. सूर्यकान्त बाली ने ऐसे तमाम उद्धरण देकर मनुज को मनु की सन्तान बताया है। मनुज, मनुष्य या मानव मनु के विस्तार हैं। कालगणना की बड़ी इकाई है मन्वन्तर। इसके पहले छोटी इकाई है युग। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चार युगों को जोड़कर महायुग बनता है। 31 महायुग का जोड़ मन्वन्तर है। हरेक मन्वन्तर में एक मनु हैं। मन्वन्तर दो मनुओं के बीच का अन्तर काल है। अब तक अनेक मनु हो चुके हैं। एक मनु ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद के ऋषि ने मनु को पिता कहा है। हरेक मंगल कार्य में आगे-आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित मनु जलप्रलय में वे मछली की सहायता से अकेले ही बच निकले थे। मनु ने ही सृष्टि बीजों की रक्षा की थी। अथर्ववेद वाले मनु भी ऐसे ही हैं और मत्स्य पुराण वाले मनु भी। जयशंकर प्रसाद की ‘कामायनी‘ में भी इन्हीं मनु का वर्णन है।
भारतीय काव्य, पुराण और वैदिक मन्त्रों में विस्तृत मनु हमारी राष्ट्रीय स्मृति के रहस्यपूर्ण प्रतीक हैं। मनु की स्मृति में लगभग 2000 वर्ष पहले एक ग्रन्य रचा गया मनुस्मृति। मनुस्मृति की भाषा वैदिक संस्कृत छन्दस में नहीं है। मनुस्मृति के श्लोक व्याकरण के अनुशासन में हैं। व्याकरण का अनुशासन पाणिनि ने तय किया। मनुस्मृति की संस्कृत ऋग्वेद-अथर्ववेद के बाद की है। श्लोकों की रचना में भाषा का आधुनिक प्रवाह है। 2000 वर्ष पहले का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। इसके 500 बरस पहले बुद्ध हैं। मनुस्मृति मनु की रचना नहीं है। यह मनु की स्मृति में लिखी गई किसी अन्य विद्वान की कृति है। वैसी ही जैसी गांधीजी की स्मृति में लिखी कोई पुस्तक है। गांधी का लिखा साहित्य उपलब्ध है इसलिए हम गांधीजी की स्मृति में लिखे गए ग्रन्थों व गांधी द्वारा लिखे गए साहित्य में फर्क कर लेते हैं। मनु ने स्वयं कोई पुस्तक लिखी नहीं।
ऋग्वेद में मनु सम्बन्धी विवरण ऋषियों के हैं। शतपथ ब्राह्मण या पुराणों के मनु विषयक उल्लेख अन्य रचनाकारों के हैं। जल प्रलय कवि कल्पना या छोटी घटना नहीं थी। इसका उल्लेख बाईबिल में है, कुरान में भी है। चीन की कथाओं में है। यूनान के भी कथा सूत्रों में है। जल प्रलय में अकेले बचे मनु ने कोई ग्रन्थ लिखा नहीं। वे मनुस्मृति के लेखक नहीं हैं। मनुस्मृति के कतिपय अंश वर्ण विभेदक हैं। इसी आधार पर मनुस्मृति की निन्दा होती है। इसी किताब को लेकर मनु को गालियाँ दी जाती हैं। मनु पर जाति व्यवस्था को जन्म देने के आरोप लगाए जाते हैं। बेचारे मनु इस आरोप का उत्तर या स्पष्टीकरण देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वे तब भी उपलब्ध नहीं थे, जब मनुस्मृति की रचना हुई। इस विषय पर कुछ भी बोलने वाले मनुवादी कहे जाते हैं। मैं प्रतीक्षा में हूँ कि मुझे मनुवादी वगैरह कहा जाय।
मूलभूत प्रश्न है कि क्या कोई भी एक व्यक्ति वृहत्तर भारतीय समाज को जाति-पांति में विभाजित करने की शक्ति से लैस हो सकता है? क्या समाज उसके आदेशानुसार जातियों में बँट जाने को तैयार था? क्या उसके आदेशों के सामने पूरा समाज विवश था? वह मनु हों या कोई भी शक्तिशाली सम्राट? क्या एक व्यक्ति ऐसा कार्य करने में सक्षम हो सकता था? क्या शक्तिसम्पन्न तानाशाह, राजा या बादशाह ऐसी व्यवस्था लागू करने में सक्षम हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर है, नहीं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने जाति के जन्म और विकास पर गहन विवेचन विश्लेषण किया था। उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयार्क में 9 मई 1916 के दिन एक लिखित भाषण दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में ‘डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर लेख व भाषण‘ (खंड 1) प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में न्यूयार्क वाला भाषण संकलित है।
सम्पादक मण्डल ने भूमिका (पृष्ठ 14) में ‘भारत में जातियाँ‘ शीर्षक देकर लिखा है, ”डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को सांस्कृतिक एकता ही एक सूत्र में बाँधती है। जातियों के सम्बन्ध में विद्वानों के मतों का मूल्यांकन करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है कि बहिर्विवाह के ऊपर अन्तर्विवाह का अध्यारोपण ही जाति-समूह बनने का मुख्य कारण है।” डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, ”समाज के छोटे-छोटे भाग बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया या घटना है। इन्हीं छोटे भागों या समुदायों ने बहिष्करण व अनुकरण द्वारा विभिन्न जातियों का रूप ले लिया।” डॉ. अम्बेडकर का यह भाषण पठनीय है। लिखा है, ”मैं सर्वप्रथम भारत के स्मृतिकार के सम्बन्ध में कहूँगा। प्रत्येक देश में आपातकाल में अवतार के रूप में स्मृतिकार उत्पन्न होते हैं ताकि पतित समाज को सही दिशा-बोध कराया जा सके और न्याय तथा नैतिकता का विधान दिया जा सके। स्मृतिकार मनु यदि वास्तव में कोई व्यक्ति थे तो निश्चित ही वह अदम्य साहसी थे। यदि यह कथन सही है कि मनु ने जाति-विधान की रचना की थी तो वह अवश्य ही एक दुस्साहसी व्यक्ति रहे होंगे। जिस समाज ने उनके समाज-विभाजन नियम को स्वीकार किया वह अवश्य ही उससे भिन्न रहा होगा। हम अवगत हैं कि यह सोचा भी नहीं जा सकता कि जाति विधान कोई प्रदत्त वस्तु थी।”
डॉ. अम्बेडकर का कथन महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, “मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाति धर्म का नियम मनु द्वारा प्रदत्त नहीं है।” डॉ. अम्बेडकर ने मनु को जाति विधान का जन्मदाता नहीं माना। भारतीय इतिहास में धर्म कभी भी संगठित सत्ता नहीं रहा। पोप जैसी संस्था यहाँ कभी नहीं रही। हिन्दू धर्म की कोई एक सर्वमान्य पुस्तक नहीं। वैदिक साहित्य काव्य स्तुतियाँ हैं। ऋग्वेद के साढ़े दस हजार मन्त्रों में एक भी मन्त्र में निर्देशात्मक बात नहीं। कवि अपनी बातें मानने पर जोर नहीं देते। वाल्मीकि रचित ‘रामायण‘ अंतरराष्ट्रीय स्तर का महाकाव्य है। भारत में इसे धर्मशास्त्र की तरह नमन किया जाता है। गीता में श्रीकृष्ण वक्ता हैं, वे प्रश्नकर्ता अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। यहाँ भी मानने पर जोर नहीं। गीता के अन्तिम भाग में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, ”गुह्य ज्ञान बताया है, विचार करो, जो उचित हो, वैसा अपनी इच्छानुसार करो-यथेच्छसि कुरू।”
मान लें कि मनुस्मृति के रचनाकार ने अपनी इच्छानुसार पुस्तक लिखी। उसे मानना या न मानना बाध्यकारी नहीं। भारतीय इतिहास की किसी राज्य व्यवस्था ने उसे संविधान का दर्जा नहीं दिया। मनुस्मृति वाली राजव्यवस्था/समाज व्यवस्था इतिहास में नहीं मिलती। याज्ञवल्क्य स्मृति वाली भी नहीं। याज्ञवल्क्य वृहदारण्यक उपनिषद् में दार्शनिक नायक जैसे हैं। उपनिषद् में उनके अनेक वक्तव्य हैं। उपनिषद् विश्वदर्शन का हिरण्यगर्भ है। भारतीय समाज, धर्म और दर्शन सतत् गतिशील रहे हैं। हम हजारों बरस प्राचीन साहित्य से श्रेय और प्रेय ही ग्रहण करते हैं। कालवाह्य को छोड़ने और नूतन को आत्मसात करने की भारतीय शैली जड़ नहीं है। संस्कृति में पुनर्नवा चेतना है। हरेक ऊषा नई। हरेक प्रभात सुप्रभात। सतत् प्रवाही है यहाँ का राष्ट्रजीवन।
लेखक - हृदयनारायण दीक्षित




.jpg)