राम की कथा को नाटक के रूप में मंच पर प्रदर्शित करने वाली रामलीला भी 'हरि अनंत हरि कथा अनंता' की तर्ज़ पर वास्तव में कितनी विविध शैलियों वाली है, इसका खुलासा इन्दुजा अवस्थी ने अपने शोध-प्रबंध 'रामलीला : परंपरा और शैलियाँ' में बड़े विस्तार से किया है। इंदुजा अवस्थी के इस शोध प्रबंध की विशेषता यह है कि यह शोध पुस्तकालयों में बैठकर न लिखा जाकर विषय के अनुरूप (रामलीला) मैदानों में घूम-घूम कर लिखा गया है। रामकथा तो ख्यात कथा है, किंतु जिस प्रकार वह भारत भर की विभिन्न भाषाओं में अभिव्यक्त हुई है तो उस भाषा, उस स्थान और उस समाज की कुछ निजी विशिष्टताएँ भी उसमें अनायास ही समाहित हो गई हैं - रंगनाथ रामायण और कृतिवास या भावार्थ रामायण और असमिया रामायण की मूल कथा एक होते हुए भी अपने-अपने भाषा-भाषी समाज की 'रामकथाएँ' बन गई हैं।
समूचे उत्तर भारत में आज रामलीला का जो स्वरूप विकसित हुआ है उसके जनक गोस्वामी तुलसीदास ही माने जाते हैं, और यह भी सच है कि इन सभी रामलीलाओं में रामचरितमानस का गायन, उसके संवाद और प्रसंगों की एक तरह से प्रमुखता रहती है। बाबू श्यामसुंदर दास हों, कुँवर चंद्रप्रकाश सिंह हों या फिर आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र सभी की यह मान्यता है कि रामलीला के वर्तमान स्वरूप के उद्घाटक, प्रवर्तक और प्रसारक महात्मा तुलसीदास हैं। किंतु यह भी सच नहीं है कि तुलसी के पूर्व रामलीला थी ही नहीं, हाँ यह अवश्य है कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के पश्चात् फिर रामलीलाओं का आधार यही रामचरितमानस ही हो गया। राम की बारात निकलने पर उस प्रान्तर के सभी निवासी मानों राजा जनक के पुरवासी बनकर दूल्हे का सत्कार करते हैं, राम-वनगमन के समय राम-लक्ष्मण और सीता के पीछे अश्रु-विलगित जनता अपने को अयोध्यावासी समझती हुई आँसू बहाती चलती है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चाहे राम-कथा की महती संकल्पना के कारण हो, चाहे रामचरितमानस की लोक प्रतिष्ठा के कारण हो, रामलीला में दर्शकों का जितना संपूर्ण सहयोग होता है उतना और किसी भी नाट्यरूप में मिल पाना कठिन ही है, और यह तथ्य इस लीला नाटक को एक अभूतपूर्व और सशक्त आयाम देता है।






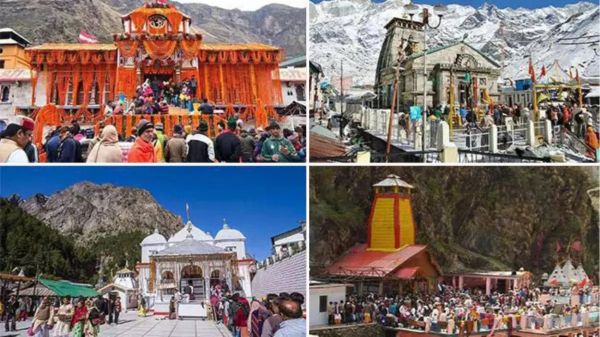










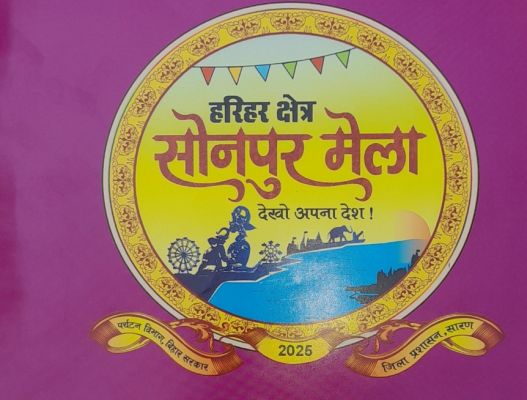















.jpg)

.jpg)









