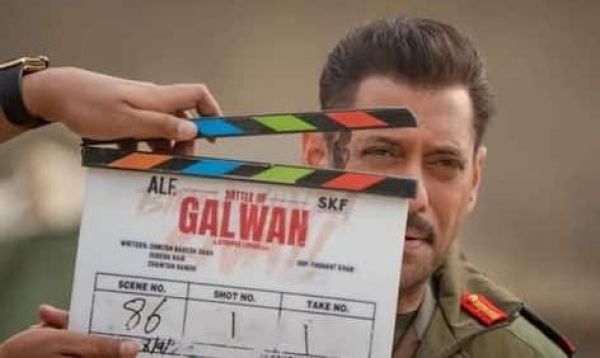लालजी जायसवाल
देश में हर साल बड़ी संख्या में बच्चे लापता होते हैं। उच्चतम न्यायालय में हाल में इस गंभीर मसले पर सुनवाई के दौरा न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक टिप्पणी की, 'मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।' उच्चतम अदालत ने टिप्पणी की कि गोद लेने की प्रक्रिया कठोर होने के कारण, इसका उल्लंघन होना स्वाभाविक है और लोग बच्चे पैदा करने के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा। मालूम हो कि अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से संचालित मिशन वात्सल्य पोर्टल पर प्रकाशन के लिए उनके नाम और संपर्क विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दे।
अदालत ने इससे पहले केंद्र से लापता बच्चों का पता लगाने और ऐसे मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा था। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लापता बच्चों का पता लगाने के काम में लगे पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी को रेखांकित किया था। अदालत ने कहा था कि पोर्टल पर प्रत्येक राज्य से एक समर्पित अधिकारी का नाम- फोन नंबर आदि हो सकता है जो सूचना प्रसारित करने के अलावा गुमशुदगी की शिकायतों का प्रभारी भी हो सकता है। पूर्व में एक एनजीओ ने अदालत का रुख किया था और अपहरण किए जा चुके या लापता बच्चों के अनसुलझे मामलों के अलावा भारत सरकार की तरफ से निगरानी किए जाने वाले खोया/ पाया पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई पर प्रकाश डाला था।
बच्चों का गायब होना सचमुच चिंताजनक है। बच्चों के लापता होने के कई कारण हैं, जिनमें अपराध, तस्करी, हत्या और देह व्यापार आदि की आशंकाएं प्रबल हैं। इसमें प्रशासनिक लापरवाही एक बड़ा कारण हो सकती है, जिसमें सुधार की आवश्यकता हमेशा देखी जाएगी। भारत में गुमशुदा या लापता बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, हर साल मानव तस्करी में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। विधि आयोग द्वारा न्यायिक नीति पर जारी संक्षिप्त पुस्तक में भी इस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इस क्षेत्र में सबसे पहले लापता बच्चों का सुराग लेने और तस्करी से जुड़े सभी संपर्कों के लिए कानूनी बदलाव की तुरंत आवश्यकता है। वर्ष 2013 और 2014 के बीच कम से कम 6,700 बच्चे लापता हुए। इनमें से 45 प्रतिशत बच्चे अवयस्क थे, जिन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया।
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, मानव तस्करी के पीछे अनेक कारण होते हैं। जबरन विवाह, बाल श्रम, घरेलू नौकर और लैंगिक शोषण इसके पीछे मुख्य कारण हैं। बच्चों की सुरक्षा किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। भारत को भी इस मोर्चे पर सुधार की जरूरत है। वर्ष 2024-25 में लगभग 45 हजार बच्चों को शोषण से बचाया गया है। इनमें से 90 प्रतिशत को बालश्रम में लगाया गया था। एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 47 हजार से अधिक बच्चे लापता सूची में हैं। इनमें से 71.4 प्रतिशत नाबालिग लड़कियां हैं। अधिकांश लापता बच्चों को बाल-श्रम, भीख मांगने या यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि खोया-पाया जैसे नागरिक प्लेटफार्म ने कुछ बच्चों को उनके परिवार से जुड़ने में मदद की है। लेकिन असली रोकथाम ऐसे रैकेट और प्रतिष्ठानों में शामिल व्यक्तियों पर तुरंत मुकदमा चलाने से होगा, जहां बच्चों को रखा जाता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मूल कारणों को दूर करना जरूरी है। सामुदायिक सतर्कता नेटवर्क की मदद से भी बच्चों की उठाईगिरी को रोका जा सकता है। लिहाजा बच्चों की सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयास होने चाहिए।
नवजात बच्चों की चोरी और तस्करी से जुड़े मामले में सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि अगर किसी नवजात बच्चे को अस्पताल से चुराया जाता है, तो उस अस्पताल का लाइसेंस रद कर देना चाहिए। नवजात शिशुओं की चोरी किसी भी समाज के लिए केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी आघात है। अस्पतालों में ऐसी घटनाओं का होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा मानकों, कर्मचारियों की नैतिकता और प्रशासनिक निगरानी में गंभीर कमी है। जिन संस्थानों में इस तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं, उनका लाइसेंस तत्काल रद किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो। लाइसेंस रद करने की नीति न सिर्फ अस्पताल प्रबंधन को जवाबदेह बनाएगी, बल्कि निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को भी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बाध्य करेगी। नवजात की सुरक्षा किसी सुविधा का विषय नहीं, बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में जरा-सी भी चूक के लिए ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति ही समाज और न्याय दोनों के हित में है। लापता बच्चा केवल एक मामला नहीं- वह राज्य की जिम्मेदारी, समाज की सतर्कता और प्रशासन की जवाबदेही का पैमाना है। वर्तमान समय में आवश्यक है कि तकनीकी संसाधनों का त्वरित उपयोग, स्पष्ट प्रोटोकाल और पारदर्शी जांच प्रक्रिया के साथ बच्चों की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए, ताकि कोई भी बच्चा व्यवस्था की चूक का शिकार न बने।
भारत में लापता बच्चों और मानव तस्करी के बढ़ते जाल ने अब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में जगह बना ली है। मानव तस्करी तो समस्त विश्व की चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के लिए तो यह और भी चिंताजनक है, क्योंकि यहां इस प्रकार के आपराधिक समूह सबसे ज्यादा फल-फूल रहे हैं। इस समस्या की भयावहता को देखते हुए इससे निपटने के लिए एक सशक्त संगठन या मंच की आवश्यकता है। मुक्त हुए बच्चों के लिए पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। प्रशासनिक तंत्र में कई स्तरों पर गंभीर कमियां हैं। परिवारों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होती। कई मामलों में पुलिस प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में यह मान लेती है कि बच्चा स्वयं लौट आएगा, जिससे खोज के शुरुआती महत्वपूर्ण घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। राज्यों के बीच समन्वय का अभाव लापता बच्चों की तलाश को और चुनौतीपूर्ण बना देता है। मिशन वात्सल्य जैसी योजनाएं व विभिन्न पोर्टल मौजूद होने के बावजूद उनका प्रभाव जमीन पर नहीं दिखता। यह समस्या दर्शाती है कि केवल नीतियां बना देना पर्याप्त नहीं है।
हालांकि, बच्चों के लापता होने के पीछे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जो परिवार, स्कूल और समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं। परिवारों में संवाद की कमी, तनावपूर्ण सामाजिक वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और जागरुकता का अभाव इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। स्कूलों में परामर्श से जुड़ी सेवाएं सीमित और औपचारिकता भर होती हैं। समुदाय स्तर पर भी बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव देखने को मिलता है। कई घटनाओं में बच्चे पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, परीक्षा के भय, भावनात्मक तनाव या प्रेम संबंधों के कारण घर छोड़ देते हैं। कुछ मामलों में रोजगार या बेहतर भविष्य के नाम पर बच्चे ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जहां से लौटना लगभग असंभव हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि यह संकट केवल अपराध नियंत्रण से संबंधित नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)





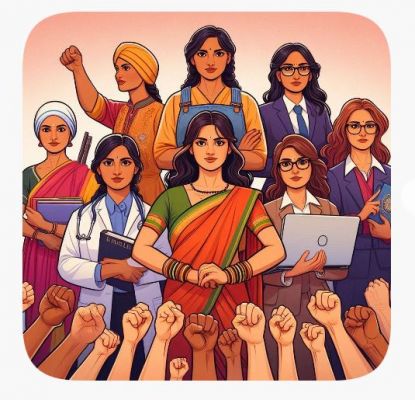

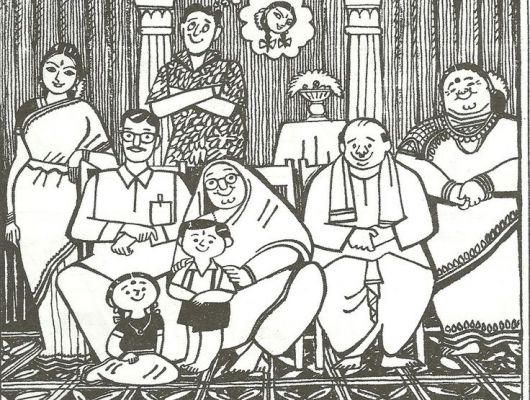


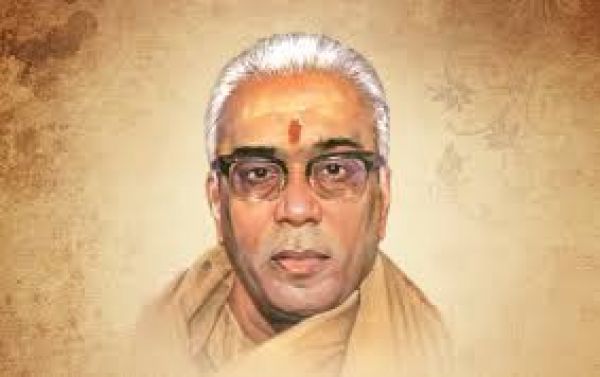



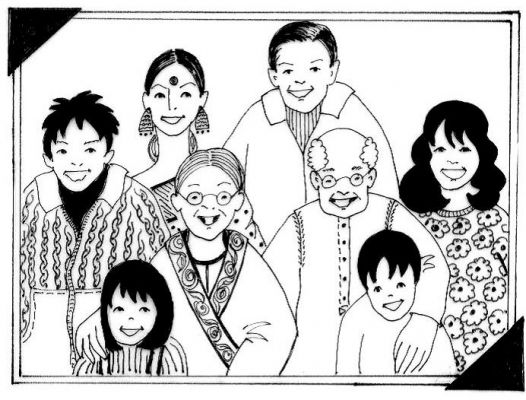
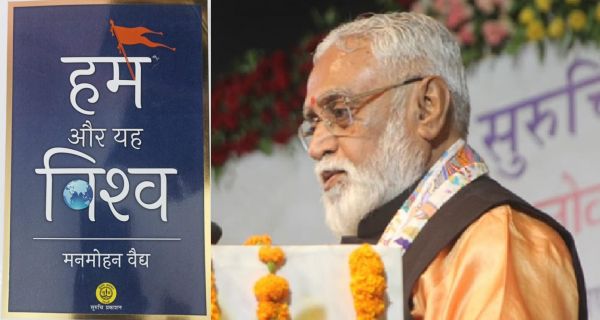






.png)