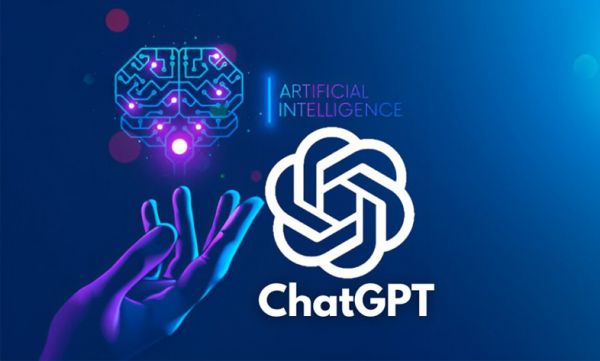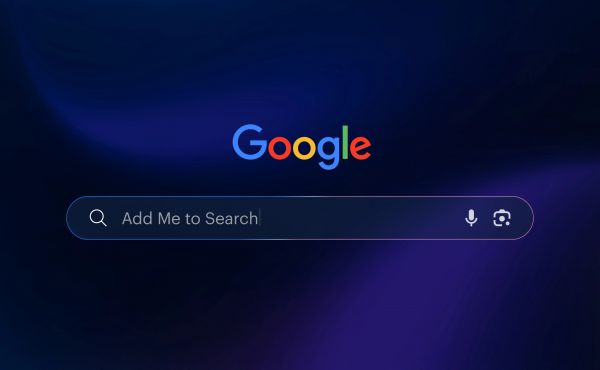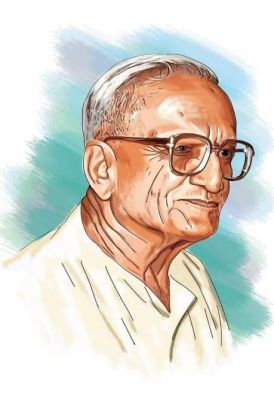कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स के एक अध्ययन में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच भारी आनुवंशिक अंतर पाया गया है।
अध्ययन की पद्धति क्या है?
- शोधकर्ताओं ने लगभग 5,000 व्यक्तियों से डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) एकत्र किया , जिनमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग शामिल थे। इस समूह में कुछ मलय, तिब्बती और अन्य दक्षिण-एशियाई समुदायों के डीएनए भी शामिल थे।
- उन्होंने उन सभी उदाहरणों की पहचान करने के लिए संपूर्ण-जीनोम अनुक्रमण किया जहां डीएनए में या तो परिवर्तन दिखा, गायब था, या अतिरिक्त आधार-जोड़े, या 'अक्षर' थे।
अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?
- अंतर्विवाही प्रथाएँ:
- भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के बीच बहुत कम मिश्रण है ।
- जाति-आधारित, क्षेत्र-आधारित और सजातीय (बंद रिश्तेदार) विवाह जैसी अंतर्विवाही प्रथाओं ने सामुदायिक स्तर पर आनुवंशिक पैटर्न को संरक्षित करने में योगदान दिया ।
- एक आदर्श परिदृश्य में, आबादी में यादृच्छिक संभोग होता, जिससे अधिक आनुवंशिक विविधता और वेरिएंट की कम आवृत्ति होती, जो विकारों से जुड़ी होती है।
- क्षेत्रीय रुझान:
- ताइवान जैसी अपेक्षाकृत बहिष्कृत आबादी की तुलना में, दक्षिण एशियाई समूह - और इसके भीतर, दक्षिण-भारतीय और पाकिस्तानी उपसमूह - ने संभवतः सांस्कृतिक कारकों के कारण, समयुग्मक जीनोटाइप की उच्च आवृत्ति दिखाई।
- मनुष्य के पास आमतौर पर प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं। जब किसी व्यक्ति के पास एक ही प्रकार की दो प्रतियां होती हैं, तो इसे होमोजीगस जीनोटाइप कहा जाता है।
- प्रमुख विकारों से जुड़े अधिकांश आनुवंशिक वेरिएंट प्रकृति में अप्रभावी होते हैं और केवल दो प्रतियों में मौजूद होने पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। (विभिन्न प्रकार का होना - अर्थात विषमयुग्मजी होना - आमतौर पर सुरक्षात्मक होता है।)
- अनुमान लगाया गया कि दक्षिण-भारतीय और पाकिस्तानी उपसमूहों में उच्च स्तर की अंतःप्रजनन दर थी, जबकि बंगाली उपसमूह में काफी कम अंतःप्रजनन देखा गया।
- न केवल दक्षिण एशियाई समूह में अधिक संख्या में ऐसे वैरिएंट थे जो जीन के कामकाज को बाधित कर सकते थे, बल्कि ऐसे अनोखे वैरिएंट भी थे जो यूरोपीय व्यक्तियों में नहीं पाए गए थे।
- ताइवान जैसी अपेक्षाकृत बहिष्कृत आबादी की तुलना में, दक्षिण एशियाई समूह - और इसके भीतर, दक्षिण-भारतीय और पाकिस्तानी उपसमूह - ने संभवतः सांस्कृतिक कारकों के कारण, समयुग्मक जीनोटाइप की उच्च आवृत्ति दिखाई।
- समयुग्मक वेरिएंट की उच्च आवृत्ति का जोखिम:
- दुर्लभ समयुग्मक वेरिएंट की उपस्थिति से हृदय रोग, मधुमेह , कैंसर और मानसिक विकार जैसे विकारों का खतरा बढ़ गया है ।
आनुवंशिक विविधता पर अन्य अध्ययन क्या हैं?
- 2009 में, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में कुमारसामी थंगराज के समूह द्वारा नेचर जेनेटिक्स में एक अध्ययन से पता चला कि भारतीयों के एक छोटे समूह को अपेक्षाकृत कम उम्र में हृदय विफलता का खतरा है ।
- ऐसे व्यक्तियों के डीएनए में हृदय की लयबद्ध धड़कन के लिए महत्वपूर्ण जीन में 25 बेस-जोड़े की कमी थी (वैज्ञानिक इसे 25-बेस-जोड़े का विलोपन कहते हैं)।
- यह विलोपन भारतीय आबादी के लिए अद्वितीय था और, दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ समूहों को छोड़कर, अन्यत्र नहीं पाया गया था।
- यह विलोपन लगभग 30,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था , कुछ ही समय बाद जब लोगों ने उपमहाद्वीप में बसना शुरू किया, और आज भारतीय आबादी का लगभग 4% प्रभावित होता है ।
- ऐसी आनुवांशिक नवीनताओं की पहचान करने से जनसंख्या-विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों और कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है।
आनुवंशिक विविधता पर ऐसे अध्ययनों का क्या महत्व है?
- अध्ययनों से पता चला है कि विशिष्ट आनुवंशिक नवीनताएं भारत की आबादी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं । इन आनुवंशिक विविधताओं को समझने से प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं के लिए बेहतर हस्तक्षेप हो सकता है।
- देश के भीतर आनुवांशिक अध्ययन करने से कमजोर समुदायों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी अनुसंधान संगठनों द्वारा संभावित शोषण से बचाया जा सकता है।




.jpg)