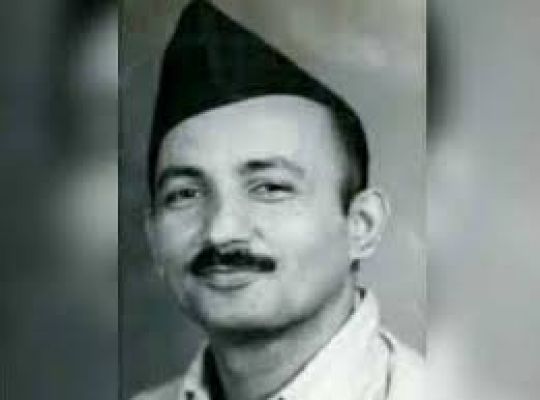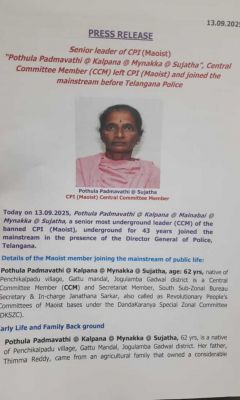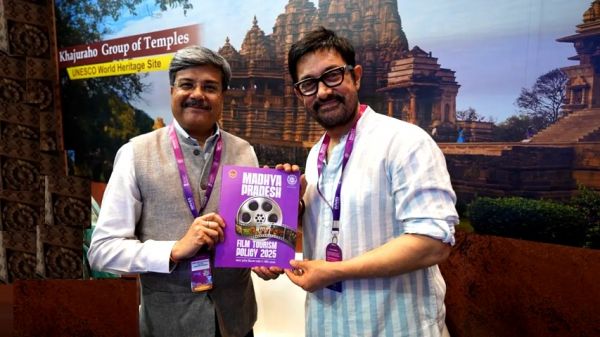ये जिद आज भारत में उन तमाम करोड़ों लोगों की है, जोकि हिन्दी के सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। हिन्दी उनके जीवन में परस्पर संवाद का काम करती है और उन्हें खुशहाल बनाती है। इसलिए ये साफतौर पर आज देश भर में यही कह रहे हैं, “हिन्दी बोलने के लिए साहब आप कितना भी क्यों न मारिए, पर मैं हिन्दी बोलना नहीं छोडूंगा।” पर कुछ सिरफिरे हैं, जिनके पास लगता है कोई काम नहीं, वह भाषा विवाद पैदा करके ही अपनी राजनीति चमकाते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों से लेकर महाराष्ट्र तक में यह संकट बहुत घना है। अचानक बीच-बीच में यहां एक आन्दोलन खड़ा होता है और आवाज बुलंद की जाती है कि हिन्दी का विरोध करना है।
अभी महाराष्ट्र से पहले तमिलनाडु, कर्नाटक में हिन्दी के खिलाफ आवाज तेजी से उठती दिखी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि राज्य में हिन्दी का विरोध किया जाएगा, क्योंकि हिन्दी मुखौटा है और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा', पर क्या वास्तव में ऐसा है? अभी सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के कार्यकर्ताओं द्वारा एक गुजराती दुकानदार की पिटाई करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, वास्तव में ये वीडियो बहुत आहत करता है। भाषा के लिए आप किसी को भी मारेंगे ? एमएनएस कार्यकर्ता दुकानदार से कहते हैं कि ये महाराष्ट्र है, इसलिए यहां मराठी बोलना ही होगा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मराठी और इंग्लिश अनिवार्य करने की अपील की है। इन्हें हिन्दी से दुश्मनी है!
दूसरी ओर महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए हिन्दी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था। किताबे छप चुकी, लेकिन अब एमएनएस की तरह ही राज्य में कई संगठन और राजनीतिक दलों ने हिन्दी पढ़ाने का विरोध जारी रखा। जिसके चलते आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने 22 अप्रैल को हिन्दी अनिवार्य करने का अपना निर्णय वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र में हिन्दी बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है। यहां गंभीरता से विचार सभी को यह अवश्य करना चाहिए कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार त्रि-भाषा सूत्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्यों लेकर आई।
तथ्यों को गहराई से जानें तो भारत में स्वाधीनता के बाद सबसे पहले त्रि-भाषा सूत्र को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) ने वर्ष 1968 की नीति में उल्लेखित किया था। कोठारी आयोग ने ही सिफ़ारिश की थी कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा अथवा दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक के अध्ययन की व्यवस्था एवं अहिन्दी भाषी राज्यों में राज्य भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। इसी व्यवस्था को त्रि–भाषा सूत्र के नाम से जाना गया। इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत की संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया जिसे ‘राजभाषा संकल्प 1968’ के नाम से जाना जाता है।
राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार- भारत की एकता एवं अखंडता की भावना को बनाए रखने एवं देश के विभिन्न भागों में जनता में संपर्क सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि भारत के केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित किया जाएगा। कोठारी आयोग के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। चूंकि त्रि-भाषा सूत्र को पूरी तरह व्यावहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सका था, इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि उपर्युक्त त्रि-भाषा सूत्र को लागू किया जाएगा। अब थोड़ा अध्ययन अपने आसपास के देशों का और युरोप सहित दुनिया के प्रमुख देशों का भी भाषा के स्तर पर कर लेना चाहिए।
भारत के पड़ोसी देश चीन में 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। चीनी भाषा (सिनिटिक) में सात मुख्य भाषा समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें मंदारिन, वू, कैंटोनीज़, मिन, हक्का, गान और जियांग शामिल हैं। किंतु एक भाषा के स्तर पर चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। इन सभी में भारत की तरह से कोई आपसी विरोध नहीं दिखता। नेपाल में 124 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। जिसमें कि नेपाली देश की आधिकारिक भाषा है । इसके बाद मैथिली दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेपाल में कई अन्य भाषाओं में भोजपुरी, थारू, नेवारी, लिम्बू, राय, शेरपा, मगर, गुरुंग हैं। पाकिस्तान में लगभग 70 से 80 भाषाएं हैं। उर्दू को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सरायकी और बलूची जैसी भाषाएं भी पाकिस्तान में व्यापक रूप से लोग बोलते हैं। हिंडको, ब्राहवी, कोहिस्तानी, और अन्य कई भाषाएं भी पाकिस्तान में बोली जाती हैं। पर उर्दू के मामले में सभी एकमत हैं।
भारत के एक अन्य पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में लगभग 40 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 36 जातीय अल्पसंख्यक भाषाएं हैं और 6 गैर-जातीय अल्पसंख्यक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषा बांग्ला है। कुछ प्रमुख भाषाएं हैं- चकमा, उर्दू, गारो, मीतेई, कोकबोरोक, और राखीन। इस देश में भी कोई भाषा विवाद नजर नहीं आता। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से दो आधिकारिक भाषाएं हैं: पश्तो और दारी। इसके अलावा, कई अन्य क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि उज्बेकी, तुर्कमेनी, बलूची, पशाई, अरबी, उर्दू, और कुछ पामीरी भाषाएं। श्रीलंका में मुख्य रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं, सिंहली और तमिल। कुछ लोग क्रियोल मलय जैसी अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। पर आपस में किसी का कोई परस्पर भाषायी विवाद नहीं।
जर्मनी में लगभग 250 बोलियां हैं, जिनमें से मानक जर्मन देश की आधिकारिक भाषा है। यहां प्रमुखता सेतुर्की, कुर्द, पुर्तगाली, अरबी, अल्बानियाई, रूसी, पोलिश, आदि, जो जर्मनी में प्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। जर्मनी में अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन जैसी विदेशी भाषाएं भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 350 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी और इसके बाद स्पेनिश का नंबर आता है। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 150 मूल अमेरिकी भाषाएं भी बोली जाती हैं।
रूस में, रूसी भाषा राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र आधिकारिक भाषा है, लेकिन इसके अलावा, 35 अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। फ्रांस में फ्रेंच देश की आधिकारिक भाषा है, वहीं लगभग 75 क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ को स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। जिनमें ओसीटान, ब्रेटन, बास्क, कोर्सीकन, अलसैटियन और कुछ मेलानेशियन भाषाएं शामिल हैं। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। साथ ही कुछ क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां भी हैं, जैसे कि रयुक्युआन भाषाएं, जो ओकिनावा और कागोशिमा के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं, और ऐनू भाषा, जो होक्काइडो में बोली जाती है।
ब्रिटेन में अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ स्वदेशी हैं और कुछ विदेशी हैं। यहां वेल्श, स्कॉटिश गेलिक, आयरिश, स्कॉट्स और कॉर्निश जैसी स्वदेशी भाषाएं भी मौजूद हैं। ब्रिटेन में दुनिया भर से आए प्रवासियों के कारण कई विदेशी भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि पोलिश, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, और फ्रेंच। कुल यहां पर 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ब्रिटेन की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी 300 से अधिक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है। अन्य प्रमुख भाषाओं में मंदारिन, अरबी, कैंटोनीज़, वियतनामी और इतालवी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 23 स्वतंत्र भाषा परिवारों और 9 अलग-अलग समूहों को मान्यता दी गई है, जिसमें कुल 32 स्वतंत्र भाषा समूह हैं।
दूसरी तरफ भारत में 121 प्रमुख भाषाएँं और 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कहना होगा कि भारत में भाषाओं की विविधता देश की सांस्कृतिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हम अन्य देशों के स्तर पर देख सकते हैं। पर भारत में तो आपस में विवाद हो रहा है। हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जा रही, पर माहौल यही बनाया जाता है। क्या भारत में एक संपर्क भाषा नहीं होनी चाहिए? अंग्रेजी भाषा जोकि एक विदेशी भाषा है, उसे हंसते हुए स्वीकार करेंगे, लेकिन हिन्दी जो उनके देश की ही एक भाषा है, उसका विरोध करेंगे। क्या यह गुलाम मानसिकता का परिचय नहीं है? दुनिया का कौन अभागा देश होगा, जहां इस तरह से उस देश के लोग भाषा विवाद खड़ा कर एक दूसरे को पीट रहे हैं? जैसा कि भारत में आए दिन दिखाई देता है!
वस्तुत: सोचने वाली बात यही है कि जब देश भाषा के स्तर पर बहुत समृद्ध है फिर हमें अंग्रेजी को एक संपर्क भाषा के रूप में क्यों रखना चाहिए? यदि हिन्दी सरल है तब हम अपनी इस भाषा को संपर्क की भाषा क्यों नहीं बनाएं? इसके साथ ही हिन्दी भाषियों को क्यों हिन्दी या अंग्रेजी तक सीमित रहना चाहिए, उन्हें भी अन्य भारतीय भाषाओं में रुचि दिखाकर उन्हें सीखना चाहिए और यही बात हिन्दी राज्यों के अलावा अन्य भाषायी राज्यों पर भी लागू होती है। समझने की बात यही है कि दुनिया के तमाम देशों में हमारे पड़ोसी मुल्कों तक में अनेक बोली-भाषा प्रचलन में हैं, किंतु आपसी विवाद नहीं। इसी प्रकार की स्थिति आज भारत में होने की आवश्यकता है।
लेखक- डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)





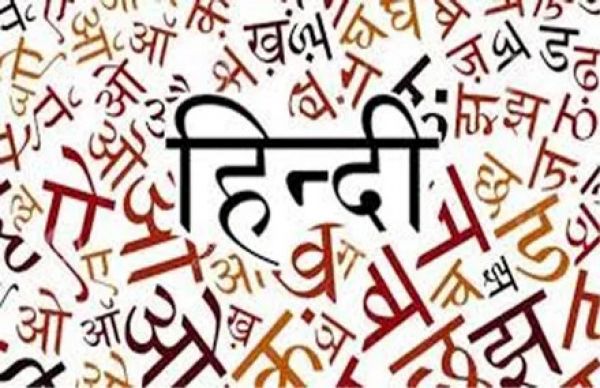

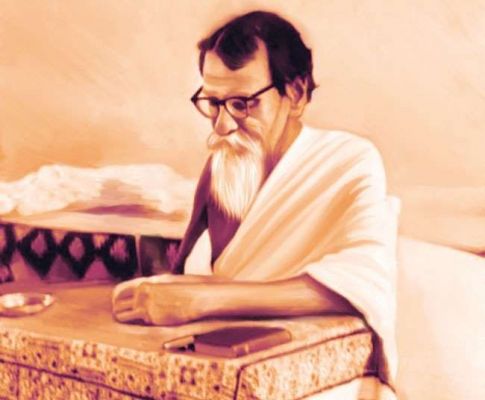
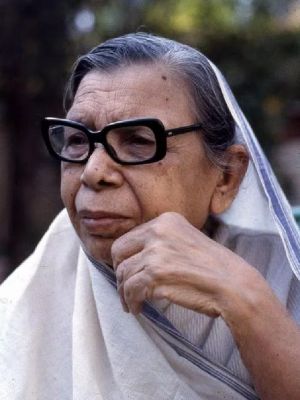
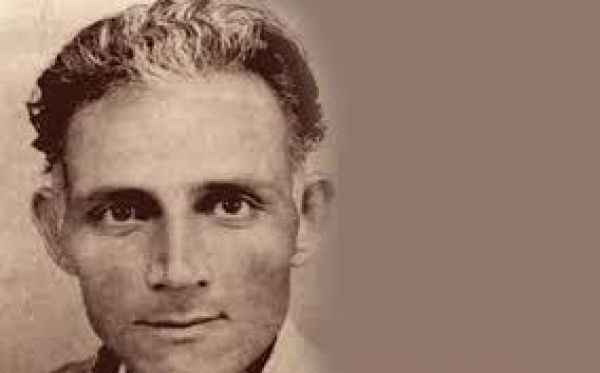
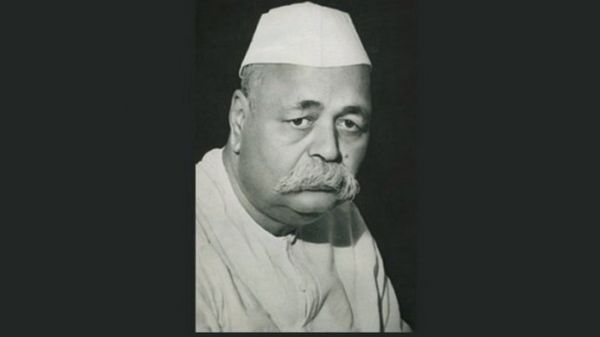


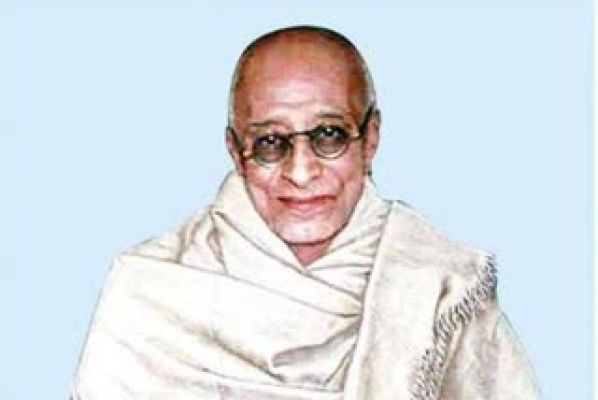

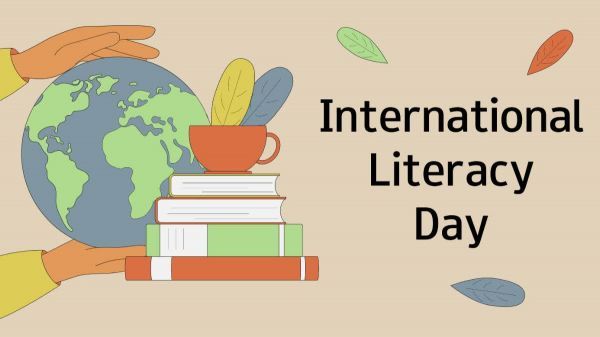


.jpg)