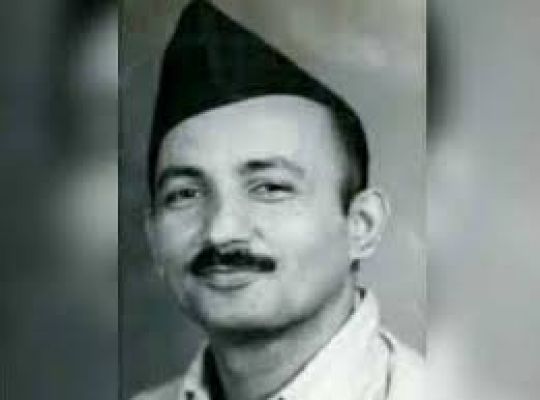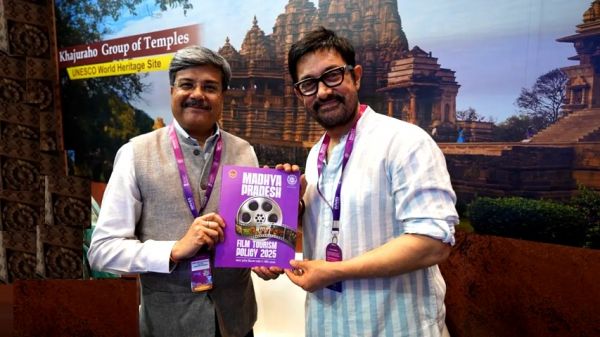गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हुए हालिया पुरातात्विक शोध से यह खुलासा हुआ है कि इस इलाके में मानव बस्तियां हड़प्पा सभ्यता से हजारों वर्ष पहले भी थीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (IITGN) के नेतृत्व में, IIT कानपुर, IUAC दिल्ली और PRL अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन को अंजाम दिया। इस शोध में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति को कम से कम पाँच हजार साल पीछे ले जाते हैं।
शोध में यह संकेत मिला कि उस समय के प्रारंभिक मानव समुदाय मैन्ग्रोव से भरपूर इलाके में रहते थे और अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से शंख प्रजातियों जैसे द्विकपाटी (ऑयस्टर) और गैस्ट्रोपोड्स पर निर्भर थे। ये समुद्री जीव उस पर्यावरण के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित थे।
IIT गांधीनगर के पृथ्वी विज्ञान विभाग में पुरातात्विक विज्ञान केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध के प्रमुख अन्वेषक प्रो. वी.एन. प्रभाकर के अनुसार, ब्रिटिश काल में किए गए सर्वेक्षणों में इन शंख जमावों का उल्लेख तो था, लेकिन उन्हें मानव उपभोग के बाद छोड़े गए शंख ढेर (शंख-मिट्टियों) के रूप में नहीं पहचाना गया था। अब इन स्थलों को सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व दिया गया है और इनके कालक्रम की पुष्टि भी की गई है।
इन स्थलों की आयु मापने के लिए शोधकर्ताओं ने एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) तकनीक का उपयोग किया, जिसमें शंखों में उपस्थित कार्बन-14 के रेडियोधर्मी समस्थानिक को मापा जाता है। विश्लेषण से यह साफ हुआ कि ये स्थल हड़प्पा काल से काफी पुराने हैं और इनसे प्राचीन मानव उपस्थिति के दुर्लभ साक्ष्य मिलते हैं।
कच्छ के ये नव-चिह्नित स्थल अब ऐसे पहले पुरातात्विक स्थल माने जा रहे हैं जिनका एक निश्चित सांस्कृतिक और कालक्रमिक सन्दर्भ है। शोध में यह भी पाया गया कि इन स्थलों की विशेषताएं पाकिस्तान के लसबेला और मकरान क्षेत्र तथा ओमान प्रायद्वीप के तटीय स्थलों से मिलती-जुलती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रारंभिक तटीय समुदायों ने समान जीवनशैली और भोजन एकत्रण की रणनीतियाँ अपनाई थीं।
शंख जमावों के अलावा, शोध टीम को पत्थर के औजार भी मिले हैं जो काटने, छीलने और चीरने जैसे कार्यों में उपयोग किए जाते थे। औजारों के साथ-साथ उनके निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पत्थर भी मिला है। IITGN की पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता और इस अध्ययन की सह-लेखिका डॉ. शिखा राय का मानना है कि इन उपकरणों की उपस्थिति दर्शाती है कि ये समुदाय तकनीकी रूप से काफी दक्ष थे। यह कच्चा माल संभवतः खड़ीर द्वीप से लाया गया होगा, जहां बाद में प्रसिद्ध हड़प्पा नगर धोलावीरा बसा।
ये निष्कर्ष कच्छ क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास को लेकर अब तक की सामान्य धारणा को चुनौती देते हैं। प्रो. प्रभाकर के अनुसार, यह विकास बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत हुआ, जिसमें स्थानीय पर्यावरण, जल स्रोतों और नौवहन के बारे में ज्ञान ने प्रमुख भूमिका निभाई। यही स्थानीय विशेषताएं बाद में हड़प्पा नगरों की बेहतर योजना और व्यापारिक नेटवर्क के विकास में सहायक रहीं।
शोधकर्ता मानते हैं कि शंख-मिट्टियाँ न केवल पुरातात्विक महत्व रखती हैं, बल्कि वे प्राचीन पर्यावरण और जलवायु अध्ययन (पुरापर्यावरणीय अनुसंधान) में भी सहायक साबित होंगी। चूंकि शंख जैसे जीवों में जलवायु संकेत संरक्षित रहते हैं, इसलिए उनके विश्लेषण से उस समय की जलवायु परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।
IIT गांधीनगर पहले ही खड़ीर द्वीप के पिछले 11,500 वर्षों के पुरापर्यावरणीय मानचित्रण पर काम कर चुका है। अब इन नए खोजे गए स्थलों का और गहन अध्ययन उस कालखंड की जलवायु, मानव अनुकूलन और सांस्कृतिक विकास को और गहराई से समझने का अवसर देगा। शोध टीम अब प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक की सांस्कृतिक यात्रा को समझने के लिए गुजरात का व्यापक सांस्कृतिक मानचित्र तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है।





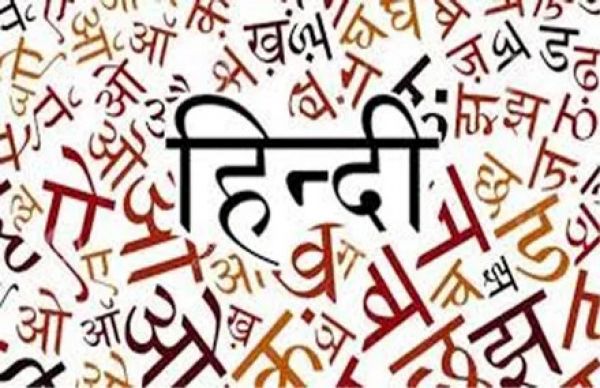

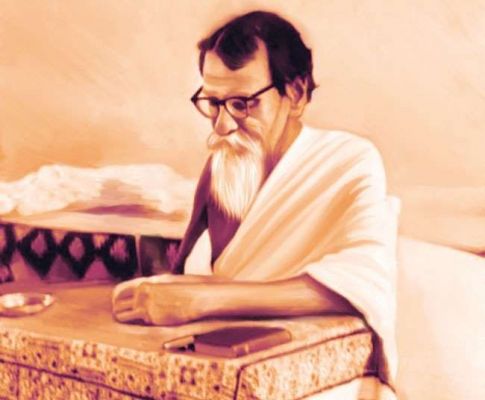
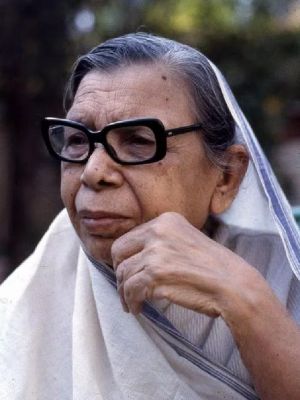
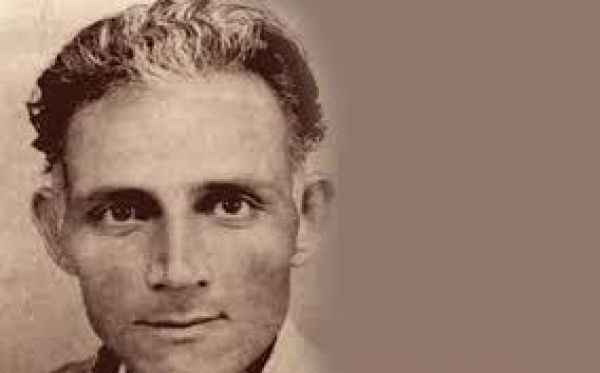
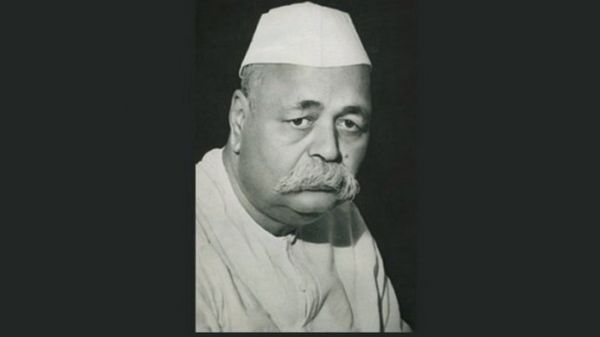


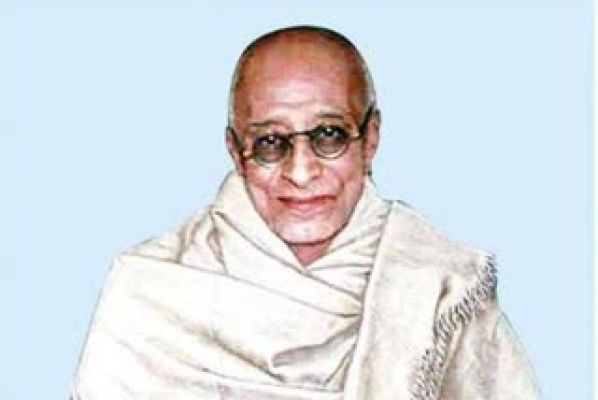

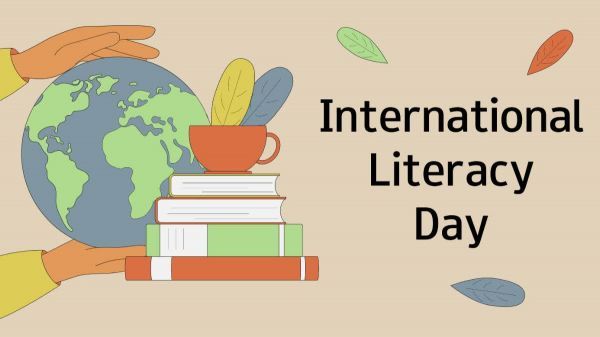


.jpg)