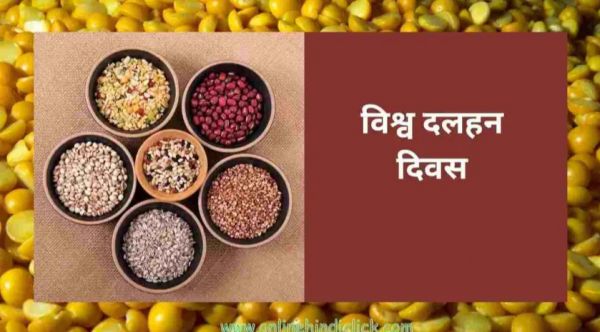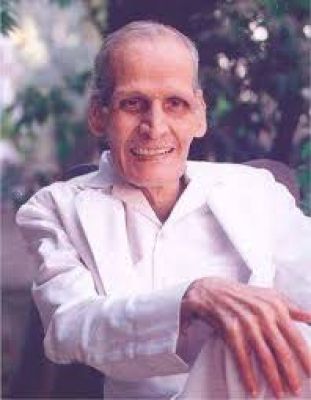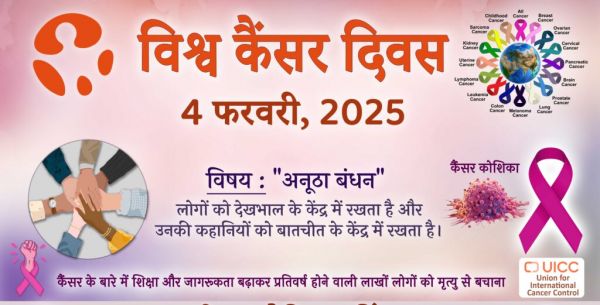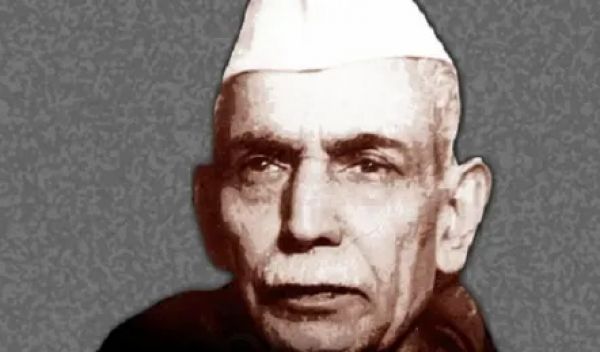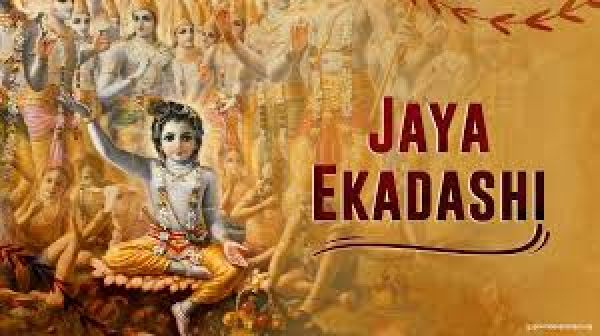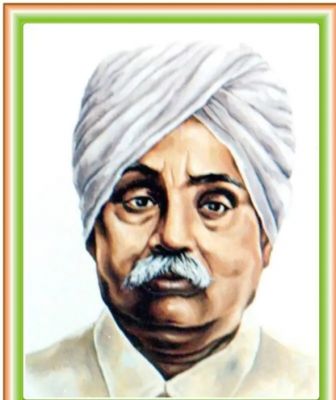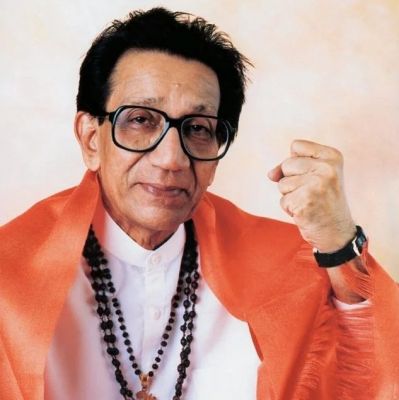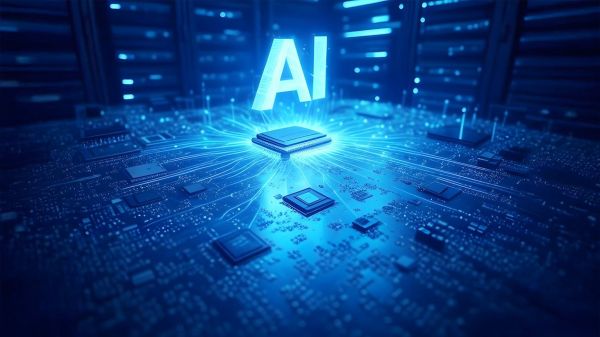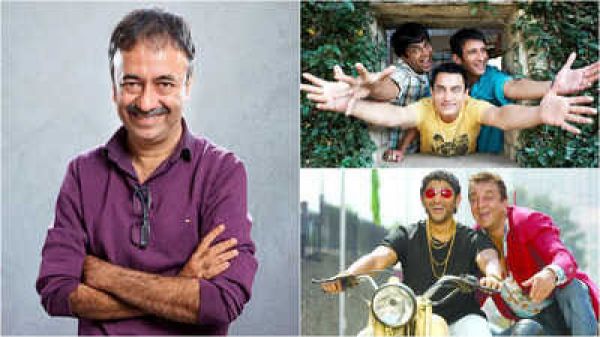हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में तीन आपराधिक कानूनों को देश को समर्पित किया । इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नए कानूनों के माध्यम से त्वरित न्याय की उम्मीद जताई, जो पूरी तरह से सार्थक भी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-जैसे तीन नए आपराधिक कानून हमारे समाज में गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्ग के लोगोंं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अन्य अपराधों पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। इन प्रयासों से हमें अपने कानूनी व्यवस्था को आजादी के अमृतकाल में अधिक प्रासंगिक और सहानुभूतिपूर्वक प्रेरित करने के लिए पुनर्भाषित करते हैं। इन कानूनों को मूर्त रूप देने में केन्द्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री अमित शाह की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है।कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का विरोध करते हैं और यह दलील देते हैं कि इससे देश में तानाशाह की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन, मैं उनके इन दलीलों को पूरी तरह से हास्यास्पद मानता हूं। क्योंकि, यदि आप भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि पुराने कानून औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति हैं, जिन्हें पूरे देश पर शासन करने के लिए बनाया गया था, न कि हमारे देश की नागरिकों की सेवा के लिए। इसी भाव-शून्यता के कारण ये कानून आमजनों के उत्पीड़न और शोषण का उपक्रम बन गए, जिनका उद्देश्य वास्तव में निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा और दोषियों को दंडित करना होना चाहिए था। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गये नए कानून निश्चित रूप से उपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। सार्वजनिक सेवा और जनकल्याणकारी कानूनों से एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमें याद रखना होगा कि न्याय में देरी केवल लोगों को हताश-निराश ही नहीं करती, बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो कानून एवं व्यवस्था का आदर न करने और उसके उल्लंघन के आदी लोगों का दुस्साहस बढ़ता है। तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल से एक ओर जहां 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना आवश्यक होगा।आंकड़े बताते हैं कि भारत के न्यायिक व्यवस्था में 3.5 करोड़ से भी अधिक लंबित मामले हैं और यहां विचाराधीन कैदियों की संख्या 77 फीसदी है, जो दोषियों की संख्या से तीन गुना अधिक है। वहीं, भ्रष्टाचार, अत्यधिक काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही तीव्र और पारदर्शी न्याय व्यवस्था को कायम करने की दिशा में एक बड़ी बाधा है। ऐसे में, मोदी विरोधी इस बात को समझें कि नियमों में बदलाव समय की मांग थी। सरकार के इन प्रयासों से निश्चित रूप से हमारे न्याय प्रणाली में अपेक्षित सुधारों को सुनिश्चित करते हुए, न्यायालयों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। देश में न्यायिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा भी बारंबार आग्रह किया गया है। क्योंकि, आजादी के बाद न्यायालय की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सुधारों को लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन, मोदी सरकार ने हमें 10 वर्षों के दौरान हमें एक नई उम्मीद दी है।कानून के जानकार इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ‘न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है’ और भारतीय संदर्भ में यह बात पूरी तरह से चरितार्थ होती है। यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि लंबित मामले और विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या हमारे समाज में अन्याय की भावना को जन्म देता है। हमने अखबारों की सुर्खियों में ऐसा कई बार पढ़ा है कि किसी मामले में न्यायालय जब तक अपना फैसला सुनाता है कि आरोपित की मृत्यु हो चुकी होती है। वहीं, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है, जब कोई आरोपी अपने आरोपों के दंड से अधिक समय जेल में बिता देते हैं। फिर, वर्षों तक जेल में रहने के बाद उन्हें न्यायालय से आरोप मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति न्याय की दृष्टि से अन्याय को जन्म देती है। इस स्थिति में त्वरित सुधार की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून समय की अनिवार्यता हैं और हमें इन प्रयासों का स्वागत करना चाहिए। हालांकि, अभी बस केवल एक शुरुआत हुई है। हमें निकट भविष्य में अपने न्याय व्यवस्था की कार्य पद्धति के विविध पक्षों में सुधार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें नियुक्तियां, स्थानांतरण व अवसंरचनात्मक विकास जैसे प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा, भारतीय न्यायिक सेवा में भाषायी मुद्दों का भी एक विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि यदि कोई कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति ओडिशा में न्यायाधीश का पदभार संभाला है, तो इससे वहां न्यायाधीशों और जनता के माध्यम से संचार में रुकावट पैदा होती है। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि ऐसी नियुक्तियों के दौरान हमारी भाषायी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए। साथ ही, हमें अपने न्याय व्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल भी बेहद कुशलतापूर्वक करना होगा। इससे न्यायालय और न्यायाधीशों के अलग-अलग प्रदर्शनों को मूल्यांकन करना बेहद आसान हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी के साथ कार्य करेंगे और समाज में अधिकार और न्याय को स्थापित करने की दिशा में आने वाली हर एक बाधा को दूर करते हुए पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे।
लेखक:- डॉ. विपिन कुमार